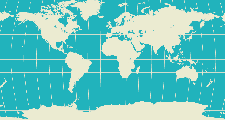साहित्य में घुसा बाज़ारवाद और जुगाड़वाद
अंबा प्रसाद श्रीवास्तव
नए संदर्भों में एक नया प्रश्न बहुत तेजी से उभर रहा है जो पहले प्रश्न से भी अधिक जटिल है किन्तु उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। जीवन के दूसरे क्षेत्रों पर बाजारवाद का पहले ही कब्जा हो चुका है और अब उसने चुपके-चुपके साहित्य सृजन के क्षेत्र पर भी अपना आधिपत्य जमा लिया है। भौतिकवाद की आँधी से उठी क्रान्ति की लहर ने प्रकाशकों को ही नहीं, लेखकों और समीक्षकों की दृष्टि भी बदल दी है। आमतौर पर कहा जाता है कि मुद्रणकला के विकास ने साहित्य को समृद्ध करने में ऐतिहासिक योग दिया है, जबकि वास्तविकता ठीक इसके विपरीत है। आज से डेढ़-दो-सौ वर्ष पहले प्रतिभा-विहीन व्यक्ति, कवि या लेखकों की जमात में शामिल होने की बात सोच भी नहीं सकता था और यदि किसी ने कवि होने के भ्रम में किसी कृति की रचना भी की तो पाठकों ने पहली ही नजर में उसे खोटे सिक्के की तरह नकार दिया।
ऐसी सैकड़ों पुस्तकें नष्ट हो चुकीं और जो किसी तरह बची रहीं, वे किसी संग्रहालय में ममी की तरह रखी हुई हैं। मुद्रण कला के विकास ने अब हर किसी को अपनी पुस्तक छपाने की सहज सुविधा उपलब्ध करा दी, जिसके कारण प्रायः हर रोज सैकड़ों पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, जिनका मूल्य किसी न किसी अंश में पाठकों को चुकाना पड़ता है। ऐसे अनेक कारण हैं जिनके आधार पर यह बेहिचक कहा जा सकता है कि कतिपय प्रकाशक जो येन-केन प्रकारेण धन अर्जित करने के लिए इस व्यवसाय में हैं, वे लेखकों का शोषण करने के साथ पाठकों का भी शोषण कर रहे हैं। पुस्तक का प्रकाशन और विक्रय व्यवसाय होता है किन्तु लेखन को किसी भी दृष्टि से व्यवसाय या धन अर्जित करने का जरिया मानना रचनाधर्मिता की अवमानना है।
अरस्तू और भरत मुनि से लेकर पूर्व या पश्चिम के किसी भी चिन्तक ने लेखन को व्यवसाय नहीं माना। आचार्य मम्मट के ‘अर्थकृते’ का आशय भी आजकल की तरह रायल्टी या पारिश्रमिक के रूप में रुपया कमाना नहीं रहा है। यह मार्क्सवादी दर्शन की देन है कि प्रत्येक कर्म को, वह किसी भी नीयत या उद्देश्य से किया जाय, श्रम से जोड़ दिया जाता है। इस दर्शन में लेखक की भावयित्री प्रतिभा को तो स्वीकार किया ही नहीं जाता, उसकी कारयित्री प्रतिभा को भी श्रम कौशल मान लिया जाता है। रचनाकार की कारयित्री प्रतिभा और सड़क पर गिट्टी तोड़ने वाले श्रमिक के कौशल में कोई अन्तर नहीं माना जाता। अच्छे-बुरे, सकाम-निष्काम, स्वार्थ और परार्थ सभी कर्मों का मूल्य पैसे में आँकने की मानसिकता ने ही मार्क्स को धर्म को भी व्यवसाय मानने के लिये प्रेरित किया था।
मार्क्स ने जिस संस्कृति को जन्म दिया है उसमें केवल शारीरिक श्रम का ही नहीं चिन्तन, मनन, बुद्धि और समय का मूल्य भी पैसे में आँका जाता है। लेखन या रचना-धर्मिता को भी इस संस्कृति ने अपनी चपेट में ले लिया है। साहित्य सृजन व्यवसाय बन गया है और प्रकाशक की भूमिका एक ऐसे फैक्टरी मालिक की बन गई है जो मजदूरों को मजदूरी का भुगतान कर माल का उत्पादन करता है। शोषण भी मार्क्सवादी दर्शन का ही शब्द है। इस संस्कृति के बीज साहित्य के क्षेत्र में कला, कला के लिये या कला जीवन के लिये विषय पर बहस के रूप में पिछली सदी के प्रारम्भिक दशकों में बोये गये थे जो अब वटवृक्ष की तरह चारों ओर जड़ जमा कर विशाल आल-बाल की शक्ल में बदल गये हैं। आज न तो कोई तुलसी की तरह ‘स्वान्तःसुखाय रघुनाथगाथा’ लिखने के लिये तैयार है और न भवभूति की भाँति भविष्य में कृति का मूल्यांकन करनेवालों की आशा में निश्चिन्त होकर बैठ जाने को तैयार है। उसकी रचनाधर्मी की भूमिका खत्म हो चुकी है और वह लेखकीय कौशल की पूँजी के बल पर, दूकानदार बन कर, पाठकों को उपभोक्ता मान कर, साहित्य के बाजार में बैठ गया है।
नई संस्कृति में लेखन का उद्देश्य बदल गया है और लेखकीय प्रतिभा के मानदण्ड भी बदल गये हैं। जिस प्रकार अमृत की प्राप्ति के लिये भेष बदलकर देवताओं की पंक्ति में बैठे राहु को देवता भी नहीं पहचान सके थे, उसी प्रकार आज पाठकों के लिये असली और नकली लेखकों की पहचान कठिन हो गई है। यह समस्या उन लोगों ने पैदा की है जो अपनी गाँठ का रुपया खर्च कर अथवा प्रभुता या किसी अन्य जुगाड़ से ऐसी पुस्तकें छपा लेते हैं जो सृजन की किसी कोटि में नहीं आती और उन्हें साहित्य के क्षेत्र में फैलती या फैलाती ‘प्रदूषण’ कहने में कोई हर्ज नहीं होगा। आजकल एक ओर केवल रुपया के लिये लिखने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और दूसरी ओर ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है जो अपना रुपया खर्च करके लेखकों की पंक्ति में बैठने के लिये छटपटाते रहते हैं। ऐसी ढेरों कविता पुस्तकें प्रकाशित हो रही है, जिनसे छायावादी युग की वे कवितायें ही हजार गुना अच्छी थीं जिन्हें एकान्त में गुनगुनाने से ही लोगों को कुछ क्षण के लिये ही सही, आनन्द की अनुभूति होती थी।
ईमानदार असली टिकाऊ लेखन की कमी आज हर पाठक को खलने लगी है, जबकि नकली लेखकों की मुलम्मा चढ़ी पुस्तकों से बाजार पटा रहता है। व्यवसाय की दृष्टि से हटकर पिछली सदी के चौथे दशक के आस-पास ही विदेशी भाषा और साहित्य के प्रभाव से हिन्दी में भी ऐसी पुस्तकें लिखी गई और प्रकाशित हुई जो पाठकों को आकृष्ट तो अवश्य करती रहीं किन्तु नैतिकता, सांस्कारिकता की दृष्टि से उनका कभी स्वागत नहीं किया गया। ऐसी पुस्तकों के लेखन की प्रेरणा अंग्रेजी और उर्दू के उन लेखकों से मिली थी, जो शराबखोरी और यौन सम्बन्धों के धरातल पर ही अपनी कहानियाँ और उपन्यास लिखते रहे तथा जिसे यथार्थवादी लेखन कहा जाता रहा। लेखन और प्रकाशन को व्यवसाय बनते ही सृजन के सम्पूर्ण क्षेत्र पर बाजारवाद ने कब्जा कर लिया और इसी के साथ समीक्षकों ने भी बिचौलिया दलाल की भूमिका अख्तियार कर ली।
आजकल किसी भी पुस्तक की समीक्षा लिखी नहीं जाती, लिखाई जाती है। ऐसी समीक्षाएँ ऐकान्तिक रूप से लेखक और समीक्षक के सम्बन्धों पर आधारित होती है, जिसमें या तो समीक्ष्य कृति को वर्ल्ड-क्लासिक सिद्ध किया जाता है या उसे पूरी तरह घटिया मानकर खारिज कर दिया जाता है। कला या समीक्षा के कोई मानदण्ड नहीं हैं। जब ‘कला के लिए’ या ‘कला जीवन के लिए’ मुद्दे पर बहस छिड़ी थी, तभी कविता और सृजन की अन्य विधाओं को उपयोगितावाद अर्थात् व्यवसाय से जोड़ने की शुरुआत हो चुकी थी। मार्क्सवादी समीक्षा के सिद्धान्त इस मान्यता पर आधारित हैं कि मनुष्य के जीवन में आर्थिक प्रेरणा ही मुख्य है और इसी के प्रभाव से कला तथा मानव-संस्कृति का विकास होता है। इस नीति से विकसित समाज के स्वरूप को प्रतिबिम्बित करने वाला साहित्य ही उच्च कोटि का होता है।
इससे पहले यूनानी आलोचक लांजायनस ने कहा था कि अर्थ के प्रति आकर्षण अच्छे साहित्य की सर्जना में सबसे बड़ा अवरोध होता है। दूसरे समीक्षक भी इससे सहमत रहे किन्तु मार्क्सवादियों ने अर्थप्रधान राजनीति के बल पर सभी मानदण्डों को एक ही झटके में तोड़कर फेंक दिया। कदाचित् यह भी मार्क्सवादी ‘थ्योरी-ऑफ-इवोल्यूशन’ का नतीजा है कि कुछ समय पहले तक मार्क्सवादी समीक्षा का जो रूप था वह भी अब बदलने लगा है और लेखक, समीक्षक के परस्पर सम्बन्ध तथा राजनीतिक आस्थाएँ ही समीक्षा का प्रमुख मानदण्ड बनते जा रहे हैं। लेखक और समीक्षक के सम्बन्ध बहुत कुछ अंशों में ठीक वैसे ही बनते जा रहे हैं जैसे औद्योगिक प्रतिष्ठान और विज्ञापन एजेन्सियों में होते हैं।
साहित्य के क्षेत्र पर बाजारवाद का कब्जा होने से लेखकों, प्रकाशकों और पाठकों के सामने अनेक समस्याएँ पैदा हो गई हैं। लेखक परेशान है कि उसके सृजन का समुचित समादर नहीं हो रहा, प्रकाशक परेशान है कि पुस्तक खरीदने वालों की संख्या दिन-प्रतिदिन घटती जा रही है और पाठक परेशान है कि उसे नयी समीक्षा-शैली और विज्ञापन-कला के जाल में उलझ कर निहायत ही घटिया पुस्तकें खरीदनी पड़ती है। इस बात को सभी वर्ग स्वीकार करते हैं कि पुस्तकों के प्रति पाठकों का रुझान कम होता जा रहा है, किन्तु इसके लिये कभी दूरसंचार संस्कृति को दोषी ठहराया जाता है, कभी सूचना-प्रौद्योगिकी के विस्तार को जिम्मेदार माना जाता है या कभी कोई दूसरा कारण बतला दिया जाता है। इस बात की ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा कि साहित्य में बाजारवाद के पनपते ही ‘लेखकों, समीक्षकों और प्रकाशकों’ के प्रति पाठकों का विश्वास उठता जा रहा है।

 मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश