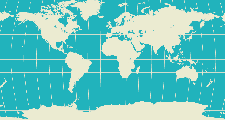हिंदी अगली सदी का शोधपत्र
सूर्यबाला
एक समय की बात है, हिन्दुस्तान में एक भाषा हुआ करती थी। उसका नाम था हिन्दी। हिन्दुस्तान के लोग उस भाषा को दिलोजान से प्यार करते थे। बहुत सँभालकर रखते थे। कभी भूलकर भी उसका इस्तेमाल बोलचाल या लिखने-पढ़ने में नहीं करते थे। सिर्फ कुछ विशेष अवसरों पर ही वह लिखी-पढ़ी या बोली जाती थी। यहाँ तक कि साल में एक दिन, हफ्ता या पखवारा तय कर दिया जाता था। अपनी-अपनी फुरसत के हिसाब से और सबको खबर कर दी जाती थी कि इस दिन इतने बजकर इतने मिनट पर हिन्दी पढ़ी-बोली और सुनी-समझी (?) जाएगी। निश्चित दिन, निश्चित समय पर बड़े सम्मान से हिन्दी झाड़-पोंछकर तहखाने से निकाली जाती थी और सबको बोलकर सुनाई जाती थी।
ये दिन पूरे हिन्दुस्तान में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते थे। बच्चों से लेकर विशिष्ट अतिथि और आयोजनों के अध्यक्ष तक इस भाषा में बोली जानेवाली कविता, निबन्ध अथवा भाषणों का रट्टा मारा करते थे। चूँकि उस दिन रिवाज के मुताबिक आना-जाना, उठना-बैठाना तथा हार पहनाना आदि सब कुछ हिन्दी में होता था, अतः अनुवाद की निरंकुश अफरा-तफरी और बेचैनी मच जाती थी। अनुवादकों की बन आती थी। पलक झपकते शब्द-के-शब्द, वाक्य-के-वाक्य दल-बदल लेकर कायापलट तक कर जाया करते थे। देखते-देखते ‘प्रपोजल’ ‘प्रस्ताव’ में, ‘रिक्वेस्ट’ ‘प्रार्थना’ में, ‘प्लीज’ ‘कृपया करके’ में, ‘थैंक्स’ ‘धन्यवाद’ में और ‘स्पीच’ ‘भाषण’ में बदल जाते थे।
देखते-देखते परम्परा, संस्कृति, भाषा, संस्कार, समृद्ध साहित्य, आदर्श, राष्ट्रीयता, कटिबद्ध, एकसूत्रता आदि शब्दों का ट्रैफिक जाम हो जाया करता था। इनाम पर इनाम, तमगे पर तमगे बाँटे जाते थे। इस एक दिन हिन्दी लाभ और मुनाफे की भाषा हो जाया करती थी। इसका सम्पूर्ण व्यक्तित्व छूट और ‘भव्य सेल’ की चकाचौंध से जगमगा उठता था। लेकिन यह छूट सिर्फ इन्हीं दिनों के लिए थी। बाकी दिनों बात बिना बात हिन्दी बोलने, इसे खर्च करने के जुर्म की सजा हर बेरोजगार, दकियानूसी और पिछड़े आदमी को भुगतनी पड़ती थी।
चूँकि यह भाषा समूचे हिन्दुस्तान की गरिमा की प्रतीक थी, इसलिए इसे वातानुकूलित ऑफिसों की एयरटाइट फाइलों में बन्द करके रखा जाता था। सरकार की तरफ से इसकी सुरक्षा के कड़े निर्देश थे। जेड क्लास सुरक्षा चक्रों के बीच, संसद की बैठकों में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता था कि ‘माननीय सभासदो! माननीय अध्यक्षजी!’ के अतिरिक्त सब कुछ अंग्रेजी में हो। इसलिए कुछेक सिरफिरों को छोड़कर सारे प्रस्ताव अंग्रेजी में ही प्रस्तावित और खारिज किए जाते थे। सारी-की-सारी योजनाएँ और बड़े-से-बड़े स्केंडल अंग्रेजी में ही किए जाते थे; जैसे बोफोर्स। सिर्फ कुछ विशेष प्रकार के स्केंडल हिन्दी में होते थे, जैसे प्रतिभूति घोटाला। कम अंग्रेजी बोलते थे, जो हिन्दीभाषी (पैदाइशी) थे, वे ज्यादा। क्योंकि उन्हें अपने पद की गोपनीयता की तरह ही अपनी भाषा की, गोपनीयता बनाए रखने की चिन्ता सर्वोपरि थी।
उस सदी में पूरे देश में गणतंत्र लागू होने पर भी तथा सभी सम्भव प्रकार के घोटालों की पूरी छूट होते हुए भी हिन्दी के मामले में सरकार के स्पष्ट अनुशासित और कड़े निर्देश थे कि खबरदार! हिन्दी को कोई छूने न पाए। यह सम्पूर्ण राष्ट्र की अस्मिता का प्रश्न है। अतः साक्षात्कारों तथा स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के अध्ययन तक हिन्दी के जरिए जो पहुँचने की कोशिश करेगा उसका प्रमोशन, परीक्षाफल, फाइल, आवेदन, अनुरोध, प्रार्थना तथा सारे अटके पड़े काम हमेशा के लिए अटके रह जाएँगे। वह लोगों द्वारा हेय दृष्टि से देखा जानेवाला उपेक्षा का पात्र होगा।
उस सदी में कुछ बड़े-बड़े लोगों के लिए ही हिन्दी बोलने का कोटा निर्धारित किया जाता था। कोई बड़ा लेखक, राजनीतिज्ञ, अफसर या अहिन्दीभाषी जब हिन्दी बोलता तो तालियाँ पिट जाती थीं, लोग ‘साधु-साधु’ कह उठते थे; लेकिन वही हिन्दी जब कोई सामान्य व्यक्ति बोलता तो वह उपहास, दया या उपेक्षा का पात्र समझा जाता था। इसलिए प्रायः ऐसे लोग अपने देश में अंग्रेजी और विदेशों में जाकर हिन्दी बोल आया करते थे।
स्कूलों में भी इस भाषा पर कोई आँच न आने पाए, इसका पूरा ध्यान रखा जाता था और हिन्दी की सारी पढ़ाई अंग्रेजी के माध्यम से करा दी जाती थी। आज की बात और है। आज तो हिन्दी भाषा का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। हिन्दी है ही नहीं। हिन्दी, इतिहास की, अतीत की भाषा हो चुकी है; लेकिन पिछली सदी में जब वर्तमान की भाषा थी तब भी सरकार और शिक्षाविदें ने ऐसी तकनीक ईजाद कर ली थी कि बगैर हिन्दी का एक शब्द भी खर्च किए हिन्दी पढ़ा-लिखा दी जाती थी। उन दिनों माताओं के लिए सबसे ज्यादा गर्व की बात यही हुआ करती थी कि उनका बच्चा सिर्फ हिन्दी में फेल हो गया। गोया हिन्दी में फेल होना अन्य विषयों में पास होने से ज्यादा महत्त्वपूर्ण था।
हमारी नवीनतम शोधें बताती हैं कि कुछ गलत दस्तावेज़ों और पुस्तकों के आधार पर हम हिन्दी को बीसवीं शताब्दी के हिन्दुस्तान की राष्ट्रभाषा, राजभाषा, सम्पर्कभाषा या मातृभाषा जैसा कुछ मान बैठते हैं। पर हकीकत तो यह है कि वह इनमें से कुछ भी नहीं हैं। ये सारे तथ्य भ्रामक हैं। शोध बताती है कि दरअसल हिन्दी भाषा थी ही नहीं। वह खास-खास अवसरों पर पहनी जानेवाली पोशाक थी, लगाया जानेवाला मुखौटा थी। वह एक डफली थी, जिस पर लोग अपने-अपने राग गाया करते थे। वह चश्मा थी, जिसे लगाकर अनुदानों, पुरस्कारों की छाया में सांस्कृतिक यात्राओं का सुख लूटा जा सकता था। वह एक सीढ़ी थी, जिसके सहारे आदमियों के मंच तक चढ़ा जा सकता था और करेंसी नोट थी, जिसे विशिष्ट आयोजनों पर सार्त्र, मार्क्स, ऑस्कर वाइल्टानस्टॉप, चे़खव और कामू के माध्यम से भुनाया जा सकता था। अपने देश की पिछली और अगली शताब्दियों के गरीब कवि-लेखकों में इसे भुनाने की औकात नहीं थी। ग्लानि और लज्जावश कबीर, सूर, तुलसी, रत्नाकर, भारतेन्दु, महादेवी वर्मा, प्रसाद और निराला तक नेपथ्य में छुप जाया करते थे, राजमार्गों से हट जाया करते थे।
दिक्कत सि़र्फ एक थी, हरेक के अपने चश्मे थे—और चश्मा जिस रंग को सही बताता था, दूसरा उसे पूरी तरह खारिज कर देता था।
डफलियाँ भी सबकी अलग-अलग, जिस पर अपने राग गाते तो भी ठीक था, लेकिन बाद के दिनों में सिर्फ डुगडुगी पीटने लगे और इसी फेरफार में हिन्दी की डुगडुगी पिट गई और वह पूरी तरह इतिहास की भाषा हो गई। अपने देश के लोगों द्वारा अपने देश की मिट्टी में विलीन हो गई।
दुःख है कि पिछली सदी की इस भाषा का कोई अवशेष नहीं रहा। इसलिए शोध छात्रों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनकी सुविधा के लिए सूचना दी जाती है कि वे चाहें तो विदेशों के कुछ विश्वविद्यालयों से हिन्दी से सम्बन्धित कुछ सामग्री और सूचनाएँ उपलब्ध कर सकते हैं।

 मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश