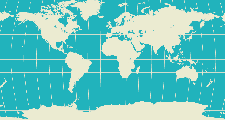राजनीतिक शून्यता का लोकतंत्र

पुण्य प्रसून वाजपेयी
जिस आर्थिक सुधार का ताना-बाना बीते दो दशक से देश में बुना जा रहा है, उसके भविष्य को लेकर अब कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। यह लगने लगा है कि यह ताना-बाना जमीन से ऊपर बुना जा रहा था। जमीन पर रहने वाले नागरिकों की जगह हवा में उड़ते उपभोक्ताओं के लिए अर्थव्यवस्था का खांचा बनाया गया, इसलिए कई सवाल एक साथ उठ सकते हैं। मसलन, क्या इन बीस बरसों में संसदीय राजनीति भी जमीन से उठ कर हवा में गोते लगाने लगी है? क्या लोकतंत्र का राग अलापती चुनावी प्रक्रिया भी लोगों के वोट से ऊपर उठ गई है? क्या सरकार का टिकना या चलना, जनता की आकांक्षाओं पर निर्भर नहीं रहा? क्या सत्ता का मतलब चुने हुए नुमाइंदों से हट कर कुछ और हो गया? जाहिर है, ये सभी सवाल राजनीतिक हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि असल में इस दौर में राजनीतिक शून्यता गहराती चली गई और इस वक्त देश एक ऐसे मुहाने पर आ खड़ा हुआ है, जहां विकल्प का सवाल भी विकल्पहीन हो चला है?
देश के चौदह कैबिनेट मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की सूची अण्णा समूह ने जारी की है। प्रधानमंत्री चाहे जितने बेदाग़ हों, लेकिन क्या यह काफी है? क्या प्रधानमंत्री को सिर्फ निजी ईमानदारी के दावे से आंका जाएगा? क्या प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों की जवाबदेही से बच सकते हैं? एक अहम सवाल यह भी है कि क्या दाग़दार लोग कभी बेदाग़ नीतियां बना सकते हैं? गृह, रक्षा, संचार, कोयला, खनन, जहाजरानी, सड़क, ऊर्जा, वाणिज्य मंत्रालय से लेकर योजना आयोग तक की नीतियों से यह गंभीर स्थिति सामने आई है। जाहिर है कि यहां सवाल सीधे सरकार का है, जिसे जनता ने चुना है, लेकिन यहीं से राजनीतिक शून्यता का वह सिलसिला शुरू होता है, जो बताता है कि आख़िर जनता की चुनी गई सरकार, लगातार ख़ुद की सत्ता बनाए रखने के लिए, लोकतंत्र का अवमूल्यन करते जाने से बाज नहीं आती।
लोकतंत्र की नई परिभाषा हर सत्ता अपने-अपने तरीके से गढ़ती जा रही है और वही लोकतंत्र की सत्ता कहलाने लगी है। यह सत्ता भ्रष्ट को भी पनाह देती है और ईमानदार को तमगे से नवाजती भी है। रईसों की सुविधा के लिए नीतियां बनाती है तो ग़रीब को भी सियासी सुविधा में तोलती है। यह नौकरशाह को सरकार से जुड़ने का न्योता देकर उसको अपनी सत्ता बनाने का मौका भी देती है और अपनी स्वायत्तता बरकरार रखने वाले नौकरशाह को सत्ता की हनक दिखाती भी है। यह एक ओर जनता को वोट की ताकत समझती है, और दूसरी ओर, कॉरपोरेट को ताकतवर बना कर ख़ुद उसके सामने नतमस्तक भी हो जाती है, यानी सत्ता लोकतंत्र का ऐसा ताना-बाना बुन रही है, जिसमें हर कोई अपने-अपने घेरे में किसी हद तक सत्ता बनने की पहल को ही लोकतंत्र मान ले।
विकल्प का सवाल यहीं से शुरू होता है। विपक्ष की राजनीतिक दिशा विकल्प का ताना-बाना बुनती है, लेकिन यहीं से एक दूसरा सवाल भी खड़ा होता है कि सत्ता के रुझान अगर जनता को नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो क्या विपक्ष की राजनीति जन-सरोकारों को देख कर अपना रास्ता बना रही है? अगर विपक्ष की राजनीति के सरोकार जमीन से जुड़े हैं, तो फिर सरकार कैसे जमीन से ऊपर हवा में गोते लगा कर अपनी सत्ता बरकरार रख सकती है? जाहिर है, यहां सरकार को ही नहीं, विपक्ष को भी परखने की जरूरत है और विपक्ष का जो हाल है, वह केंद्र से लेकर राज्यों तक में इस अहसास को जगाता है कि सत्ता बरकरार होने या रखने का मतलब राजनीतिक शून्यता से लबरेज़ होना है।
संघ परिवार केंद्र में भाजपा का रास्ता यह कह कर बनाने पर आमादा होता है कि वह तो समाज और देश को देखता है, सियासत या सत्ता-प्राप्ति की कोशिश तो भाजपा को करनी है। जाहिर है, कांग्रेसी सत्ता के लिए यह काफी सुविधाजनक स्थिति है, क्योंकि राजनीति का ककहरा भाजपा को वह परिवार पढ़ाता है, जो खुद को ग़ैर-राजनीतिक मानता है। इसका दोहरा असर राजनीतिक तौर पर भाजपा या संघ के भीतर से कैसे निकलता है, यह नरेंद्र मोदी या संजय जोशी के सियासी कदमताल से समझा जा सकता है। गुजरात में संघ की व्यूह रचना करते-करते मोदी, संघ के दायरे से बाहर, भाजपा की नई राजनीति के मार्गदर्शक बनते नज़र आते हैं। दूसरी तरफ भाजपा की राजनीति के सांगठनिक व्यूह को रचते संजय जोशी, भाजपा से बाहर निकाल दिए जाते हैं और उनका आसरा संघ हो जाता है।
राजनीतिक शून्यता का यह खेल संयोग से हर प्रांत में उभरता है और सत्ता अपने लोकतंत्र का जाप करती जाती है। मसलन, नरेंद्र मोदी को राजनीतिक टक्कर देते नीतीश कुमार का लोकतंत्र बिहार से आगे जाता नहीं और बिहार में लोकतंत्र का मतलब नीतीश की सत्ता पर अंगुली न उठा पाने की शून्यता है। अगर कानून-व्यवस्था को छोड़ दें, तो बिहार के हालात में कोई परिवर्तन आया हुआ दिखता नहीं है, लेकिन हालात की तफसील में जाने का मतलब है, नीतीश के कार्यकाल की खामियों से ध्यान हटा कर लालू यादव-राबड़ी देवी के कार्यकाल की कटु स्मृतियों को ताजा करना, जो कोई बिहारी चाहेगा नहीं और राजनीतिक तौर पर विपक्ष की यही शून्यता नीतीश को टिकाए रखेगी और मनमाफिक तानाशाह बनने से रोकेगी भी नहीं, अगर बारीकी से परखें तो मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, ओड़िशा, उत्तर प्रदेश, पंजाब सरीखे राज्यों में यही स्थिति है।
उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी यादव परिवार की बहू को चुनाव के मैदान में कोई चुनौती इसलिए नहीं मिलती, क्योंकि राजनीतिक गणित में समाजवादी पार्टी की स्थिति, शतरंज की बिसात पर इस वक्त घोड़े की ढाई चाल वाली है और हर किसी को लगता है कि जो हालात देश के हैं, उनमें मुलायम सिंह यादव की किसी भी चाल की जरूरत उन्हें कभी भी पड़ सकती है, लेकिन लोकतंत्र के तकाजे में जरा अतीत के पन्नों को टटोलें, तो इससे पहले यादव परिवार की बहू को उस कांग्रेसी उम्मीदवार ने मात दी थी, जिसकी पहचान राजनीतिक तौर पर नहीं थी। कांग्रेसी टिकट पर राजबब्बर इसलिए जीत गए थे, क्योंकि तब डिंपल की जीत का मतलब सफेद पैंट-शर्ट पहने वसूली करने वालों का हुजूम होता। राजबब्बर की जीत के साथ मतदाताओं ने ख़ुद को वसूली के आतंक से निजात दिलाई थी।
मगर, इस दौर में क्या सपा बदल गई? चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने पुरानी गलतियों से सबक लेने की बात बार-बार दोहराई थी, लेकिन सपा की नई सरकार बनने के बाद जल्दी ही यह साफ हो गया कि उसके चाल-चरित्र में कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन, अब सपा के विरोध का मतलब है, दुबारा उन मायावती की ओर रुख करना, जिन्होंने राजनीतिक साख को भी नोटों की माला में बदल कर पहना और गाए दलित संघर्ष के गीत। तो बेटे के जरिए मुलायम का कथित समाजवाद लोकतंत्र के जैसे भी गीत गाए, उसे बर्दाश्त करना ही होगा। यही सवाल पंजाब में अकालियों को लेकर खड़ा है। वहां कांग्रेसी कैप्टन का दरवाज़ा ही आम लोगों के लिए कभी नहीं खुलता, इसलिए लोग बादल परिवार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त करने को विवश हैं।
छत्तीसगढ़ में जिसने भी कांग्रेसी जोगी की सत्ता के दौर को देखा-भोगा, उसके लिए रमन सिंह की सत्ता की लूट कोई मायने नहीं रखती। मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान इसलिए बर्दाश्त किए जाते हैं, क्योंकि उनकी सत्ता जाने का मतलब है, कांग्रेस के सियासी शहंशाहों का कब्जा। दिग्गी राजा से लेकर सिंधिया परिवार तक को लगता है कि उनका तो राजपाट है मध्यप्रदेश। कमोबेश यही स्थति ओड़िशा की है। वहां कांग्रेस या भाजपा खनन के रास्ते लाभ उठाती रहीं और इन्फ्रास्ट्रक्चर चौपट होता रहा। ऐसे में नवीन पटनायक चाहे ओड़िशा में कोई नई धारा अभी तक न बना पाए हों, लेकिन उनके विरोध का मतलब उन्हीं कांग्रेस-भाजपा को जगाना होगा, जिनसे ओड़िशा आहत महसूस करता रहा है। यानी सत्ता ने ही इस दौर में अपनी परिभाषा ऐसी गढ़ी, जिसमें वही जनता हाशिये पर चली गई, जिसके वोट को सहारे लोकतंत्र का गान देश में बीते साठ बरस से लगातार होता रहा है, क्योंकि जो सत्ता में है उसका विकल्प कहीं बदतर है।
सरकार से लोग जितने निराश हैं, विपक्ष को लेकर उससे कम मायूस नहीं हैं, चाहे केंद्र का मामला हो या राज्यों का। यही कारण है कि अब सवाल पूरी संसदीय राजनीति को लेकर उठ रहे हैं और राजनीतिक तौर पर पहली बार लोकतंत्र ही कठघरे में खड़ा दिखता है, क्योंकि जिन माध्यमों के जरिये लोकतंत्र को देश ने कंधे पर बिठाया उन माध्यमों ने ही लोकतंत्र को सत्ता की परछाईं तले ला दिया है और सत्ता ही लोकतंत्र का पर्याय बन गई है। इसलिए, अब यह सवाल उठेगा ही कि जो राजनीतिक व्यवस्था चल रही है, उसमें सत्ता परिवर्तन का मतलब सिर्फ चेहरों की अदला-बदली है और हर चेहरे के पीछे सियासी खेल एक-सा है, फिर आम आदमी या मतदाता कितना मायने रखता है? ऐसे में जो नीतियां बन रही हैं, जो संस्थाएं नीतियों को लागू करवा रही हैं, जो विरोध के स्वर हैं, जो पक्ष की बात कर रहे हैं, जो विपक्ष में बैठे हैं, सभी प्रकारांतर से एक ही हैं।
यानी इस दायरे में राजनेता, नौकरशाही, कॉरपोरेट और स्वायत्त संस्थाएं एक सरीखी हो चली हैं तो फिर बिगड़ी अर्थव्यवस्था या सरकार के कॉरपोरेटीकरण के सवाल का मतलब क्या है और 2014 को लेकर जिस राजनीतिक संघर्ष की तैयारी में सभी राजनीतिक दल ताल ठोंक रहे हैं, वह ताल भी कहीं साझा रणनीति का हिस्सा तो नहीं है, जिससे देश के बहात्तर करोड़ मतदाताओं को लगे कि उनकी भागीदारी के बगैर सत्ता बन नहीं सकती, चाहे 2009 में महज साढ़े ग्यारह करोड़ वोटों के सहारे कांग्रेस देश को लगातार बता रही है कि उसे जनता ने चुना है और पांच बरस तक वह जो भी कर रही है, जनता की नुमाइंदगी करते हुए कर रही है। यह अलग बात है कि इस दौर में जनता सड़क से अपने नुमाइंदों को, संसद को चेताने में लगी है और संसद कह रही है कि यह लोकतंत्र पर हमला है। जनसत्ता से साभार।

 मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश