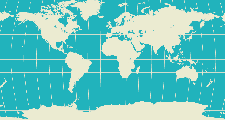अछूत की शिकायत के बहाने

बंधु कुशावर्ती
हीरा डोम (पटना) की लिखी कविता अछूत की शिकायत सन् 1914 में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित की थी। भोजपुरी भाषा/ बोली में लिखी पांच छंदों की इस कविता को खड़ी बोली के उस दौर में पहली दलित रचना होने का श्रेय है। यह कविता डोमवृत्ति में ही रहने का आर्तनाद है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जातियों के बीच अस्पृश्यजनों के साथ होते व्यवहार का भी हीरा डोम की यह कविता अत्यंत प्रामाणिक दस्तावेज प्रस्तुत करती है। बेधरम होकर ईसाई बनना दरअसल धर्मच्युत होने की इस हद की पीड़ा का द्योतक है कि मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे, यानी इधर कुआं और उधर खाईं। ईश्वर भी अस्पृश्यों को छूने से डरता है। ऐसी अभिव्यक्ति को दलित अलम्बरदारों ने हिन्दू और मनुवादी मानसिकता की रचना घोषित कर कबीर, दादू, रैदास आदि की कोटि में डाल दिया। इसी दौर में प्रेमचंद ने उर्दू से हिन्दी में भी कथा लेखन की शुरुआत की है। कहना कठिन है कि प्रेमचंद ने अछूत की शिकायत को पढ़ा होगा। इस कविता के अंतिम तीन छंद प्रेमचंद कृत दलित लेखन के सूत्र हैं। वस्तुतः इसी को लक्ष्य करके मैंने इस कविता के प्रकाशन केदौर में हिन्दी कथा लेखन में पदार्पण करने वाले प्रेमचंद को लेकर दुविधा केसाथ कहा है कि प्रेमचंद ने अछूत की शिकायत कविता को पढ़ा होगा। प्रेमचंद बचपन से ही पाठ्येतर, विशेष रूप से कथा साहित्य पढ़ते रहे हैं,
संदर्भ बताते हैं किन्तु यह सब उर्दू या अंग्रेजी में छपा हुआ रहता था। स्पष्ट है कि प्रेमचंद तब हिन्दी लिखने की तरह पढ़ने के भी अनभ्यस्त थे, लेकिन उनकेसाहित्य का बड़ा हिस्सा अछूत की शिकायत को ही वाणी देता मिलता है। 21वीं सदी की शुरुआत के आसपास इन्हीं प्रेमचंद की रंगभूमि का जलाया जाना कफन, पूस की रात, ठाकुर का कुआं आदि कहानियों को बराबर दलित विमर्श में निशाने पर रखना तथा प्रश्नों के चक्रव्यूह में घेरकर धराशायी करना जिस भी बौद्धिक चेतना के चलते होता आया हो, मुझे वस्तुतः कभी भी विमर्श नहीं लगा, क्योंकि; इस सारे द्रविण- प्राणायाम में हमेशा असहमति और तर्क की प्रखरता की जगह असंतोषपूर्ण वैमनस्य की केंद्रीयता रही है। इस वैमनस्य और असंतोष की आंच भारत सरकार तक को ऐसी महसूस हुई कि गांधी का दिया हरिजन शब्द भी असंवैधानिक करार दिया गया। स्थानापन्न दलित शब्द अब प्रचलन में और सर्वस्वीकृत है, परंतु; क्या यह शब्द सचमुच उस बोध को व्यक्त करता है जिसे हीरा डोम कृत अछूत की शिकायत के पांच छंदों में अभिव्यक्ति मिली है।
सवाल का जवाब मिले, यहां अभीष्ट यह नहीं है। प्रचलन में आ जाने के कारण दलित शब्द से जो बोध स्वीकार्य हो गया है, उस पर सवाल खड़े करने का अब कोई मतलब ही नहीं रह गया है, परंतु; जो विचारशील सौमनस्य दलित विमर्श में रहना चाहिए वही प्रायः अनुपस्थित रहता है। दलित की पीड़ा को दलित ही व्यक्त कर सकता है। इसी सिलसिले में बड़ी टेक है।
दलित जीवन की कदाचित सबसे ज्यादा एवं गहरी संवेदना से लिखी होने केबावजूद प्रेमचंद की एतद्विषयक कहानियां और प्रेमचंद सबसे ज्यादा लानत-मलामत के शिकार हैं। ऐसे ही एक विवाद केबीच श्री लाल शुक्ल ने लगभग एक दशक पहले दलित लेखन में स्वानुभूति और सहानुभूति की दृष्टि से विचार का महत्वपूर्ण सूत्र दिया था परंतु ; इसे भी दलित विमर्शकारों द्वारा ठेंगे पर ही रखा गया है जिसे बौद्धिक विवेक के अनुरूप कतई नहीं कहा या माना जा सकता है।
बहुधा कहा जाता है कि दलितों के विमर्श के अपने मानक है, समीक्षा और आलोचना के अपने औजार हैं और अपना सौंदर्यशास्त्र भी! साहित्य में प्रचलित आलोचना-समीक्षा के और मूल्यांकन के मानक- औजार आदि दलित विमर्श केकाम के नहीं है। राजेंद्र यादव और उन्हीं जैसे सुरैय्ये दलित लेखन में परिपक्वता, तराश आदि पर भी गौर न करने और छूट देते रहने की बात करते रहते हैं, जो संवेदना, अनुभव और अभिव्यक्ति के स्तर पर अंततः लेखन के लिए अनिवार्य है, परंतु यह बलात्, तुष्टिकरण और पक्षधरता के अलावा भला और क्या है?
आज का हिन्दी दलित लेखन भी मराठी की कलम से वस्तुतः अलग क्या है? बीस-पच्चीस वर्षों से ज्यादा हिन्दी में अभी इसकी यात्रा नहीं हुई है। कमलेश्वर ने सारिका के संपादक केरूप में मराठी दलित लेखन के गवाक्ष हिन्दी केलिए सन् 1970-72 में नहीं खोले होते तो हिन्दी का दलित लेखन अभी शायद पालने में होता। और सच तो यह है कि दलितों ने हिन्दी में लिखना शुरू भी नहीं किया। डा. अम्बेडकर को भी हिन्दी केबुद्धिजीवियों और दलित बुद्धिजीवियों द्वारा भी बीती सदी में 90 से पहले कितना पढ़ा-गुना गया है? ईमानदारी की बात तो यह है कि स्वयं हिन्दी का समीक्षा और आलोचनाशास्त्र संस्कृत, कविता मार्क्सवादी या विदेशी समीक्षा आलोचनाशास्त्र से सचमुच कितना आत्मविकसित और स्वायत्त रहा है?
स्वयं हिन्दी में प्रगतिशील आंदोलन का प्रादुर्भाव विदेशी जमीन से हुआ। संयोग से अधिक प्रेमचंद की नौजवानों को प्रोत्साहित करने की सदाशयी प्रवृत्ति बड़ा कारण है कि उन्होंने दूरंदेशी का ख्याल रखते हुए प्रगतिशील लेखक संगठन के आयोजन (लखनऊ, अप्रैल 1936) की अध्यक्षता की। सांगठनिक स्तर पर प्रेमचंद को सज्जाद जहीर, मुल्कराज आनंद आदि ने सम्यक-विधिवत् रूप से अपने से न तो जोड़ा था और न एकाध बैठकों के अपवाद से ज्यादा पूछा या अपने साथ शामिल ही किया था। प्रेमचंद पहले भी इन सबकी तरह मार्क्सवादी सोच व दल से नहीं जुड़े रहे। उन्होंने ऐसी किसी पार्टी का सदस्य होने से भी इनकार किया है। अन्यथा सन् 1924-25 से भारत में आयी कम्युनिस्ट पार्टी से सीधे जुड़ने से उन्हें कौन रोक सकता था? हां, प्रगतिशील लेखक संघ के लखनऊ सम्मेलन की अध्यक्षता केबाद उनका निधन ऐसी पराकाष्ठा था कि वह संघ और कम्युनिस्ट, दोनों ही उन्हें अपने हद में कंधों पर उठाए रहे।
प्रेमचंद जीवित होते तो अमृतराय की तरह कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य न ही बनते और खुदा-न-ख्वास्ता बनते भी अगर तो कौन कह सकता है कि राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, पीसी जोशी वगैरह की तरह पार्टी बदर न किए जाते? बताने की जरूरत नहीं है कि कम्युनिस्ट पार्टी का सैद्धांतिक वर्चस्व, विवेकशील सृजनात्मक सोच और विचारशीलता के प्रति अधिकांशतः कितना अनुदार, अव्यावहारिक और असंवेदनशील रवैये से लबरेज रहा है। इस सारे क्रम में हिन्दी के दलित लेखन और दलित बुद्धिजीवियों एवं विमर्शकारों का आकलन करें तो पाते हैं कि वे सृजन और विचार की यात्रा में हैं। परिपक्वता और पुख्तगी की वह मंजिल जहां उसका अपना सौंदर्यशास्त्र समीक्षा और आलोचनाशास्त्रों, अभी दूर भले न हो किन्तु नजदीक भी नहीं है। मील का पत्थर जैसी कोई रचना भी फिलवक्त उसकेहिस्से में नहीं है, परंतु नहीं होगी, यह कैसे कहा जा सकता है। ऐसे में कम्युनिस्ट पार्टी की हाईलाइनर यानि कट्टरप्रकृति केसाथ अपने एवं दलितेत्तर रचनाओं तथा रचनाकारों केप्रति असहिष्णुता की हद तक जाकर भी सख्त रवैया अख्तियार किए हुए विमर्श करना सृजनात्मक और संवेदना सजग प्रवृत्ति को प्रमाणित कतई नहीं करता। हां, प्रेमचंद के कफन जैसे शीर्षक को लेकर एक दलित द्वारा लिखी गई कहानी को कफन से ज्यादा बड़ी यानि की बड़ी लकीर खींच देने की बचकानी खुशफहमियां जरूर उभार पर है। क्या इस सबमें वह संजीदगी, गहराई, गंभीरता और संवेदना का लेशमात्र भी है, जो रचना और रचनाकार के व्यक्तित्व, दोनों को ऊंचाई और बड़ा कद देता है। हीरा डोम की अछूत की शिकायत में पीड़ा की गहरी अनुभूति का जैसा विस्फोट है, अपने पूरे समाज की लहरों की जैसी मर्मान्तक हिलोर है, सदियों की उपेक्षा-अपमान आदि.... मात्र 40 पंक्तियों में, पांच छंदों में जिस स्फीति केसाथ सिमट आए हैं, पिछले 20-25 वर्षों के स्वानुभूति के दलित लेखन में वह अभिव्यक्त हो पाया है क्या? आत्ममुग्धता और बड़बोलेपन से यह गंभीरता से विचार करने का विषय है।
बहुत आसान है कबीर, रैदास, दादू आदि के खाते में हीरा डोम और उनकी इस कविता को भी डाल देना परंतु; कबीर, रैदास, दादू 20वीं सदी और हीरा डोम आज की 21वीं सदी की उपज नहीं थे। इसे पूरी शिद्दत से याद रखना चाहिए।

 मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश