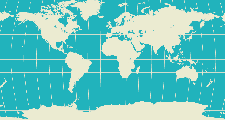
а§Ча•Ба§∞а•В-৙а•Ва§∞а•На§£а§ња§Ѓа§Њ а§Ха•З а§Е৶а•Н৵ৃ ৙а•На§∞১а•Аа§Х а§Ха•Л а§ђа§Ња§∞а§Ва§ђа§Ња§∞ ৮ু৪а•На§Ха§Ња§∞!
Friday 19 July 2013 12:27:34 PM

а§єа•Г৶ৃ৮ৌа§∞а§Ња§ѓа§£ ৶а•Аа§Ха•Нৣড়১

а§єа§Ѓ а§≠а§Ња§∞১ а§Ха•З а§≤а•Ла§Ч ৮ а§Ьৌ৮а•З а§Хড়১৮а•З а§Ь৮а•На§Ѓа•Ла§В а§Єа•З ৙а•На§∞а§Хৌ৴ а§Еа§≠а•А৙а•На§Єа•Б а§єа•Иа§Ља§Ва•§ ৙а•На§∞а§Хৌ৴ а§єа§Ѓ а§Єа§ђа§Ха•Л а§≤а§єа§Ња§≤а•Ла§Я а§Ха§∞১ৌ а§єа•Иа•§ ৙а•Ва§∞а§ђ а§Ѓа•За§В а§Ка§Ја§Њ а§Жа§Иа•§ а§≠а•Ла§∞ а§Ха•З ৙৺а§≤а•З, а§∞ৌ১а•На§∞а§њ ৶а•З৵а•А ৵ড়৶ৌа§И а§≤а•З а§∞а§єа•А а§єа•Иа§Ва•§ а§Ха•Нৣড়১ড়а§Ь а§Еа§∞а•Ва§£ а§єа•Л а§∞а§єа•З а§єа•Иа§Ва•§ а§єа§Ѓа§Ња§∞а•З ৙а•Ва§∞а•Н৵а§Ьа•Ла§В ৮а•З а§Ка§Ја§Њ а§Ха•А а§Жа§≠а§Њ а§Ха•Л ৙а•На§∞а§£а§Ња§Ѓ а§Ха§ња§ѓа§Ња•§ а§Ђа§ња§∞ а§Жа§П а§Єа•Ва§∞а•На§ѓа•§ ৵а•И৶ড়а§Х а§Ла§Ја§ња§ѓа•Ла§В а§Ха•З а§≤а§Ња§°а§Ља§≤а•З ৶а•З৵ а§Єа§µа§ња§§а§Ња•§ ৺ু৮а•З а§Й৮৪а•З 'а§Ьа•На§Юৌ৮ ৙а•На§∞а§Хৌ৴- а§Іа•Аа§Ѓа§єа§ња§Іа§ња§ѓа•Л' а§Ѓа§Ња§Ва§Ча§Ња•§ ৵а•З а§Єа§Ња§ѓа§Ва§Ха§Ња§≤ а§Ъа§≤а•З ৵ড়৴а•На§∞а§Ња§Ѓ а§Ха•А а§Уа§∞а•§ ৺ু৮а•З а§Єа§Ва§Іа•На§ѓа§Њ а§Ха•А ৵а•За§≤а§Њ а§Ѓа•За§В а§Й৮а•На§єа•За§В а§Ђа§ња§∞ а§Єа•З ৮ু৪а•На§Ха§Ња§∞ а§Ха§ња§ѓа§Ња•§ ৶ড়৵৪ ৙а•На§∞а§Хৌ৴ а§єа•И а§Фа§∞ а§∞ৌ১а•На§∞а§њ ১ু৪а•На•§ а§Єа•Ва§∞а•На§ѓ ৶а•З৵ а§∞ৌ১а•На§∞а§њ а§Ѓа•За§В ৮৺а•Аа§В а§Йа§Ч১а•За•§ а§Йа§Ч১а•З ১а•Л а§∞ৌ১ ৮ а§єа•Л১а•Аа•§ а§∞ৌ১а•На§∞а§њ а§Ѓа•За§В ৙а•На§∞а§Хৌ৴ ৶а•З৮а•З а§Ха§Њ а§Ха§Ња§Ѓ а§Єа•Ва§∞а•На§ѓ а§Єа•З а§Ка§∞а•На§Ьа§Њ а§≤а•За§Ха§∞ а§Ъа§В৶а•На§∞а§Ѓа§Њ а§Ха§∞১ৌ а§єа•Иа•§ ৵а•Иа§Ьа•На§Юৌ৮ড়а§Ха•Ла§В ৮а•З а§Єа•Ма§∞ а§Ка§∞а•На§Ьа§Њ а§Ха•З ৙а•На§∞а§Хৌ৴ а§Й৙а§Ха§∞а§£ а§Еа§ђ а§Ца•Ла§Ьа•З а§єа•Иа§Ва•§ ৙а•На§∞а§Ха•Г১ড় а§Ѓа•За§В а§Єа•Ма§∞ а§Ка§∞а•На§Ьа§Њ а§Єа•З ৶а•А৙ড়১ а§Ъа§В৶а•На§∞ а§Ха§ња§∞а§£а•За§В ৮ а§Ьৌ৮а•З а§Ха§ђ а§Єа•З а§Еа§Ѓа•Г১а§∞а§Є а§ђа§∞а§Єа§Њ а§∞а§єа•А а§єа•Иа§В, а§≤а•За§Хড়৮ а§Ъа§В৶а•На§∞а§Ѓа§Њ а§≤а§Чৌ১ৌа§∞ а§Ша§Я১ৌ ৐৥৊১ৌ а§єа•Иа•§ а§Ша§Я৮а•З а§Ха§Њ а§Еа§В১ড়ু ৙ৰ৊ৌ৵ а§Еুৌ৵৪а•На§ѓа§Њ а§єа•И а§Фа§∞ ৙а•На§∞а§Хৌ৴ а§Ха§Њ а§Ъа§∞а§Ѓ ৙а•Ва§∞а•На§£а§ња§Ѓа§Ња•§ а§≠а§Ња§∞১ ৮а•З ৶а•Л৮а•Л а§Ха•Л ৙а•На§ѓа§Ња§∞ а§Ха§ња§ѓа§Њ а§єа•Иа•§ ৶а•А৙৙а§∞а•Н৵ а§Ч৺৮ а§Еুৌ৵৪ ৵ৌа§≤а•А а§∞ৌ১а•На§∞а§њ а§Ха•Л а§єа•А а§∞а§Ца§Њ, а§єа§∞а•За§Х а§Еুৌ৵৪ а§Ха•Л а§Єа•Н৮ৌ৮ ৵а•На§∞১ а§Ха•З а§Е৮а•Ба§Ја•Н৆ৌ৮ а§∞а§Ца•З, а§≤а•За§Хড়৮ ৙а•Ва§∞а•На§£а§ња§Ѓа§Њ а§Ха•А а§Ца•Б৴а•А а§Ха•А ৐ৌ১ а§єа•А ৶а•Ва§Єа§∞а•А а§єа•Иа•§ ৴а§∞৶ ৙а•Ва§∞а•На§£а§ња§Ѓа§Њ а§Еа§Ѓа•Г১а§∞а§Є ৶а•З১а•А а§єа•Иа•§ а§Ха§Ња§∞а•Н১ড়а§Ха•А ৙а•Ба§£а•На§ѓ ৙а•На§∞а§§а§Ња§™а•§ а§Еৣৌ৥৊ ৙а•Ва§∞а•На§£а§ња§Ѓа§Њ ৐ৌ৶а§≤а•Ла§В а§Єа•З ৥а§Ха•З а§Ж৪ুৌ৮ а§Ха•З ৐ৌ৵а§Ьа•В৶ а§Ца§ња§≤১а•А а§єа•Иа•§ а§≠а§Ња§∞১ ৮а•З а§Йа§Єа•З а§Ча•Ба§∞а•В ৙а•Ва§∞а•На§£а§ња§Ѓа§Њ а§Ха§єа§Ња•§ ৙а•Ва§∞а•На§£а§ња§Ѓа§Њ а§≠а§Ња§∞১ а§Ха•З ু৮ а§Ха•А ৙а•На§∞ড়ৃ১ুৌ а§єа•Иа•§ а§Ла§Ча•Н৵а•З৶ а§Ха•З а§Ла§Ја§њ ৮а•З а§Ъа§В৶а•На§∞а§Ѓа§Њ а§Ха•Л а§Ьа§Ч১ а§Ха§Њ ু৮ ৐১ৌৃৌ а§єа•И-а§Ъа§В৶а•На§∞а§Ѓа§Њ ু৮ а§Єа•Л а§Ьа§Ња§§а§Ња•§
а§Ча•Ба§∞а•В ৵ড়৵а•За§Х а§єа•И, а§Ъа§В৶а•На§∞а§Ѓа§Њ ু৮ а§єа•Иа•§ а§ђа§°а§Ља§Њ ৙а•На§ѓа§Ња§∞а§Њ ৴৐а•Н৶ а§єа•И а§Ча•Ба§∞а•Ва•§ а§Ча•Ба§∞а•В১а•Н৵ а§За§Єа•А а§Єа•З а§Йа§Ча§Њ а§єа•И а§Фа§∞ а§За§Єа•А а§Ха§Њ ৵ড়৪а•Н১ৌа§∞ а§єа•И а§Ча•Ба§∞а•В১а•Н৵ৌа§Ха§∞а•На§Ја§£а•§ а§ѓа•Ла§В а§Ча•Ба§∞а•В১а•Н৵ৌа§Ха§∞а•На§Ја§£ а§Ха•Л ৙а•Г৕а•Н৵а•А а§Ха§Њ а§Жа§Ха§∞а•На§Ја§£ а§Ха§єа§Њ а§Ьৌ১ৌ а§єа•И, а§≤а•За§Хড়৮ а§За§Єа§Ха§Њ а§Ѓа•Ва§≤ а§Еа§∞а•Н৕ а§≠а§Ња§∞ а§Ха§Њ а§Жа§Ха§∞а•На§Ја§£ а§єа•Иа•§ а§Ча•Ба§∞а•В ৙а•На§∞а•А১ড়৙а•Ва§∞а•На§£ а§Е৵৲ৌа§∞а§£а§Њ а§єа•Иа•§ а§Йа§Єа§Ѓа•За§В а§Ча•Ба§∞а•В১а•Н৵ а§єа•И, а§≤а•За§Хড়৮ а§За§Єа§Ха§Њ а§Єа§Ва§Ч а§єа§Ѓа§Ха•Л ৮ড়а§∞а•На§≠а§Ња§∞ а§Ха§∞১ৌ а§єа•И, а§Ѓа•Ба§Ха•Н১ а§Ха§∞১ৌ а§єа•Иа•§ ৵ড়৴а•Н৵ а§Ха•А а§Ха§ња§Єа•А а§≠а•А а§Єа§≠а•Нৃ১ৌ а§Ѓа•За§В 'а§Ча•Ба§∞а•В' а§Ьа•Иа§Єа§Њ ৙а•На§∞১а•Аа§Х ৮৺а•Аа§В а§єа•Иа•§ ৙ৌ৶а§∞а•А а§Ча•Ба§∞а•В ৮৺а•Аа§В а§єа•Иа§В, ৵а•З а§Иа§Єа§Ња§Зৃ১ а§Ха•А ৴ড়а§Ха•На§Ја§Њ ৶а•З১а•З а§єа•Иа§Ва•§ а§Ѓа•Ма§≤৵а•А а§≠а•А а§Ча•Ба§∞а•В ৮৺а•Аа§В а§єа•Иа§В, ৵а•З а§За§Єа•На§≤а§Ња§Ѓа•А а§Ьа•На§Юৌ৮ ৶а•З১а•З а§єа•Иа§Ва•§ ৙ৌ৶а§∞а•А а§Фа§∞ а§Ѓа•Ма§≤৵а•А а§ђа§Ња§В৲১а•З а§єа•Иа§В а§Е৙৮а•А а§Жа§Єа•Н৕ৌ а§Ѓа•За§В, а§≤а•За§Хড়৮ а§Ча•Ба§∞а•В а§Ѓа•Ба§Ха•Н১ а§Ха§∞১ৌ а§єа•Иа•§ а§Ча•Ба§∞а•В ৴ড়ৣа•На§ѓ а§Ха•Л ৶а•Ва§Єа§∞а§Њ а§Ь৮а•На§Ѓ ৶а•З১ৌ а§єа•Иа•§ а§Па§Х а§Ь৮а•На§Ѓ а§Ѓа§ња§≤১ৌ а§єа•И ুৌ১ৌ-৙ড়১ৌ а§Єа•За•§ а§Ча•Ба§∞а•В ৶а•Ва§Єа§∞а§Њ а§Ь৮а•На§Ѓ ৶а•З১ৌ а§єа•Иа•§ а§Ча•Ба§∞а•В ৶а•Н৵ড়а§Ь ৐৮ৌ১ৌ а§єа•Иа•§ а§Е৕а§∞а•Н৵৵а•З৶ а§Ха•З а§Єа•Ба§В৶а§∞ а§Єа•Ва§Ха•Н১ (11.7) а§Ѓа•За§В а§Х৺১а•З а§єа•Иа§В, а§Ча•Ба§∞а•В а§Йа§Єа•З ১а•А৮ а§∞ৌ১ ১а§Х а§Ьа•На§Юৌ৮ а§Ча§∞а•На§≠ а§Ѓа•За§В а§∞а§Ц১а•З а§єа•Иа§В, а§Ьа§ђ ৵৺ а§ђа§Ња§єа§∞ а§Ж১ৌ а§єа•И, ৶ড়৵а•На§ѓ ৴а§Ха•Н১ড়ৃৌа§В а§Йа§Єа§Ха§Њ а§Еа§≠ড়৮а§В৶৮ а§Ха§∞১а•А а§єа•Иа§Ва•§'' а§Ьа•На§Юৌ৮ а§Ча§∞а•На§≠ а§Ца•Ва§ђа§Єа•Ва§∞১ ৙а•На§∞১а•Аа§Х а§єа•Иа•§ а§Ѓа§Ња§В а§Ха§Њ а§Ча§∞а•На§≠ а§єа§Ѓа§Ха•Л ৙а•На§∞а§Ња§£ а§Фа§∞ а§Ха§Ња§ѓа§Њ ৶а•З১ৌ а§єа•Иа•§ а§Ча•Ба§∞а•В а§Ха§Њ а§Ьа•На§Юৌ৮а§Ча§∞а•На§≠ а§єа§Ѓа§Ха•Л а§ђа•Ла§І ৶а•З১ৌ а§єа•И а§Фа§∞ ৶а•Н৵ড়а§Ь ৐৮ৌ১ৌ а§єа•Иа•§ а§Й৙৮ড়ৣ৶ а§Ха•З а§Ла§Ја§њ а§Х৺১а•З а§єа•Иа§В, а§Ча•Ба§∞а•Ва§∞а•З৵ ৙а§∞а§Ѓ а§Іа§∞а•На§Ѓа•Л, а§Ча•Ба§∞а•Ва§∞а•З৵ ৙а§∞а§Њ а§Ч১ড়-а§Ча•Ба§∞а•В ৙а§∞а§Ѓа§Іа§∞а•На§Ѓ а§єа•И а§Фа§∞ ৵৺а•А ৙а§∞а§Њ-а§Ч১ড় а§єа•Иа•§'' а§Й৙৮ড়ৣ৶а•На§Ха§Ња§∞ ৮а•З а§Іа§∞а•На§Ѓ ৮৺а•Аа§В ৙а§∞а§Ѓа§Іа§∞а•На§Ѓ а§Ха§єа§Њ а§єа•И а§Фа§∞ а§Ч১ড় а§Ха•З а§≠а•А ৙৺а§≤а•З ৙а§∞а§Њ ৴৐а•Н৶ а§Ха§Њ ৙а•На§∞а§ѓа•Ла§Ч а§Ха§ња§ѓа§Њ а§єа•Иа•§ ১а•Л ৙а§∞а§Ѓ а§Іа§∞а•На§Ѓ а§Ха•На§ѓа§Њ а§єа•И? а§Іа§∞а•На§Ѓ ৵а•На§ѓа§Ха•Н১ড় а§Фа§∞ а§≤а•Ла§Х а§Ха•З а§Єа§Ва§ђа§Ва§Іа•Ла§В а§Ха•А а§Жа§Ъа§Ња§∞ а§Єа§В৺ড়১ৌ а§єа•И, а§ѓа§є ৵а•На§ѓа§Ха•Н১ড় а§Фа§∞ а§≤а•Ла§Х а§Ха•З а§Ѓа§Іа•На§ѓ а§Еа§В১а§∞а•На§Єа§Ва§Ча•А১ а§Ха§Њ а§Ыа§В৶৪а•Н а§єа•Иа•§ ৙а§∞а§Ѓа§Іа§∞а•На§Ѓ а§За§Є а§Іа§∞а•На§Ѓ а§Ха§Њ а§Е১ড়а§Ха•На§∞а§Ѓа§£ а§єа•Иа•§ а§Іа§∞а•На§Ѓ а§Ьа•А৵৮ а§Ха§Њ ৙а•Ба§Ја•Н৙ а§єа•И а§Фа§∞ ৙а§∞а§Ѓа§Іа§∞а•На§Ѓ ৙а§∞а§Ња§Ча•§ а§Ьа•Иа§Єа•З ৙а§∞а§Ња§Ч а§Ђа•Ва§≤ а§Ха§Њ а§Єа§∞а•Н৵а•Л১а•Н১ু а§∞а§Є а§єа•И, ৵а•Иа§Єа•З а§єа•А ৙а§∞а§Ѓа§Іа§∞а•На§Ѓ а§Іа§∞а•На§Ѓ а§Ха§Њ ৴ড়а§Ца§∞а•§ ৙а§∞а§Ѓа§Іа§∞а•На§Ѓ а§Па§Хৌ১а•На§Ѓ а§Е৮а•Ба§≠а•В১ড় а§єа•Иа•§
а§Ьа§Ч১ а§Ч১ড়৴а•Аа§≤ а§єа•Иа•§ а§Ч১ড় а§Єа•Н৵ৌа§≠ৌ৵ড়а§Х ৮ড়ৃ১ড় а§єа•Иа•§ а§ђа•Ба§∞а•А а§Ч১ড় ৶а•Ба§∞а•На§Ч১ড় а§єа•Иа•§ а§Йа§Ъড়১ ৶ড়৴ৌ а§Ѓа•За§В а§Ч১ড় ৙а•На§∞а§Ч১ড় а§єа•Иа•§ ৪১а•На§ѓ ৶ড়৴ৌ а§Ха•А а§Ч১ড় ৪৶а•На§Ч১ড় а§єа•И, ১৐ а§Й৙৮ড়ৣ৶а•Н ৵ৌа§≤а•А ৙а§∞а§Ња§Ч১ড় а§Ха•На§ѓа§Њ а§єа•И? а§Єа§Ња§∞а•А а§Ч১ড়ৃৌа§В а§Ъа§Ха•На§∞ৌ৮а•Б৵а§∞а•Н১а•А а§єа•Иа§Ва•§ а§єа§Ѓ а§Ха§єа•Аа§В а§Єа•З а§Ъа§≤а•За§В, а§Ъа§≤১а•З а§єа•А а§∞а§єа•За§В ১а•Л ৵৺а•Аа§В ৙৺а•Ба§Ва§Ъа•За§Ва§Ча•З, а§Ьа§єа§Ња§В а§Єа•З а§Ъа§≤а•З ৕а•За•§ а§Ра§Єа•А а§Ч১ড় а§Ха§Њ а§Ха•На§ѓа§Њ а§≤а§Ња§≠? а§Ъа§≤а•З а§≠а•А, ৕а§Ха•З а§≠а•А, а§Яа•Ва§Яа•З а§Фа§∞ а§ђа•Б৥৊ৌа§П а§≠а•А, а§≤а•За§Хড়৮ ৙৺а•Ба§Ва§Ъа•З а§Ха§єа•Аа§В ৮৺а•Аа§Ва•§ а§Ѓа•Иа§В а§∞а§Ња§Ь৮а•А১ড় а§Ѓа•За§В а§Ч১ড়৴а•Аа§≤ а§єа•Ва§Ва•§ а§Ь৵ৌ৮а•А а§Ѓа•За§В а§Ѓа§Ва§Ъ, а§Ѓа§Ња§≤а§Њ, а§Ѓа§Ња§За§Х а§Ха•З а§Жа§Ха§∞а•На§Ја§£ ৕а•За•§ а§Еа§В১а§∞а•Н৶а§≤а•Аа§ѓ а§Єа§ња§∞ а§Ђа•Ба§Яа•М৵а§≤ ৕а•Аа•§ ৵ড়৙а§Ха•На§Ја•А ৙а§∞ а§Жа§Ха•На§∞а§Ѓа§£ ৕а•За•§ а§єа§Ѓ а§Ъа§≤১а•З а§Ча§П, ৐৥৊১а•З а§Ча§П, а§≤а•За§Хড়৮ а§Ѓа§Ва§Ъ, а§Ѓа§Ња§≤а§Њ, а§Ѓа§Ња§За§Х а§Фа§∞ ৃ৴ а§≤а•Ла§≠ а§Ьа§Є а§Ха•З ১৪ а§єа•Иа§Ва•§ а§Ьа•А৵৮ а§Ха•А а§Ча§Ња§°а§Ља•А а§Йа§Єа•А а§Єа•На§Яа•З৴৮ ৙а§∞ а§≤а•Ма§Я а§Жа§И, а§Ьа§єа§Ња§В а§Єа•З а§Ъа§≤а•А ৕а•Аа•§ '৙а§∞а§Ња§Ч১ড়' а§Ра§Єа•А а§Ч১ড় а§Ха§Њ а§Е১ড়а§Ха•На§∞а§Ѓа§£ а§єа•Иа•§ а§Й৙৮ড়ৣ৶а•Н а§Ха•З а§Ла§Ја§њ ৮а•З а§Ча•Ба§∞а•В а§Ха•Л '৙а§∞а§Ња§Ч১ড়' ৐১ৌৃৌ а§єа•Иа•§ а§Ча•Ба§∞а•В а§Ха§Њ а§Єа§Ва§Єа•Н৙а§∞а•Н৴ а§Ж১а•На§Ѓа§ђа•Ла§І а§Ьа§Чৌ১ৌ а§єа•Иа•§ а§Ъа§Ха•На§∞а•Аа§ѓ а§Ч১ড় а§Єа•З а§ђа§Ња§єа§∞ а§Ха§∞১ৌ а§єа•Иа•§ а§Ч১ড় а§Ха•З ৙ৌа§∞ а§≤а•З а§Ьৌ১ৌ а§єа•Иа•§ ৙а§∞а§Ња§Ч১ড় ৵৪а•Н১а•Б১: а§Ха•Ла§И а§Ч১ড় ৮৺а•Аа§Ва•§
а§Ча•Ба§∞а•В а§Ка§∞а•На§Ьа§Њ а§Ха§Њ а§ђа§°а§Ља§Њ а§ђа§ња§В৶а•Б а§єа•Иа•§ ৵৺ ৵ড়а§∞а§Ња§Я а§ђа•На§∞а§єа•На§Ѓ а§Ха•А а§Ка§∞а•На§Ьа§Њ а§Єа•З а§Єа•Аа§Іа•З а§Ьа•Ба§°а§Ља§Њ а§єа•Ба§Ж а§єа•Иа•§ ৴ড়ৣа•На§ѓ а§Ка§∞а•На§Ьа§Њ а§Ха§Њ а§Ыа•Ла§Яа§Њ ৙ড়а§Ва§° а§єа•И, а§≤а•За§Хড়৮ ৵৺ ৵ড়а§∞а§Ња§Я а§Єа•З а§Єа•Аа§Іа•З а§Ка§∞а•На§Ьа§Њ а§≤а•З৮а•З а§Ѓа•За§В а§Єа§Ха•На§Ја§Ѓ ৮৺а•Аа§В а§єа•Иа•§ а§Е৙৮а•А а§Е৙৮а•А а§Ча•На§∞а§Ња§єа•Нৃ১ৌ а§єа•Иа•§ а§Ча•Ба§∞а•В ু৺ৌ৙ৌ৵а§∞ а§єа§Ња§Йа§Є а§Єа•З а§Єа•Аа§Іа•З а§Ьа•Бৰ৊১ৌ а§єа•Иа•§ а§Ка§∞а•На§Ьа§Њ а§≤а•З১ৌ а§єа•И, а§Яа•На§∞а§Ња§Ва§Єа§Ђа§Ња§∞а•На§Ѓа§∞ ৐৮১ৌ а§єа•Иа•§ ৴ড়ৣа•На§ѓ а§Ха•Л а§Яа•На§∞а§Ња§Ва§Єа§Ђа§Ња§∞а•На§Ѓа§∞ а§Ча•Ба§∞а•В а§Єа•З а§Ка§∞а•На§Ьа§Њ а§≤а•З৮а•З а§Ѓа•За§В а§Єа•Б৵ড়৲ৌ а§єа•Иа•§ ৴ড়ৣа•На§ѓ а§Ча•Ба§∞а•В а§Єа•З а§Ьа•Бৰ৊১ৌ а§єа•Иа•§ а§Ча•Ба§∞а•В ৴ড়ৣа•На§ѓ а§Ѓа•За§В ৙а•На§∞৵ৌ৺ড়১ а§єа•Л১ৌ а§єа•Иа•§ ৴ড়ৣа•На§ѓ а§єа•Л৮ৌ а§Єа•Н৵а§≠ৌ৵ а§єа•Иа•§ ৴ড়ৣа•На§ѓ а§Еа§∞а•Н৕ৌ১ а§Єа•Аа§Ц৮а•З а§Ха•Л ৪৶ৌ ১а•Иа§ѓа§Ња§∞а•§ а§Ьа§ђ а§Єа•Аа§Ц৮а•З а§Ха•А ১১а•Н৙а§∞১ৌ а§Єа•Н৵а§≠ৌ৵ ৐৮ а§Ьৌ১а•А а§єа•И, ১а•Л а§Єа§Ња§∞а§Њ а§Еа§Єа•Н১ড়১а•Н৵ а§Ча•Ба§∞а•В ৐৮ а§Ьৌ১ৌ а§єа•Иа•§ а§Іа§∞১а•А, а§Жа§Хৌ৴, а§Єа•Ва§∞а•На§ѓ, а§Ъа§В৶а•На§∞, а§Еа§Ча•Н৮ড়, ৵ৌৃа•Б а§Фа§∞ а§Ьа§≤ а§≠а•А а§Ча•Ба§∞а•В а§єа•Л а§Ьৌ১а•З а§єа•Иа§В, ১৐ а§За§Єа§Ха•З а§≤а§ња§П а§Ьа§∞а•Ва§∞а•А а§єа•И, а§Ка§Ва§Ъа•З ১а§≤ а§Єа•З ৙а•На§∞৵ৌ৺ а§Фа§∞ ৮а•Аа§Ъа•З а§Ха•З ১а§≤ ৙а§∞ а§Єа•Н৵а•Аа§Ха§Ња§∞а•§ а§К৙а§∞ а§Єа•З а§Е৮а•Ба§Ха§В৙ৌ, ৮а•Аа§Ъа•З а§Єа•З ৲৮а•Нৃ৵ৌ৶ а§≠а§Ња§µа•§ а§Ка§∞а•На§Ьа§Њ а§ђа§°а§Ља•З а§Ка§∞а•На§Ьа§Њ ৙ড়а§Ва§° а§Єа•З а§Ыа•Ла§Яа•З а§Ка§∞а•На§Ьа§Њ ৙ড়а§Ва§° а§Ха•Л ৐৺১а•А а§єа•Иа•§ ৵ড়а§Ьа•На§Юৌ৮ а§ѓа§є ৪ড়৶а•На§І а§Ха§∞ а§Ъа•Ба§Ха§Њ а§єа•Иа•§ а§ѓа§є ৵ড়а§Ьа•На§Юৌ৮ а§Ха§Њ ৮ড়ৃু ৮৺а•Аа§В а§єа•Иа•§ ৮ড়ৃু ৙а•На§∞а§Ха•Г১ড় а§Ха§Њ а§єа•И, ৵а•Иа§Ьа•На§Юৌ৮ড়а§Х ৮а•З ৶а•За§Ца§Њ а§єа•Иа•§ ৵а•Иа§Ьа•На§Юৌ৮ড়а§Х ৙а•На§∞а§Ха•Г১ড় ৙а•На§∞৵ৌ৺ а§Ха•З ৮ড়ৃু ৶а•За§Ц а§Єа§Х১а•З а§єа•Иа§Ва•§ а§Ла§Ја§њ а§Ъа•З১৮ а§Ха•А а§Ч১ড় а§≠а•А ৶а•За§Ц১а•З а§∞а§єа•З а§єа•Иа§Ва•§ а§Ча•Ба§∞а•В а§Фа§∞ ৴ড়ৣа•На§ѓ а§Ха•А ৙а•На§∞а•А১ড় а§Ла§Ја§њ а§Е৮а•Ба§≠а•В১ড় а§єа•Иа•§ а§Й১а•Н১а§∞ ৵а•И৶ড়а§Х а§Ха§Ња§≤ а§Ха•З а§Ж৴а•На§∞а§Ѓа•Ла§В а§Ѓа•За§В а§Ча•Ба§∞а•В ৴ড়ৣа•На§ѓ а§Ха•А ৙а•На§∞а•А১ড় ৥а§≤১а•А ৕а•Аа•§ ৶а•Л৮а•Ла§В ৪ৌ৕-৪ৌ৕ а§Єа•Н১а•Б১ড় а§Ха§∞১а•З ৕а•З, а§У3а§Ѓа•Н ৪৺৮ৌ৵৵১а•Б, ৪৺৮а•М а§≠а•Б৮а§Ха•Н১а•Б-৪ৌ৕ ৪ৌ৕ а§єа•Л৮а•З, ৪ৌ৕ ৪ৌ৕ а§Єа•Аа§Ц৮а•З, а§Цৌ৮а•З а§Фа§∞ а§Уа§Ьа§Єа•Н৵а•А ৃ৴৪а•Н৵а•А а§єа•Л৮а•З а§Ха•Аа•§ ১৐ а§Ча•Ба§∞а•В а§Ѓа§Іа•Ба§Ѓа§ѓ ৕а•З, ৴ড়ৣа•На§ѓ а§Ѓа§Іа•Бু১а•Н১ ৕а•За•§ а§Ча•Ба§∞а•В ৙а•На§∞৪ৌ৶ ৙а•Ва§∞а•На§£ ৕а•З, ৴ড়ৣа•На§ѓ ৙а•На§∞৪ৌ৶ а§Еа§≠а•А৙а•На§Єа•Б ৕а•За•§ а§Ча•Ба§∞а•В а§Ла§Ха•Н ৕а•З,৴ড়ৣа•На§ѓ а§Єа§Ња§Ѓ ৕а•За•§ а§Ча•Ба§∞а•В а§Єа•Ва§∞а•На§ѓ ৕а•З, ৴ড়ৣа•На§ѓ а§Ъа§В৶а•На§∞ ৕а•За•§ а§Ча•Ба§∞а•В а§Ѓа•За§В ৙а•Ва§∞а•На§£а§ња§Ѓа§Њ ৶а•За§Ц৮ৌ ৴ড়ৣа•На§ѓ а§Ха•А а§Е৙৮а•А а§Ъа§В৶а•На§∞а§Е৮а•Ба§≠а•В১ড় а§єа•Иа•§
а§Ча•Ба§∞а•В ৙а•Ва§∞а•На§£а§ња§Ѓа§Њ а§єа•А а§єа•Л а§Єа§Х১ৌ а§єа•Иа•§ а§Еа§Ва§Іа§Ха§Ња§∞ а§єа§Ѓа§Ња§∞а§Њ а§Ч৺৮ а§Е৮а•Ба§≠৵ а§єа•Иа•§ а§Ѓа§Ња§В а§Ха•З а§Ча§∞а•На§≠ а§Ѓа•За§В а§Ша•Ла§∞ а§Еа§Ва§Іа§Ха§Ња§∞ а§Ѓа•За§В ৺ু৮а•З ৪৮а•На§ѓа§Ња§Є а§Ьа•Иа§Єа•З а§Єа•Ба§Ц ৙ৌа§П а§єа•Иа§Ва•§ ৮ а§≠а•Ла§Ь৮ а§Ха•А ৙а§∞৵ৌ৺ а§Фа§∞ ৮ а§Ша§∞ а§Ха•Аа•§ а§Еа§єа§Ва§Ха§Ња§∞ а§Ха•З ৶а§В৴ ৕а•З ৮৺а•Аа§Ва•§ а§Єа§ђ а§Ѓа§Ња§В ৙а§∞ а§•а§Ња•§ а§єа§Ѓ а§Ѓа§Ња§В а§Ѓа•За§В ৕а•З, а§Ѓа§Ња§В а§єа§Ѓа§Ѓа•З ৕а•Аа•§ а§Ьа§Ч১ а§Ѓа•За§В а§Жа§П ১а•Л а§Єа•Ва§∞а•На§ѓ ৙а•На§∞а§Хৌ৴ а§Єа•З ৪ৌু৮ৌ а§єа•Ба§Ж ১а•Л а§∞ৌ১а•На§∞а§њ а§Ьа•Нৃৌ৶ৌ а§≠а§Ња§Иа•§ ৶ড়৮ ৴а•На§∞а§Ѓ ৐৮ৌ а§Фа§∞ а§∞ৌ১а•На§∞а§њ ৵ড়৴а•На§∞а§Ѓа•§ а§Ъа§В৶а•На§∞а§Ѓа§Њ ৮а•З ৕৙а§Ха•А ৶а•Аа•§ ৵ড়৴а•На§∞а§Ѓ а§Ха•Л а§Ѓа§Іа•Ба§Ѓа§ѓ а§ђа§®а§Ња§ѓа§Ња•§ а§∞ৌ১а•На§∞а§њ а§Ха•Л а§Ѓа§Іа•Ба§∞ ৙а•На§∞а§Хৌ৴ুৃ а§ђа§®а§Ња§ѓа§Ња•§ а§Ча•Ба§∞а•В а§≠а•А а§ѓа§єа•А а§Ха§∞১ৌ а§єа•Иа•§ ৵৺а•А а§ђа•На§∞а§єа•На§Ѓа§Њ а§єа•И, а§Єа•Га§Ь৮а§Ха§∞а•Н১а•Н১ৌ а§єа•Иа•§ ৵৺ ৙ৌа§≤а§Х ৵ড়ৣа•На§£а•Б а§Ха•А а§≠а•Ва§Ѓа§ња§Ха§Њ а§Ѓа•За§В а§єа•Л১ৌ а§єа•Иа•§ а§Єа§Ва§∞а§Ха•На§Ја§£ ৶а•З১ৌ а§єа•И, ৙а•Ла§Ја§£ а§≠а•А ৶а•З১ৌ а§єа•Иа•§ ৵৺ а§Ѓа§єа•З৴ а§єа•Л১ৌ а§єа•И, а§єа§Ѓа§Ња§∞а•З а§Еа§єа§Ва§Ха§Ња§∞ а§Ха•Л ৮ৣа•На§Я а§Ха§∞১ৌ а§єа•Иа•§ а§Еа§єа§Ва§Ха§Ња§∞ а§єа•А а§єа§Ѓа§Ња§∞а•З а§єа•Л৮а•З а§Ха§Њ ুড়৕а•На§ѓа§Ња§≠а§Ња§Є а§єа•Иа•§ ৙а•Ва§∞а•Н৵а§Ьа•Ла§В ৮а•З а§Ча•Ба§∞а•В а§Ха•Л ৆а•Аа§Х а§єа•А а§ђа•На§∞а§єа•На§Ѓ, ৵ড়ৣа•На§£а•Б а§Фа§∞ а§Ѓа§єа•З৴ а§Ха§єа§Њ а§єа•И, а§≤а•За§Хড়৮ а§Е৮а•Ба§≠а•В১ড় а§Єа•З ৐৮а•А ৴а•На§∞৶а•На§Іа§Њ а§З১৮а•З ৙а§∞ а§єа•А ৮৺а•Аа§В а§∞а•Ва§Ха•Аа•§ а§Жа§Ча•З а§Йа§Єа•З а§Єа§Ња§Ха•Нৣৌ১ '৙а§∞ а§ђа•На§∞а§єа•На§Ѓ' а§≠а•А а§Ха§єа§Ња•§ ৙а§∞а§ђа•На§∞а§єа•На§Ѓ а§ђа•На§∞а§єа•На§Ѓ а§Ха•З ৙ৌа§∞ а§Ха•А ৪১а•Н১ৌ а§єа•Иа•§ а§Ѓа•За§≤а•З а§Ѓа•За§В а§Ца•Л а§Ча§П а§Еа§ђа•Ла§І а§ђа§Ъа•На§Ъа•Ла§В а§Ха•Л а§Ьа•Иа§Єа•З а§Йа§Ва§Ча§≤а•А ৙а§Ха§°а§Ља§Ха§∞ а§Ха•Ла§И а§Єа§Ьа•На§Ь৮ а§Ша§∞ ৙৺а•Ба§Ва§Ъа§Њ ৶а•З১ৌ а§єа•И, ৵а•Иа§Єа•З а§єа•А а§Ча•Ба§∞а•В а§≠а•А а§Ѓа•Ва§≤ а§Ча§В১৵а•На§ѓ ১а§Х а§≤а•З а§Ьৌ১ৌ а§єа•Иа•§ а§Ча•Ба§∞а•В ৙а•На§∞а§Ња§£ а§Єа•З а§Ьа•Бৰ৊১ৌ а§єа•И, ৙а•На§∞а§Ња§£а§Ѓа§ѓ а§Ѓа§Ьа§ђа•В১ а§Ха§∞১ৌ а§єа•Иа•§ а§єа§Ѓа•За§В ৵ড়а§Ьа•На§Юৌ৮ а§Єа•З а§Ьа•Ла§°а§Ља§Ха§∞ ৵ড়а§Ьа•На§Юৌ৮ুৃ ৐৮ৌ১ৌ а§єа•Иа•§ ৵৺ ৙а•На§∞а§Ьа•На§Юৌ৮ а§єа•И, ৙а•На§∞а§Ьа•На§Юৌ৮а•А ৐৮১ৌ а§єа•Иа•§ ৵৺ а§Ж৮а§В৶ а§єа•И, а§Йа§Єа§Ха§Њ а§Єа§Ва§Єа•Н৙а§∞а•Н৴ а§Ж৮а§В৶а•А ৐৮ৌ১ৌ а§єа•Иа•§
а§Ча•Ба§∞а•В ১а•Аа§∞а•Н৕ а§єа•Иа•§ а§Йа§Єа§Ха§Њ а§Єа§Ва§Ч, ৪ৌ৕ а§Фа§∞ а§Єа§Ва§Єа•Н৙а§∞а•Н৴ а§Й৙৮ড়ৣ৶а•Н а§Ха§єа§≤ৌ১ৌ а§єа•Иа•§ а§Ча•Ба§∞а•В а§Ьа•Иа§Єа§Њ а§єа•А ৙а•На§ѓа§Ња§∞а§Њ ৴৐а•Н৶ а§єа•И-а§Йа§™а§®а§ња§Ја§¶а•§ а§Й৙ а§Ха§Њ а§Еа§∞а•Н৕ а§єа•И ৮ড়а§Ха§Яа•§ ৮ড় а§Ха§Њ а§Еа§∞а•Н৕ ৆а•Аа§Х а§Єа•З а§Фа§∞ ৣ৶а•Н а§Ха§Њ а§Еа§∞а•Н৕ а§єа•Л৮ৌ, а§ђа•Иа§†а§®а§Ња•§ а§Ха§Ѓа§Ња§≤ а§Ха•А ৐ৌ১ а§єа•И а§Ха§њ ৵ড়৴а•Н৵ а§Ха§Њ а§Єа§ђа§Єа•З а§ђа§°а§Ља§Њ а§Ьа•На§Юৌ৮ ৮ড়а§Ха§Я а§ђа•И৆৮а•З а§Ха•А а§Єа§Ња§Іа§Ња§∞а§£ а§Ч১ড়৵ড়৲ড় а§Ѓа•За§В а§Йа§Ча§Ња•§ а§Ьа•Иа§Єа•З а§∞а•Ла§Ч а§Єа§Ва§Ха•На§∞а§Ња§Ѓа§Х а§єа•Л১а•З а§єа•Иа§В, ৵а•Иа§Єа•З а§єа•А а§Ьа•На§Юৌ৮ а§≠а•Аа•§ а§∞а•Ла§Ча•А а§Ха§Њ ৪ৌ৕ а§∞а•Ла§Ч ৶а•З১ৌ а§єа•И, а§≠а•Ла§Ча•А а§Ха§Њ а§Єа§Ва§Ч а§≠а•Ла§Ч ৶а•З১ৌ а§єа•И, а§ѓа•Ла§Ча•А а§Ха•А ৙а•На§∞а•А১ড় а§ѓа•Ла§Ч ৶а•З১а•А а§єа•И а§Фа§∞ а§Ча•Ба§∞а•В а§Ха§Њ ৪ৌ৕ а§Й৙৮ড়ৣ৶а•Н ৐৮১ৌ а§єа•И, а§Й৙৮ড়ৣ৶а•Н а§єа•Л১ৌ а§єа•Иа•§ а§Й৙৮ড়ৣ৶а•Н а§Ча•Ба§∞а•В а§Фа§∞ ৴ড়ৣа•На§ѓ а§Ха•З а§Ѓа§Іа•На§ѓ а§Ша§Яড়১ а§Єа§В৵ৌ৶ а§єа•А а§єа•Иа§Ва•§ а§Ча•Ба§∞а•В а§ђа•Ла§≤а•З, ৴ড়ৣа•На§ѓ ৮а•З а§Єа•Ба§®а§Ња•§ ৴ড়ৣа•На§ѓ а§Ха•З а§Еа§В১:а§Ха§∞а§£ а§Ѓа•За§В ৙а•На§∞৴а•Н৮, ৙а•На§∞১ড়৙а•На§∞৴а•Н৮ а§Йа§Ча•За•§ а§Ча•Ба§∞а•В ৮а•З а§Е৮а•Ба§≠а•В১ড় а§Єа•З а§Й১а•Н১а§∞ ৶ড়а§П, а§≤а•За§Хড়৮ а§Х৕৮-৴а•На§∞а•Б১ড় а§Ха•А а§За§Є а§Ха§Ња§∞а•Нৃ৵ৌ৺а•А а§Ѓа•За§В ৐ড়৮ৌ а§ђа•Ла§≤а•З а§єа•А ১ুৌু ৙а•На§∞৴а•Н৮ а§Йа§Ча•З, ৐ড়৮ৌ а§ђа•Ла§≤а•З а§єа•А ১ুৌু а§Й১а•Н১а§∞ а§≠а•А а§Жа§Па•§ ৶а•Л৮а•Ла§В ৮а•З ৴৙৕ а§≤а•А ৕а•А, а§Л১а§В ৵৶ড়ৣа•На§ѓа§Ња§Ѓа§њ, ৪১а•На§ѓа§В ৵৶ড়ৣа•На§ѓа§Ња§Ѓа§њ,'' а§Ха•Аа•§ а§Л১ а§єа•А а§ђа•Ла§≤а•Ва§Ва§Ча§Њ, ৪১а•На§ѓ а§єа•А а§Ха§єа•Ва§Ва§Ча§Ња•§ а§Жа§Ъа§Ња§∞а•На§ѓ а§Єа•Н৵а§∞ ৕ৌ, ৴ড়ৣа•На§ѓ а§ђа§Ња§Ва§Єа•Ба§∞а•А а§•а§Ња•§ а§Й৙৮ড়ৣ৶а•Н а§Ча•А১ а§єа•Иа§В а§За§Єа•А а§ђа§Ња§Ва§Єа•Ба§∞а•А а§Ха•За•§ а§Ьৌ৮ ৙ৰ৊১ৌ а§єа•И а§Ха§њ а§Л১ а§Фа§∞ ৪১а•На§ѓ а§єа•А ৵а§Ха•Н১ৌ ৴а•На§∞а•Л১ৌ ৕а•За•§ а§Ча•Ба§∞а•В а§Л১ ৕ৌ, ৴ড়ৣа•На§ѓ ৪১а•На§ѓ ৐৮ৌ, а§Ьа•Л а§Л১ ৕ৌ, ৵৺а•А ৪১а•На§ѓ а§•а§Ња•§ ৶а•Л৮а•Ла§В а§Па§Х ৕а•З, ৶а•Л ৕а•З а§єа•А ৮৺а•Аа§Ва•§ ৙а•Ва§∞а•На§£а§ња§Ѓа§Њ а§Ѓа•За§В а§Єа•Ва§∞а•На§ѓ а§Ха§Њ а§єа•А ১а•За§Ь а§єа•Иа•§ а§Ъа§В৶а•На§∞а§Ѓа§Њ ু৮ ১а•Л а§Єа•Ва§∞а•На§ѓ а§Ж১а•На§Ѓа§Ња•§ а§Ча•Ба§∞а•В а§Фа§∞ ৙а•Ва§∞а•На§£а§ња§Ѓа§Њ а§Ха•З а§Е৶а•Н৵ৃ ৙а•На§∞১а•Аа§Х а§Ха•Л а§ђа§Ња§∞а§Ва§ђа§Ња§∞ ৮ু৪а•На§Ха§Ња§∞ а§єа•Иа•§

 а§Ѓа§Іа•На§ѓ ৙а•На§∞৶а•З৴
а§Ѓа§Іа•На§ѓ ৙а•На§∞৶а•З৴ 





















