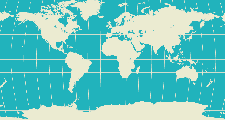सच्चाई और पीड़ा को सीने से लगाता नंदी
 उपन्यास 'छपाक-छपाक' की समीक्षा
उपन्यास 'छपाक-छपाक' की समीक्षा

माणिक

होशंगाबाद के अशोक जमनानी के तीन उपन्यास भी पाठकों के बीच बहुत लोकप्रिय हुए हैं। अपनी सबसे प्रखर कृति व्यास गादी में उन्होंने आज कल के बाबा-तुंबाओं की आश्रम बनाओ प्रतियोगिता के सच को अपनी गूंथी हुई शैली में पूरी बेबाकी से लिखा। मध्य प्रदेश साहित्य अकादेमी के दुष्यंत कुमार सम्मान से पिछले साल ही नवाजे गए जमनानी के अन्य उपन्यासों में बूढ़ी डायरी और को अहम् भी खासे चर्चित रहे। इस बार भाषा के स्तर पर नए प्रयोग का असर देने वाला उपन्यास छपाक-छपाक पाठक के हाथों में आ गया है। पांच भागों में बंटा हुआ नया उपन्यास एक सौ साठ पेज का है, जिसे एक बार फिर दिल्ली के तेज प्रकाशन ने छापा है। मैंने एक ही बैठक में साठ पेज पढ़ते हुए उसे सहजता से पार किया। एक भाग पढ़ा। इसी बीच पांच बार रोया। अशोक भाई को अपनी टिप्पणी देते हुए भी रो पड़ा। उनसे हुई बातों में पता लगा कि अशोक खुद भी लिखते वक्त इस कहानी में घंटों रोए हैं। समाज के जीवंत चित्रण को शब्दों में ढालता ये उपन्यास बहुत शुरुआत में तो इमोशनल किस्म का जान पड़ता है, मगर अंत तक जाते-जाते बहुत हद तक पिछड़े परिवारों की मानसिकता और मुसीबतों की परतें पाठक के सामने खोलता जाता है। इसके केंद्रीय भाव में समाज के मुख्य हिस्से कहे जाने वाले मगर गुरूजीब्रांड लोगों के बैनर तले शिष्यों से ली जाने वाली बेगार प्रथा भी जमी हुई नजर आई।
भारतीय लोकतंत्र में साक्षरता के आंकड़े भले ही ऊंचे उठ गए हों मगर आज भी इस किताब के संवाद पढ़ते हुए ऐसा आभास होता है कि ऐसी कई परंपराएं मौजूद हैं जो पाठक के पैरों के नीचे की जमीन ढहाती लगती हैं। रचना का मुख्य पात्र नंदी बहुत प्रभावपूर्ण ढंग से पाठक के मानस पटल पर अपनी तस्वीर बनाता है। शुरुआत से लेकर अंत तक भले आदमी के माफिक अपने दायित्व के इर्दगिर्द चलता है। न बहुत दूर, न ही बहुत सटा हुआ। सामाजिक और धार्मिक जीवन में ऊंचे स्थान पर मानी जाने वाली नर्मदा नदी के साथ ही वहां के आलम को इस उपन्यास में पर्याप्त रूप से मान मिला है। हर थोड़ी देर में नदी के बहाव को देखता हुआ लेखक अपने पात्रों के बहाने असल जीवन दर्शन को कागज में छापता है। शाम-सवेरे और सूरज जैसी उपमाओं के जरिए भी बहुत गहरी बातें संवादों में रूक-रूक कर समाहित की गई हैं। संवादों में बहुत से ऐसे शब्दों का समावेश मिलेगा जो उस इलाके के देशज लगते हैं। समय के साथ अपने में बदलाव करता नंदी उम्र के साथ जिम्मेदारियां ओढ़ता जाता है, मगर आसपास की समस्याएं उसे हमेशा सालती रहती हैं। गलत संगत के चलते बिगड़ते स्कूली बच्चों पर केंद्रित ये उपन्यास बस्ती जैसे हल्कों की सच बयानी करता है। कथ्य भी मध्य प्रदेश में बहती नर्मदा मैय्या के किनारे वाले प्रवाह-सा रूप धरता है। पढ़ते हुए कभी मुझे ये उपन्यास पाठक को सपाट गति से समझ में आने वाली फिल्म के माफिक भी लगता है।
ये छपाक-छपाक वो आवाजें हैं जिनमें नंदी ने अपने पिता भोरम, अपनी माँ सोन बाई को खो दिया। ये ही वो छपाक की धम्म है जिसके चलते नंदी को स्कूल छोड़ना पड़ा। ये ही वो आवाज़ है जहां अपने कुसंस्कारों की औलादें बीयरपार्टी सनी पिकनिक मनाती है और बहते पानी में अपने मित्र खो देते लोगों की कहानी बनाती है। ऊंची जात के युवक जब बहते हुए मरने वाले होते हैं तो नीची जात के कुशल तैराक उन्हें बचा लेते हैं। मगर खून तब खौलता है जब उपन्यास में वो ऊंची जात के मरते-मरते बचे बेटे वीरेंद्र की माँ तैरने में उस्ताद नंदी की जात पूछकर खीर खिलाने का बरतन डिसाइड करती है। दकियानूसी परिवारों में फंसी सादे घरों की बेटियों की पीड़ा झलकाता देवांगी का चरित्र भी बहुत कम समय उपस्थित रह कर भी प्रमुखता से उभरा है। उपन्यास के बहुत बड़े हिस्से को घेरे बैठे दो नबर के धंधेबाज भैयाजी और उनके बेटे वीरेंद्र जैसे घाघ किस्म के लोग भी इस दुनिया में बहुतेरे भरे पड़े हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज भी नंदी जैसे आदिवासी उनके बड़े दरवाजों वाले मकानों के भाव में डूब कर उनके पैर दबा रहे हैं। उपन्यास के अंत में खुद के अंत के साथ ही बाज आने वाला तंतर-मंतर का पोटला वो पड़िहार भी घाघ ही था। इस रचना में जहां पापी लोग भरे हैं वहीं ठीक दिल के पत्र भी इसका हिस्सा रहे हैं।
मानवीय मूल्यों की बात करें तो सभी बातों और विचारों के बीच सोन बाई, बघनखा और भोरम के मरने पर नंदी के मन का दुरूख समझने वाले पंचा काका और बचपने की मित्र महुआ जैसे लोग कम ही सही मगर आज भी हमारे इस परिदृश्य में बचे हैं। माँ नहीं होकर भी सुखो काकी ने नंदी पर अपना वात्सल्य उड़ेल दिया। ये भाव अब भी देहात में सरस सुलभ हैं। वीरेंद्र ने नंदी को पुलिस से बचाने के हित अपने पिता तक से दुश्मनी कर ली। नंदी को जेल से छुडाने में गिरवी रखे खेतों पर सेठजी की खराब नज़र भी अंत तक जाते-जाते भली बन पड़ी। इन उदाहरणों को पढ़ कर लगता है कि मानव-मूल्यों की याद आदमी को धीरे से ही आए मगर अंततोगत्वा उन्ही की शरण से मुक्ति संभव लगती है। वैसे भी आजकल अच्छे दिल के लोगों को भगवान जल्दी ही ऊपर बुला ले रहा है, वहीं बाकी की कसर तेजी से बदलते जमाने की इस रफ्तार में मानव मूल्यों की चटनी बनाकर पूरी कर दी है। यहां इस रचना में भी कई भले लोग जल्दी ही मर गए।
कुछ दह तक व्यवसाई अशोक,स्पिक मैके नामक सांस्कृतिक आंदोलन से भी जुड़े होने से अपने बहुत से गुणों के साथ उपन्यास में धुंधले से ही सही मगर दिखते हैं। बाकी सारे हिस्से में उनका रचना कौशल साफ झलकता है। उपन्यास में उनके कला और धर्मप्रेम की झलक बखूबी दिखती है। अशोक, निचले तबके के लोगों के कठोर श्रमप्रधान जीवन से भली-भांति परिचित है। थोड़े-थोड़े दिनों में नर्मदा नदी के किनारे अकेले में की गई उनकी लंबी यात्राएं भी इस रचना से झांकती नजर आई हैं। एक नदी के प्रति माँ-सा भाव उनकी अपनी मिट्टी के प्रति उनके समर्पण भाव और स्वयं को उन्हीं प्राकृतिक और विरासती पहचानों के हित भुला देने की उनकी प्रवृति को मैं सलाम करता हूं। उनकी पिछली रचनाओं की अपेक्षा ये उपन्यास आम पाठकों तक पहुंच बनाने में ज्यादा अच्छे से सफल हो पाएगा, ऐसा मेरा मानना है।
उपन्यास में आए पात्रों के नाम भी पूरे रूप में आदिवासी पहचान लिए हुए हैं। गोया गुलमा, सुखो, भोरम, बघनखा, पड़िहार, सोन बाई, सरना। नदी, जंगल, बस्ती के इर्दगिर्द जंगली पेड़ों के नाम और देश-दुनिया की गतिशील यात्रा से वहां का अछूता जीवन आज भी शहरों की आधुनिकता के आगे थूंकता है। आज भी ऐसे गांव हैं जहां अपनी रोजी के रूप में लोग नदी में धर्म के नाम पर डाले गए सिक्के खंगालते हैं। आज भी अपने किसी काम के बाकी रहते लोग मर जाने पर मुक्ति के लिए भटकते रहते हैं। इसके उलट समाज की बहुत सी बीमारियां आज भी दबे कुचले गांवों में जड़ें पकड़ी हुई हैं। ये एक रूप है तो दूजा नंदी के प्यार में उसकी हर पीड़ा को समझने वाली महुआ, नायिका के रूप में अपने थोड़े मगर सुगठित संवादों के साथ उभरी है। उपन्यास में एक के बाद एक बहुत सी कथाएं खुलती जाती हैं। इस तरह बहुत से रसों और भावों का समिश्रण यहां मिलेगा। मिले-जुले जीवन को लिखते इस उपन्यास में परेशानियों के हालात में नंदी को गांवों में मिलने वाली सहज स्नेह दृष्टी के साथ कई सारे कड़ुए घुट भी पीने पड़े, फिर भी ऐसा क्या था कि वो अडिग रहा पथ पर। रचना पढ़ने पर ही अनुभव किया जा सकता है।
समग्र रूप से छपाक-छपाक जैसा उपन्यास एक बार फिर पाठकों को सोचने के हित कई सारे मुद्दे छोड़े जा रहा है। यही नहीं आज फिर से हमारी आर्थिक और वैचारिक गुलामी का द्योतक भी साबित हुआ है। ये रचना पढ़ने के बाद एक बार फिर लगा कि पुलिस तंत्र सहित सेठ-साहूकारों, वकीलों, डॉक्टरों और गुरुजनों तक के सहयोग से भ्रटाचार की दीमक खुलेआम फैल ही चुकी है। आज भी देहाती इलाकों में हॉस्पिटल जैसी चिड़िया का मिलना मुश्किल है और मजबूरन आदमी जादू-टोने के भरोसे ही सांस लेते हैं। एक बार फिर सच तो यही लगने लगा है कि झुग्गियों और बस्तियों की जिंदगी में, पास बहते नदी-नाले के पानी में, छप-छप करने और कूदने पर छपाक-छपाक आवाज़ें आने मात्र ही उनके मनोरंजन के साधन बनकर उन्हें खुशियां देते हैं और ये ही वो जगह है जहां वे अपना दुख साझा कर सकते हैं। वाकई ये उपन्यास बहुत दूर तक पढ़ा जाएगा। प्रकाशक-तेज़ प्रकाशन, दरियागंज नई दिल्ली। मूल्य दो सौ पचास रूपये।

 मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश