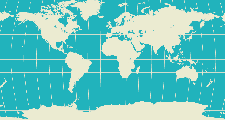बसपा का ब्राह्मण प्रेम कितना सफल, कितना फेल
डॉ रमेश सिंह बौद्ध
लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी के ब्राह्मण प्रेम से दलित और ब्राह्मण समाज में काफी उथल-पुथल है। दोनों ही तरफ से इस ‘प्रेम’ के नफे नुकसान पर चर्चा हो रही है। बसपा का ब्राह्मण फार्मूला और आगे राजनीति में कैसा परिणाम देगा यह तो समय ही बताएगा मगर इतिहास जो बोल रहा है वो यह है कि जब भी दलितों ने ब्राह्मणों से समझौता करने की कोशिश की तो दलितों के हाथ कुछ नहीं लगा। ब्राह्मणों ने तो पूरा लाभ उठाया पर दलित आंदोलन कमजोर ही हुआ। एक समय बाद उसके नेता भी गुमनामी में चले गये। दलितों के कंधे पर बैठकर दूसरे राजनीतिक दलों ने लंबे समय तक राजपाट जरूर चलाया। यही कारण रहा कि देश में दलित आंदोलन, ब्राह्मण की भूमिका शुरू होते ही अपने मुकाम से पहले ही रूक गया। दलित राजनीति में दूसरी जातियों की भूमिका का आंकलन करने वालों के अपने अपने मत हैं।
पिछली सदी के आखिर में इसका ज्वलंत उदाहरण बिहार के कांग्रेसी नेता बाबू जगजीवन राम का है, जो ब्राह्मणों पर भरोसा कर उन्हीं के कारण एक बार ब्राह्मणों के वर्चस्व वाली कांग्रेस से अलग होने को मजबूर हुए। वे शिखर पर पहुंचने के लिए जीवन भर ब्राह्मणों के पीछे लगे रहे। जब वह देश के सर्वोच्च पद के दोवदारों की कतार में पहुंचे तो उन्हें केवल देश के उप प्रधानमंत्री के पद पर ही संतोष करना पड़ा। बदले में उस समय के राजनीतिक दलों ने उनके व्यक्तित्व और प्रभाव का जो फायदा उठाया वह जग जाहिर है। एक लंबे समय तक कांग्रेस ने उन्हें अपने साथ रखकर दलितों का भरपूर समर्थन लिया।
इतिहास है कि देश में सबसे बड़ा दलित जागृति आंदोलन डा भीमराव अंबेडकर ने चलाया था, जो उस समय भी वह ब्राह्मणवादी व्यवस्था के प्रभाव में रहा। अम्बेडकर उस समय दलितों के लिए उन्हीं अधिकारों की बात कर रहे थे, जिनकी आज बात हो रही है। मगर उस समय पंडित जवाहर लाल नेहरू और महात्मा गांधी के सामने उनकी नहीं चल सकी। वे इसलिए उतने कामयाब नहीं हो पाये। सत्ता और राजनीति का दबाव पूरी तरह ब्राह्मणवादी व्यवस्था से नियंत्रित हो रहा था और दलित उस समय उसी व्यवस्था के प्रभाव में था इस कारण अम्बेडकर को अपना दलित आंदोलन चलाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह एक ऐसा काल था, जब अम्बेडकर अछूत व्यवस्था के खिलाफ काफी उत्तेजित और आन्दोलित थे, जिससे वह दलित क्रांति के सफल नायक नहीं कहलाये जा सके। अगर ब्राह्मण उसी समय सही मायने में अम्बेडकर की नीतियों का समर्थन करता तो देश में उसी समय दलित क्रांति आ गयी होती। ऐसे कई प्रस्तावों को जिनको ब्राह्मणों के समर्थन की जरूरत थी और समर्थन नहीं मिला।
इसीलिए आज उत्तर प्रदेश का दलित पूछ रहा है कि जब ब्राह्मणों को साथ रखकर डॉ. भीमराव अम्बेडकर को नुकसान हुआ तो मायावती के ब्राह्मणों को साथ लेकर चलने के प्रयोग की सफलता की क्या गारंटी है? बसपा को जो सफलता ब्राह्मणवाद व ब्राह्मणों के खिलाफ आन्दोलन चलाकर मिली वह सफलता ब्राह्मणों को साथ लेकर कैसे मिल सकती है। दलित यह भी पूछते हैं कि क्या आज ब्राह्मण हमारे साथ बैठकर हमारे संस्कारों का समर्थन करने को तैयार हैं? पांच हजार वर्षों के भगवान बुद्ध के मनुवाद के खिलाफ चले आन्दोलन के बावजूद भी ब्राह्मण की दलितों को इस्तेमाल करने की नीति नहीं खत्म हुई, ब्राह्मण अपनी राय नहीं बदल सके तो बसपा से जुड़कर या जोड़कर क्या वे बदल जायेंगे? क्या बसपा का यह दृष्टिकोण उसी को ही नुकसान नहीं पहुंचा सकता है? क्योंकि जब 1967 में उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी तो इसमें आरपीआई ने जिसका चुनाव चिन्ह ऊंट था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ खड़े होकर पचास सीटें जीतीं और ब्राह्मणवादी कांग्रेस को हराया। इसके बाद इंदिरा गांधी ने जब आरपीआई के अध्यक्ष बीपी मौर्य को कांग्रेस में शामिल कर लिया तो उसके बाद बीपी मौर्या का दलित आन्दोलन जाता रहा। यह इसलिए हुआ क्योंकि बुद्ध प्रिय मौर्य के तेवर कांग्रेस में जाने के बाद ब्राह्मणों के प्रति नरम पड़ गये और धीरे-धीरे बीपी मौर्या राजनीति के परिदृश्य से ही गायब हो गये। ऐसा ही हाल अम्बेडकर का कांग्रेसवादी ब्राह्मणों के सम्पर्क में आने से हुआ।
दलितों की धारणा है कि ब्राह्मणों से समझौता करने की जब-जब दलितों की कोशिशें हुई तभी दलित आन्दोलन कमजोर हुआ। अब दलितों में आशंका बढ़ रही है कि हो सकता है कि अब तक जो दलितों में जोश है वह कहीं कम न हो जाए क्योंकि वे, अब तक जिनके खिलाफ सड़क पर उतरकर संगठित हुए थे वे अब किस मन से उनके साथ खड़े होंगे। क्योंकि ब्राह्मण तो कहता है कि पांच हजार सालों की व्यवस्था को नहीं बदला जा सकता। इसके बावजूद बसपा का यह कहना कि वह अपने नए फार्मूले इसे बदलने के लिए ब्राह्मणों के साथ है। उसके एजेंडे में यह सबसे ऊपर है। कैसे बर्दाश्त करेगा। कई जगह ऐसी हैं जहां बसपा को अपनों की उपेक्षा कर ब्राह्मण लाना होगा उस स्थिति में दलितों की क्या हालत होगी यह इतिहास देखकर बयान की जा सकती है। बसपा संस्थापक कांशीराम का आन्दोलन काफी हद तक सफल रहा क्योंकि वह ब्राह्मणवाद के खिलाफ ही था। अब जो मायावती कर रही हैं, उसके तात्कालिक लाभ को छोड़कर राजनीतिक खतरे भी वैसे ही हैं।

 मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश