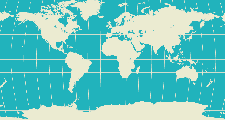
а§Па§Х а§Ца•Ла§И-৙ৌа§И а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓ

а§Уа§Ѓ ৕ৌ৮৵а•А

а§Ха•Ла§И а§∞৴а•На§Х а§Ха§∞а•З ৮ а§Ха§∞а•З, а§Ѓа•Ба§Эа•З а§За§Є ৐ৌ১ а§Ха§Њ а§Ђа§Ца•На§∞ а§єа•Л১ৌ а§єа•И а§Ха§њ а§Ѓа•Иа§В৮а•З ৪১а•На§ѓа§Ьড়১ а§∞а§Ња§ѓ а§Ха•Л ৶а•За§Ца§Њ а§•а§Ња•§ ৵৺ а§≠а•А а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓ ৐৮ৌ১а•З а§єа•Ба§Па•§ ১৐ а§ђа•Аа§Хৌ৮а•За§∞ а§Ха•З а§Єа§ња§Яа•А а§Єа•На§Ха•Ва§≤ а§Ѓа•За§В ৙а•Э১ৌ а§•а§Ња•§ а§Ж৆৵а•Аа§В а§ѓа§Њ ৮а•М৵а•Аа§В а§Ѓа•За§Ва•§ ৙а•И৶а§≤ а§Ха§Њ а§∞а§Ња§Єа•Н১ৌ а§•а§Ња•§ а§ђа•Аа§Ъ а§∞а§Ња§Єа•Н১а•З а§∞ড়ৃৌ৪১ а§Ха•З ৶а•Ма§∞ а§Ха§Њ а§Єа§∞а•Л৵а§∞ а§Єа•Ва§∞а§Єа§Ња§Ча§∞ ৙а•Ь১ৌ ৕ৌ, а§Ьа§ња§Єа§Ѓа•За§В а§Еа§ђ ৴৺а§∞ а§Ха§Њ а§Ча§В৶ৌ ৙ৌ৮а•А а§≠а§∞а§Њ а§Ьৌ৮а•З а§≤а§Ча§Њ а§•а§Ња•§ ৪ৌু৮а•З а§≠৵а•На§ѓ а§Ьа•В৮ৌа§Ча•Э а§•а§Ња•§ а§Жа§Ча•З ৙৐а•На§≤а§ња§Х ৙ৌа§∞а•На§Ха•§
১а•Л ১а•Ьа§Ха•З а§Єа•На§Ха•Ва§≤ а§Ьৌ১а•З ৵а§Ха•Н১ а§Єа•Ва§∞а§Єа§Ња§Ча§∞ а§Ха•А а§Ѓа•Ба§Ва§°а•За§∞ ৙а§∞ а§Ѓа•Иа§В а§Єа§єа§Єа§Њ ৆ড়৆а§Ха§Ња•§ а§∞а•За§≤а§Ча§Ња•Ьа•А а§Ьа•Иа§Єа•А а§Ыа•Ла§Яа•А ৙а§Яа§∞а•А ৙а§∞ а§∞а§Ца•А а§Па§Х а§Яа•На§∞а§Ња§≤а•А ৙а§∞ а§Ха•Иа§Ѓа§∞а•З а§Ха•З ৪ৌ৕ ৪১а•На§ѓа§Ьড়১ а§∞а§Ња§ѓ а§ђа•И৆а•З ৕а•За•§ а§Ша§∞ а§Ѓа•За§В а§Ж৮а•З ৵ৌа§≤а•З а§Еа§Ца§ђа§Ња§∞а•Ла§В а§Ѓа•За§В а§Й৮а§Ха•А ১৪а•Н৵а•Аа§∞ ৶а•За§Ца•А а§єа•Ла§Ча•Аа•§ ৙৺а§Ъৌ৮৮а•З а§Ѓа•За§В а§Ха•Ла§И а§≠а•Ва§≤ ৮৺а•Аа§В а§Ха•А а§Фа§∞ а§Єа•На§Ха•Ва§≤ а§Ха§Њ а§∞а§Ња§Єа•Н১ৌ а§Ыа•Ла•Ь вАШа§Єа•Л৮ৌа§∞ а§Ха•За§≤а•На§≤а§ЊвАЩ (а§Єа•Л৮а•З а§Ха§Њ а§Ха§ња§≤а§Њ) а§Ха•А ৴а•Ва§Яа§ња§Ва§Ч ৶а•За§Ц৮а•З а§≤а§Ча§Ња•§ ৵а•З а§Єа§≠а•А ৶а•Г৴а•На§ѓ а§∞а§Ња§ѓ ৮а•З а§Єа•Н৵ৃа§В а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓа§Ња§Па•§ ৶ড়৮ ৮ড়а§Ха§≤ а§Жа§ѓа§Њ а§Фа§∞ а§∞а§Ња§єа§Ча•Аа§∞ а§Ьа§Ѓа§Њ а§єа•Л৮а•З а§≤а§Ча•З, ৙а§∞ ১৐ ১а§Х а§∞а§Ња§ѓ а§Е৙৮ৌ а§Ха§Ња§Ѓ ৙а•Ва§∞а§Њ а§Ха§∞ а§Ъа•Ба§Ха•З ৕а•За•§
а§Ѓа•Иа§В а§Еа§ђ а§Єа•На§Ха•Ва§≤ ৮৺а•Аа§В а§Ьа§Њ а§Єа§Х১ৌ а§•а§Ња•§ ৮ а§Ша§∞а•§ а§Єа•Л а§ђа§Ча•Аа§Ъа•З а§Ѓа•За§В а§Ъа§≤а§Њ а§Ча§ѓа§Ња•§ а§Єа•На§Ха•Ва§≤ а§Ха•А а§Ыа•Ба§Яа•На§Яа•А а§Ха•З ৵а§Ха•Н১ ১а§Х ৵৺а•Аа§В а§°а•Ла§≤১ৌ а§∞а§єа§Њ, ১ৌа§Ха§њ а§Ша§∞ а§≤а•Ма§Яа•Ва§В ১а•Л а§≤а§Ча•З а§Ха§њ а§Єа•На§Ха•Ва§≤ а§Єа•З а§Жа§ѓа§Њ а§єа•Ва§Ва•§
а§ђа•Аа§Хৌ৮а•За§∞ а§Ѓа•За§В а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓ ৵ৌа§≤а•Ла§В а§Ха•З а§≤৴а•На§Ха§∞ а§°а•За§∞а§Њ а§°а§Ња§≤а•З а§∞৺১а•З ৕а•За•§ ৴а•Ва§Яа§ња§Ва§Ч ৶а•За§Ц৮а•З а§єа§Ѓ а§≤а•Ла§Ч ৶а•Ва§∞а§ња§ѓа§Ња§В ৮ৌ৙ а§Ха§∞ а§≠а•А а§Ча§П, ৙а§∞ а§ѓа§є а§Еа§Ъৌ৮а§Х ৪ৌু৮а•З а§Жа§ѓа§Њ а§Ѓа•Ма§Ха§Њ ৮ড়а§∞а§Ња§≤а§Њ а§•а§Ња•§ ৮ а§≠а•Аа•Ь, ৮ ৴а•Ла§∞, ৮ а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓ ৵ৌа§≤а•Ла§В а§Ха•А а§∞а§Ва§Ча•А৮а•Аа•§ а§Ѓа•Ба§Яа•Н৆а•А а§≠а§∞ ৶৪а•Н১а•З а§Ха•З ৪ৌ৕ а§Е৙৮а•З а§Ха§Ња§Ѓ а§Ѓа•За§В ৶১а•Н১а§Ъড়১а•Н১ а§Па§Х а§Ж৶ুа§Ха§¶а•§ ৵৺ а§Е৮а•Ба§≠৵ а§Ѓа•За§∞а•З ৶ড়а§≤а•Л-৶ড়ুৌа§Ч ৙а§∞ а§Ыа§Њ а§Ча§ѓа§Ња•§ а§Еа§ђ а§≠а•А а§Йа§Є а§Ша•Ьа•А а§Ха•А ৃৌ৶ ১ৌа§Ьа§Њ а§єа•Иа•§
а§Ха§є ৮৺а•Аа§В а§Єа§Х১ৌ а§Ха§њ а§Йа§Є а§Ча•Иа§∞-а§Ѓа§Ња§Ѓа•Ва§≤а•А а§Єа•Ба§ђа§є а§Ха§Њ а§Ѓа•За§∞а•А ৪ড়৮а•За§Ѓа§Њ а§∞а•Ба§Ъа§њ а§Ха•З ৥а§≤৮а•З а§Ѓа•За§В а§Ха•Ла§И а§Ха§Ња§Ѓ а§∞а§єа§Ња•§ а§Па§Х ু৺ৌ৮ а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓа§Ха§Ња§∞ а§Ха•Л а§Ша•Ьа•А а§≠а§∞ а§Ха•З а§≤а§ња§П а§Фа§Ъа§Х ৶а•За§Ц৮а•З а§Ха§Њ а§≠а§≤а§Њ а§Ха•На§ѓа§Њ а§Еа§Єа§∞ а§єа•Л а§Єа§Х১ৌ а§єа•И? ১৐ ১а§Х а§Єа§єа•А ুৌৃ৮а•З а§Ѓа•За§В ৪১а•На§ѓа§Ьড়১ а§∞а§Ња§ѓ а§Ха•З а§ђа§Ња§∞а•З а§Ѓа•За§В а§Ха•Ба§Ы а§Ѓа§Ња§≤а•Ва§Ѓ а§≠а•А ৮ а§•а§Ња•§ ৮ а§ѓа§є а§Ха§њ вАШа§Єа•Л৮ৌа§∞ а§Ха•За§≤а•На§≤а§ЊвАЩ а§Ьа•Иа§Єа§≤а§Ѓа•За§∞ а§Ха•З а§Ха§ња§≤а•З а§Ха•Л а§∞а§Ња§ѓ а§Ха•А ৶а•А а§Й৙ুৌ а§єа•И а§Фа§∞ ৙৴а•На§Ъа§ња§Ѓ а§ђа§Ва§Ча§Ња§≤ а§Єа§∞а§Ха§Ња§∞ а§Ха•З а§Ца§∞а•На§Ъ ৙а§∞ ৐৮а•А ৵৺ а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓ а§∞а§Ња§Ьа§Єа•Н৕ৌ৮ а§Ха•Л ৶а•Б৮ড়ৃৌ а§Ха•З ৮а§Ха•Н৴а•З ৙а§∞ а§Ъа§Ѓа§Хৌ৮а•З ৵ৌа§≤а•А а§єа•Иа•§ а§Ца§Ња§Єа§Ха§∞ а§Ьа•Иа§Єа§≤а§Ѓа•За§∞ а§Ха•Ла•§ ১৐ а§ѓа§є а§≠а•А а§Ха§єа§Ња§В а§Ца§ѓа§Ња§≤ ৕ৌ а§Ха§њ а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓ ৐৮৮а•З а§Ха•З ৐ৌ৶ ৪১а•На§ѓа§Ьড়১ а§∞а§Ња§ѓ а§Ха•З а§Йа§Єа•А ৮ৌু ৵ৌа§≤а•З а§Й৙৮а•На§ѓа§Ња§Є а§Ха§Њ а§єа§ња§В৶а•А а§Е৮а•Б৵ৌ৶ а§єа§Ѓа§Ња§∞а•З а§Ша§∞ а§Ѓа•За§В а§єа•Ла§Ча§Њ!
৙а§∞, а§ѓа§є а§Єа§Ъа§Ња§И а§Е৙৮а•А а§Ьа§Ча§є а§єа•И а§Ха§њ а§ђа•Ьа•З а§єа•Л৮а•З ৙а§∞ а§Ча§Ва§≠а•Аа§∞ ৃৌ৮а•А а§Єа§Ња§∞а•Н৕а§Х ৪ড়৮а•За§Ѓа§Њ ৮а•З а§Е৙৮а•А а§Уа§∞ а§ђа•З১а§∞а§є а§Ца•Аа§Ва§Ъа§Ња•§ а§≠а§Ња§∞১а•Аа§ѓ а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓа§Ха§Ња§∞а•Ла§В а§Ѓа•За§В а§Л১а•Н৵ড়а§Х а§Ша§Яа§Х а§Фа§∞ ৪১а•На§ѓа§Ьড়১ а§∞а§Ња§ѓ а§Ха§Њ а§Ра§Єа§Њ а§Ѓа•Ба§∞а•А৶ а§єа•Ба§Ж а§Ха§њ а§Ша§Яа§Х а§Ха•А а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓ вАШ১ড়১ৌ৪ а§Па§Ха§Яа§њ ৮৶а•Аа§∞ ৮ৌুвАЩ (১ড়১ৌ৪ ৮ৌু а§Па§Х ৮৶а•А а§Ха§Њ) ৥ৌа§Ха§Њ а§Ьа§Ња§Ха§∞ ৥а•Ва§В৥а•А (а§Йа§Єа§Ха•З а§Еа§Іа§ња§Ха§Ња§∞ ৵৺а•Аа§В ৕а•З, а§Еа§ђ а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓ а§≠а§Ња§∞১ а§Ѓа•За§В а§Єа•Ба§≤а§≠) а§Фа§∞ а§∞а§Ња§ѓ а§Ха•А а§Ѓа•Ва§Х а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓ вАШа§Яа•ВвАЩ (৶а•Л) а§Ха§Њ а§Ша§ња§Єа§Њ-৙ড়а§Яа§Њ а§∞а•В৙ а§Ха§єа•Аа§В а§За§Ва§Яа§∞৮а•За§Я а§Єа•З ৥а•Ва§В৥а§Ха§∞ а§Й১ৌа§∞а§Ња•§ а§Іа•Аа§∞а•З-а§Іа•Аа§∞а•З ৶а•Л৮а•Ла§В а§Ха§Ња§≤а§Ьа§ѓа•А а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓа§Ха§Ња§∞а•Ла§В а§Ха•А а§≤а§Ча§≠а§Ч а§Єа§Ња§∞а•А а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓа•За§В а§Ьа§Ѓа§Њ а§єа•Л а§Ча§Иа§Ва•§ а§∞а§Ња§Ѓа§Ха§ња§Ва§Ха§∞ а§ђа•Иа§Ь ৙а§∞ а§Ша§Яа§Х а§Ха§Њ а§Па§Х а§Жа§Іа§Њ-а§Еа§Іа•Ва§∞а§Њ ৵а•Г১а•Н১а§Ъড়১а•На§∞, а§ђа§≤а•На§Ха§њ а§Йа§Єа§Ха§Њ а§Ха§Ъа•На§Ъа§Њ а§∞а•В৙-а§Ъড়১а•На§∞а§Ха§Ња§∞ а§Ь১а•А৮ ৶ৌ৪ а§Ха•З а§Єа•Ма§Ь৮а•На§ѓ а§Єа•З а§єа§Ња§Єа§ња§≤ а§єа•Ба§Жа•§
а§Ѓа§Ча§∞, ৪১а•На§ѓа§Ьড়১ а§∞а§Ња§ѓ а§Ха§Њ а§Па§Х ৵а•Г১а•Н১а§Ъড়১а•На§∞ а§Ѓа•Ба§Эа•З а§Ха§єа•Аа§В ৮৺а•Аа§В а§Ѓа§ња§≤а§Ња•§ ৶а•За§Ц৮а•З а§Ха•Л а§≠а•А ৮৺а•Аа§Ва•§ а§Єа•Б৮১а•З а§єа•Иа§В, ৵৺ а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓ а§Ца•Б৶ а§∞а§Ња§ѓ а§Ха•З ৙ৌ৪ ৮৺а•Аа§В а§∞а§єа•А ৕а•А, ৮ а§Ха§≠а•А а§Йа§Єа§Ха§Њ а§Єа§Ња§∞а•Н৵а§Ь৮ড়а§Х ৙а•На§∞৶а§∞а•Н৴৮ а§єа•Ба§Жа•§ а§Ъа§Ња§≤а•Аа§Є а§Єа§Ња§≤ ৙৺а§≤а•З а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓ ৐৮а•А а§Фа§∞ а§Ьа§≤а•Н৶а•А а§єа•А а§єа§Ѓа§Ња§∞а•А а§Єа§∞а§Ха§Ња§∞ ৮а•З а§Йа§Є ৙а§∞ ৙а•На§∞১ড়৐а§Ва§І а§≤а§Ча§Њ а§¶а§ња§ѓа§Ња•§ а§Ьড়৮а•На§єа•Ла§В৮а•З ৐৮৵ৌа§И ৵а•З а§≠а•А а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓ а§Єа•З а§ђа§єа•Б১ а§Єа§В১а•Ба§Ја•На§Я ৮ ৕а•З, ৐ৌ৶ а§Ѓа•За§В а§Ха§єа•Аа§В ৶ড়а§Цৌ১а•З, а§Йа§Єа§Єа•З ৙৺а§≤а•З а§Ца•Б৶ а§Ха§Ња§≤ а§Х৵а§≤ড়১ а§єа•Л а§Ча§Па•§
а§Еа§Ъৌ৮а§Х а§Йа§Є а§Ца•Ла§П а§Фа§∞ а§≤а§Ча§≠а§Ч а§≠а•Ба§≤а§Ња§П а§Ьа§Њ а§Ъа•Ба§Ха•З ৵а•Г১а•Н১а§Ъড়১а•На§∞ вАШа§Єа§ња§Ха•На§Ха§ња§ЃвАЩ а§Ха•З ৮а•За§Ча•За§Яড়৵ ১а•Л ৮৺а•Аа§В, ৶а•Л ৙а•На§∞а§ња§Ва§Я а§Ха•Ба§Ы ৵а§∞а•На§Ј ৙৺а§≤а•З ৮ুа•В৶ৌа§∞ а§єа•Ба§Па•§ а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓ а§Ха•З а§Еа§Іа§ња§Ха§Ња§∞ а§Ча§Ва§Ча§Яа•Ла§Х а§Єа•Н৕ড়১ а§Жа§∞а•На§Я а§Па§Ва§° а§Ха§≤а•На§Ъа§∞ а§Яа•На§∞а§Єа•На§Я а§Са§Ђ а§Єа§ња§Ха•На§Ха§ња§Ѓ а§Ха•З ৙ৌ৪ а§єа•Иа§Ва•§ а§Па§Х ৙а•На§∞а§ња§Ва§Я а§Ца§∞а§Ња§ђ ৮ড়а§Ха§≤а§Ња•§ ৶а•Ва§Єа§∞а§Њ а§ђа•З৺১а§∞ ৕ৌ, а§Ьа•Л а§≤а§В৶৮ а§Ха•А а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓ а§Па§Ха•За§°а§Ѓа•А а§Ха•З ৙ৌ৪ а§•а§Ња•§ а§Йа§Є ৙а•На§∞а§ња§Ва§Я а§Ха•Л а§Са§Єа•На§Ха§∞ а§П৵ৌа§∞а•На§° ৵ৌа§≤а•А а§Еа§Ѓа•За§∞а§ња§Ха•А а§Єа§Ва§Єа•Н৕ৌ (а§Па§Ха•За§°а§Ѓа•А а§Са§Ђ а§Ѓа•Л৴৮ ৙ড়а§Ха•На§Ъа§∞, а§Жа§∞а•На§Яа§Є а§Па§Ва§° а§Єа§Ња§За§Ва§Єа•За§Ь) ৮а•З а§≠а§Ња§∞а•А а§∞ৌ৴ড় а§Ца§∞а•На§Ъ а§Ха§∞ а§Єа•Ба§Іа§∞а§µа§Ња§ѓа§Ња•§ ৮ৌа§В১ (а§Ђа•На§∞а§Ња§Ва§Є) а§Фа§∞ а§≤а§В৶৮ а§Ха•З а§Єа§Ѓа§Ња§∞а•Ла§єа•Ла§В а§Ѓа•За§В а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓ ৶ড়а§Ца§Ња§И а§Ча§Иа•§ а§Еа§В১১: а§≠а§Ња§∞১ а§Єа§∞а§Ха§Ња§∞ а§Ха§Њ ৵ড়৵а•За§Х а§Ьа§Ња§Ча§Ња•§
а§Єа•Ва§Ъ৮ৌ а§Фа§∞ ৙а•На§∞а§Єа§Ња§∞а§£ а§Ѓа§В১а•На§∞а§Ња§≤а§ѓ а§Ха•А а§∞а§Ња§ѓ а§≤а•За§Ха§∞ ৵ড়৶а•З৴ а§Ѓа§В১а•На§∞а§Ња§≤а§ѓ ৮а•З ৶а•Л ৵а§∞а•На§Ј ৙৺а§≤а•З ৙а•На§∞১ড়৐а§Ва§І а§Й৆ৌ а§≤а§ња§ѓа§Ња•§ а§Ха•Ла§≤а§Хৌ১ৌ а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓ а§Єа§Ѓа§Ња§∞а•Ла§є а§Ѓа•За§В а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓ ৶ড়а§Ца§Ња§И а§Ча§Иа•§ ৪১а•На§ѓа§Ьড়১ а§∞а§Ња§ѓ а§Ха•З а§ђа•За§Яа•З а§Єа§В৶а•А৙ а§∞а§Ња§ѓ а§Ха•А а§Ха•Л৴ড়৴а•Ла§В а§Ха•З ৵৴а•Аа§≠а•В১ а§Ха•Ла§≤а§Хৌ১ৌ а§Ха•А а§Па§Х а§Ха§В৙৮а•А ৮а•З ৐ৌ৵৮ ুড়৮а§Я а§Ха•А ৵৺ а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓ а§єа§Ња§≤ а§Ѓа•За§В а§ђа§Ња§Ьа§Ња§∞ а§Ѓа•За§В а§Ьа§Ња§∞а•А а§Ха•А а§єа•Иа•§
а§ђа•Ьа•З а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓа§Ха§Ња§∞ а§Жু১а•Ма§∞ ৙а§∞ ৵а•Г১а•Н১а§Ъড়১а•На§∞ ৮৺а•Аа§В ৐৮ৌ১а•З, ৙а§∞ ৪১а•На§ѓа§Ьড়১ а§∞а§Ња§ѓ ৮а•З ৙ৌа§Ва§Ъ ৵а•Г১а•Н১а§Ъড়১а•На§∞ ৐৮ৌа§Па•§ а§∞а§ђа•Аа§В৶а•На§∞৮ৌ৕ ৆ৌа§Ха•Ба§∞, а§Ъড়১а•На§∞а§Ха§Ња§∞ ৵ড়৮а•Л৶ а§ђа§ња§єа§Ња§∞а•А а§Ѓа•Ба§Ца§∞а•На§Ьа•А (৶ а§З৮а§∞ а§Жа§З), а§≠а§∞১৮ৌа§Яа•На§ѓа§Ѓ ৮а•Г১а•На§ѓа§Ња§Ва§Ч৮ৌ а§ђа§Ња§≤а§Ња§Єа§∞а§Єа•Н৵১а•А (а§ђа§Ња§≤а§Њ) а§Фа§∞ а§Х৕ৌа§Ха§Ња§∞-а§Ъড়১а•На§∞а§Ха§Ња§∞ ৙ড়১ৌ а§Єа•Ба§Ха•Ба§Ѓа§Ња§∞ а§∞а§Ња§ѓ ৙а§∞а•§ а§≠а§Ња§∞১-а§Ъа•А৮ а§ѓа•Б৶а•На§І а§Ха•З ৵а§Ха•Н১ а§Ь৵ৌ৺а§∞а§≤а§Ња§≤ ৮а•За§єа§∞а•В ৙а§∞ а§Фа§∞ ৐ৌ৶ а§Ѓа•За§В а§ђа§Ња§Ва§Ча•На§≤ৌ৶а•З৴ а§Ѓа•Ба§Ха•Н১ড় а§Єа§Ва§Ша§∞а•На§Ј ৙а§∞ а§≠а•А а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓ ৐৮ৌ৮а•З а§Ха•А а§Й৮а§Ха•А а§Ц৊৵ৌ৺ড়৴ а§∞а§єа•Аа•§
вАШа§Єа§ња§Ха•На§Ха§ња§ЃвАЩ 1971 а§Ѓа•За§В ১৐ ৐৮а•А а§Ьа§ђ а§Єа§ња§Ха•На§Ха§ња§Ѓ а§≠а§Ња§∞১ а§Ча§£а§∞а§Ња§Ьа•На§ѓ а§Ха§Њ ৙а•На§∞৶а•З৴ ৮৺а•Аа§В а§єа•Ба§Ж ৕ৌ; ৵৺ а§≠а§Ња§∞১ а§Фа§∞ (а§Ъа•А৮ а§Ха•З а§Ха§ђа•На§Ьа•З ৵ৌа§≤а•З) ১ড়৐а•Н৐১ а§Ха•З а§ђа•Аа§Ъ а§Ха§Ња§ѓа§Ѓ а§Па§Х а§∞а§Ь৵ৌа•Ьа§Њ а§•а§Ња•§ ৵৺ৌа§В а§Ха•З ১১а•На§Ха§Ња§≤а•А৮ ৴ৌ৪а§Х (а§Ъа•Ла§Ча•На§ѓа§Ња§≤) ৙ৌа§≤а•На§°а•З৮ ৕а•Ла§Ва§°а•Б৙ ৮ৌুа§Ча•На§ѓа§Ња§≤ а§Єа•З ৪১а•На§ѓа§Ьড়১ а§∞а§Ња§ѓ а§Ха•З а§Ъа§Ъа•За§∞а•З а§≠а§Ња§И а§Ха§Њ а§Ѓа§ња§≤৮ৌ-а§Ьа•Ба§≤৮ৌ а§•а§Ња•§ а§≠а§Ња§И ৶ৌа§∞а•На§Ьа•Аа§≤а§ња§Ва§Ч а§Ѓа•За§В а§∞৺১а•З ৕а•За•§ а§∞а§Ња§ѓ а§Ха•А ৙৺а§≤а•А а§∞а§Ва§Ча•А৮ а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓ вАШа§Ха§Ва§Ъ৮а§Ьа§Ва§Ша§ЊвА٠৵৺а•Аа§В ৙а§∞ а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓа§Ња§И а§Ча§И, а§Ьа§ња§Єа§Ѓа•За§В а§≠а§Ња§И ৮а•З а§Ѓа§Ња§Ѓа•Ва§≤а•А а§≠а•Ва§Ѓа§ња§Ха§Њ а§≠а•А ৮ড়а§≠а§Ња§И ৕а•Аа•§ а§Й৮а•На§єа•Ла§В৮а•З а§Ъа•Ла§Ча•На§ѓа§Ња§≤ а§Ха•А ১а§∞а§Ђ а§Єа•З а§∞а§Ња§ѓ а§Ха•Л а§Єа§ња§Ха•На§Ха§ња§Ѓ ৙а§∞ а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓ ৐৮ৌ৮а•З а§Ха§Њ ৮а•На§ѓа•Л১ৌ а§¶а§ња§ѓа§Ња•§ ৵а•Г১а•Н১а§Ъড়১а•На§∞ а§Ха•З ৮ৌু ৙а§∞ а§∞а§Ња§ѓ а§Ха•З а§Цৌ১а•З а§Ѓа•За§В ১৐ а§∞а§ђа•Аа§В৶а•На§∞৮ৌ৕ ৆ৌа§Ха•Ба§∞ ৙а§∞ ৐৮ৌа§И а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓ а§єа•А ৕а•Аа•§
а§Єа§В৶а•А৙ а§∞а§Ња§ѓ а§Ха§Њ а§Х৺৮ৌ а§єа•И а§Ха§њ а§Ъа•Ла§Ча•На§ѓа§Ња§≤ а§Ха•А а§Еа§Ѓа•За§∞а§ња§Ха•А ৙১а•Н৮а•А а§єа•Л৙ а§Ха•Ба§Х, а§∞а§Ња§ѓ а§Ха•З а§Ха§Ња§Ѓ а§Єа•З а§ђа§Ца•Ва§ђа•А ৙а§∞а§ња§Ъড়১ ৕а•Аа•§ а§єа•Л а§Єа§Х১ৌ а§єа•И вАШа§Ха§Ва§Ъ৮а§Ьа§Ва§Ша§ЊвАЩ а§≠а•А а§Й৮а•На§єа•Ла§В৮а•З ৶а•За§Ца•А а§єа•Ла•§ ৵৺ ৪১а•На§ѓа§Ьড়১ а§∞а§Ња§ѓ а§Ха•А ৙৺а§≤а•А а§∞а§Ва§Ча•А৮ а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓ ৕а•Аа•§ а§Йа§Єа§Ха•З ৐ৌ৶ а§∞а§Ња§ѓ ৮а•З а§Ьа•Л а§Ча•На§ѓа§Ња§∞а§є а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓа•За§В ৐৮ৌа§И, ৵а•З а§Єа§ђ ৴а•Н৵а•З১-৴а•На§ѓа§Ња§Ѓ ৕а•Аа§Ва•§ вАШа§Ха§Ва§Ъ৮а§Ьа§Ва§Ша§ЊвАЩ а§Ха•З ৐ৌ৶ ৐৮а•А вАШа§Еа§∞а§£а•На§ѓа•За§∞ ৶ড়৮-а§∞ৌ১а•На§∞а§њвАЩ а§ѓа§Њ вАШа§Ъа§Ња§∞а•Ба§≤১ৌвАЩ а§Ьа•Иа§Єа•А а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓа•За§В ৪১а•На§ѓа§Ьড়১ а§∞а§Ња§ѓ а§Ха•А ৴а•Ба§∞а•Ба§Ж১а•А вАШ৙৕а•За§∞ ৙ৌа§Ва§Ъа§Ња§≤а•АвА٠৴а•Га§Ва§Ца§≤а§Њ (а§Е৙а•В-১а•На§∞а§ѓа•А) а§Ха•А ১а§∞а§є ৴а•Н৵а•З১-৴а•На§ѓа§Ња§Ѓ а§Ѓа•За§В а§єа•А а§Ьৌ৮৶ৌа§∞ а§≤а§Ч১а•А а§єа•Иа§Ва•§
а§≤а•За§Хড়৮, вАШа§Єа§ња§Ха•На§Ха§ња§ЃвАЩ а§Ха•З ৪ৌ৕ ৪১а•На§ѓа§Ьড়১ а§∞а§Ња§ѓ а§Єа•Н৕ৌৃа•А а§∞а•В৙ а§Єа•З а§∞а§Ва§Ча•А৮ ৶а•Ма§∞ а§Ѓа•За§В ৙а•На§∞৵а•З৴ а§Ха§∞ а§Ча§Па•§ а§ѓа§є а§Еа§єа§Ѓ ৐৶а§≤ৌ৵ а§Ъа•Ла§Ча•На§ѓа§Ња§≤ а§Ха•З а§ђа§Ьа§Я а§Фа§∞ а§єа•Л৙ а§Ха•Ба§Х а§Ха•З ৶а§Ца§≤ а§Ха•А ৵а§Ьа§є а§Єа•З а§Єа§Ва§≠৵ а§єа•Ба§Ж а§ѓа§Њ а§∞а§Ња§ѓ а§Ха•А а§Е৙৮а•А а§Ѓа§В৴ৌ а§Єа•З, а§Х৺৮ৌ а§Ѓа•Б৴а•На§Ха§ња§≤ а§єа•Иа•§ ৙а§∞৶а•З а§Ха•А а§∞а§Ва§Ча•А৮а•А а§ђа§∞а§Єа•Ла§В ৙৺а§≤а•З ৴а•Ба§∞а•В а§єа•Л а§Ъа•Ба§Ха•А ৕а•А, а§Ьа§ња§Єа•З ৪ৌ৆ а§Ха§Њ ৶৴а§Х ৴а•Ба§∞а•В а§єа•Л১а•З-৮-а§єа•Л১а•З вАШа§Ха§Ва§Ъ৮а§Ьа§Ва§Ша§ЊвАЩ а§Ѓа•За§В а§Жа§Ьа§Ѓа§Њ а§Ха§∞ ৵а•З а§Ыа•Ла•Ь а§Ъа•Ба§Ха•З ৕а•За•§
а§ђа§єа§∞а§єа§Ња§≤, а§Й৮а§Ха•А а§Фа§∞ а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓа•Ла§В а§Ха•З а§ђа§Ња§∞а•З а§Ѓа•За§В ১а•Л а§Ѓа•Иа§В৮а•З а§Єа•Ла§Ъа§Њ ৮৺а•Аа§В, ৙а§∞ вАШа§Єа§ња§Ха•На§Ха§ња§ЃвАЩ а§Е৙৮а•З а§∞а§Ва§Ча•Ла§В а§Ѓа•За§В а§єа•А а§Ца§ња§≤১а•А а§єа•Иа•§ а§Еа§Ѓа•За§∞а§ња§Ха•А а§Еа§Хৌ৶ুа•А ৮а•З а§Ѓа§єа§Ь ৙а•На§∞а§ња§Ва§Я а§Ха•З а§ђа§≤а§ђа•В১а•З а§Йа§Єа•З ৶а•Ба§∞а•Ба§Єа•Н১ ১а•Л а§Ха§ња§ѓа§Њ, ৙а§∞ а§Хড়১৮ৌ а§ѓа§є а§Ха§єа§Њ ৮৺а•Аа§В а§Ьа§Њ а§Єа§Ха§§а§Ња•§ а§Х৺৮а•З а§Ха§Њ а§≠ৌ৵ а§ѓа§є а§Ха§њ а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓ а§Ха•З а§Ѓа•Ва§≤ а§∞а•В৙ а§Ха§Њ а§Єа•Н১а§∞ ৮ড়৴а•На§Ъа§ѓ а§єа•А а§За§Є а§Й৶а•На§Іа§Ња§∞ ৵ৌа§≤а•З а§∞а•В৙ а§Єа•З а§Ка§Ва§Ъа§Њ а§∞а§єа§Њ а§єа•Ла§Ча§Ња•§
а§Єа§ња§Ха•На§Ха§ња§Ѓ ৐ৌ৵৮ ুড়৮а§Я а§Фа§∞ ১а•За§Иа§Є а§Єа•За§Ха§Ва§° а§Ха•А а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓ а§єа•Иа•§ а§Єа§Ва§≠৵ а§єа•И, а§Ѓа•Ва§≤ а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓ ৕а•Ла•Ьа•А а§ђа•Ьа•А а§∞а§єа•А а§єа•Ла•§ а§За§Є а§Е৮а•Бুৌ৮ а§Ха•А ৶а•Л ৵а§Ьа§єа•За§В а§єа•Иа§Ва•§ ৪১а•На§ѓа§Ьড়১ а§∞а§Ња§ѓ а§Ха•А а§ђа•З৺১а§∞а•А৮ а§Ьа•А৵৮а•А вАШ৶ а§З৮а§∞ а§Жа§ЗвАЩ а§≤а§ња§Ц৮а•З ৵ৌа§≤а•А а§Па§Ва§°а•На§∞а§ѓа•В а§∞а•Й৐ড়৮৪৮ а§Ха•Л а§∞а§Ња§ѓ ৐১ৌ১а•З а§єа•Иа§В а§Ха§њ вАШа§Єа§ња§Ха•На§Ха§ња§ЃвАЩ а§Ха•З ৴а•Ба§∞а•В а§Ѓа•За§В ৪ৌ১ ুড়৮а§Я ১а§Х а§Й৮а•На§єа•Ла§В৮а•З а§Ха•Ла§И а§Ха§Ѓа•За§Ва§Яа•На§∞а•А ৮৺а•Аа§В а§Ха•А (а§Еа§Ѓа•Вু৮ ৵а•Г১а•Н১а§Ъড়১а•На§∞ а§Ѓа•За§В а§∞а§Ња§ѓ а§Ца•Б৶ а§Ха§Ѓа•За§Ва§Яа•На§∞а•А а§Ха§∞১а•З ৕а•З)а•§ а§ѓа§є ৐ৌ১ а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓ а§Ха•А ৴а•Ба§∞а•Ба§Ж১ а§Ѓа•За§В а§єа§∞ а§Ха•Ла§И а§≤а§Ха•На§Ја•На§ѓ а§Ха§∞а•За§Ча§Њ а§Ха§њ ৶а•За§∞ ১а§Х ৶а•Ва§∞-৶а•Ва§∞ а§Ха•Ла§И ৴৐а•Н৶ а§Єа•Б৮ৌа§И ৮৺а•Аа§В ৙а•Ьа§§а§Ња•§ а§Ха•З৵а§≤ а§Єа•Ма§В৶а§∞а•На§ѓ а§Ха•А а§Е৙а•Ва§∞а•Н৵ ৶а•Г৴а•Нৃৌ৵а§≤а•А а§Ха•З ৪ৌ৕ ৙а§∞৶а•З ৙а§∞ ১а•Иа§∞১а•А ৙а§∞а•Н৵১-а§Ша§Ња§Яа§ња§ѓа•Ла§В а§Ха•А а§Ж৵ৌа§Ьа§Ља•За§В, ৙а§Ха•На§Ја§ња§ѓа•Ла§В а§Ха•А а§Ъа§єа§Ъа§єа§Ња§єа§Я, ু৵а•З৴ড়ৃа•Ла§В а§Ха•А а§∞а•Б৮-а§Эа•Б৮, ৙а•Ба§Ја•Н৙ а§≤৶а•А а§°а§Ња§≤а§ња§ѓа•Ла§В а§Ха•А а§Єа§∞а§Єа§∞а§Ња§єа§Я, ৮৶а•А а§Ха•А а§Ха§≤-а§Ха§≤, а§Эа§∞৮а•З а§Ха•А а§Ыа•Ба§≤-а§Ыа•Ба§≤, а§ђа§Ња§∞ড়৴ а§Ха•А а§Я৙-а§Я৙ а§Фа§∞ а§≤а•Ла§Ха§Єа§Ва§Ча•Аа§§а•§
৙а§∞ а§Й৙а§≤а§ђа•На§І а§єа•Ба§И а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓ а§Ѓа•За§В а§ѓа§є ৮ড়:৴৐а•Н৶ а§Єа§ња§≤а§Єа§ња§≤а§Њ ১а•А৮ ুড়৮а§Я ৐ৌ৶ ৕ু а§Ьৌ১ৌ а§єа•Иа•§ ৪১а•На§ѓа§Ьড়১ а§∞а§Ња§ѓ а§Єа§ња§Ха•На§Ха§ња§Ѓ а§Ха•З а§≠а•Ва§Ча•Ла§≤ а§Ха§Њ а§≠а§Ња§Ја•На§ѓ ৴а•Ба§∞а•В а§Ха§∞১а•З а§єа•Иа§Ва•§ а§Ьа§Ња§єа§ња§∞ а§єа•И, а§≤а§Ча§≠а§Ч а§Ъа§Ња§∞ ুড়৮а§Я а§Ха§Њ ৶а•Г৴а•На§ѓа§Ња§Ва§Х৮ а§ѓа§єа§Ња§В а§Ча§Ња§ѓа§ђ а§єа•Иа•§ а§Ра§Єа•З а§єа•А, ৐১ৌৃৌ а§Ьৌ১ৌ а§єа•И, а§Ѓа§єа§≤ а§Ха•З а§≠а•Ла§Ь а§Ха•З ৪ৌ৕ а§Ча§∞а•Аа§ђа•Ла§В а§Ха§Њ а§Ьа•В৆৮ а§Цৌ৮ৌ, а§Еа§Ѓа•За§∞а§ња§Ха•А а§Ѓа•Ва§≤ а§Ха•А а§∞ৌ৮а•А а§Ха•Л ৮৺а•Аа§В а§Ьа§Ѓа§Њ а§•а§Ња•§ ৵৺ ৶а•Г৴а•На§ѓ а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓ а§Ѓа•За§В ৮৺а•Аа§В а§єа•Иа•§ а§∞а•Й৐ড়৮৪৮ а§Ха•Л а§∞а§Ња§ѓ ৐১ৌ১а•З а§єа•Иа§В а§Ха§њ а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓ а§Ха•З а§Ха§Ъа•На§Ъа•З а§∞а•В৙ а§Ѓа•За§В а§Па§Х а§Ьа§Ча§є ৮а•Ва§°а§≤ а§Цৌ১а•З ৵а§∞а§ња§Ја•Н৆ ৮а•Ма§Ха§∞৴ৌ৺ а§Ха§Њ ৶а•Г৴а•На§ѓ ৶а•За§Ца§Ха§∞ а§∞ৌ৮а•А а§ђа•Ла§≤а•А а§Ха§њ а§ѓа§є (৶а•Г৴а•На§ѓ) ৴а§∞а§Ња§∞১৮ а§≤а§Ч১ৌ а§єа•И! а§∞а§Ња§ѓ а§Х৺১а•З а§єа•Иа§В, ৵а•З а§Єа§Ѓа§Э а§Ча§П а§Ха§њ а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓ а§Ха§Њ а§ѓа§є а§єа§ња§Єа•На§Єа§Њ ৮৺а•Аа§В а§ђа§Ъа•За§Ча§Ња•§
а§∞ৌ৮а•А а§Ха•З а§За§Є а§ђа§∞১ৌ৵ а§Єа•З ৪১а•На§ѓа§Ьড়১ а§∞а§Ња§ѓ а§Ж৺১ а§єа•Ба§П а§єа•Ла§Ва§Ча•За•§ а§Й৮а•На§єа•Ла§В৮а•З а§Ха§И а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓа•За§В а§Єа§∞а§Ха§Ња§∞а•А а§Ца§∞а•На§Ъ а§Фа§∞ а§Єа§Ња§Ва§Єа•Н৕ৌ৮ড়а§Х а§Жа§Ча•На§∞а§є ৙а§∞ ৐৮ৌа§Иа§В, ৙а§∞ а§За§Є ১а§∞а§є а§Ха•А а§ђа§В৶ড়৴ а§Фа§∞ ৐ৌ৶ а§Ѓа•За§В а§Єа§∞а§Ха§Ња§∞а•А а§∞а•Ла§Х, а§Й৮а•На§єа•За§В а§Ха§єа•Аа§В а§Фа§∞ а§Эа•За§≤৮а•З а§Ха•Л а§Ѓа§ња§≤а•А а§єа•Л, а§За§Єа§Ха§Њ ৺৵ৌа§≤а§Њ ৮৺а•Аа§В а§Ѓа§ња§≤а§§а§Ња•§ ৴ৌৃ৶ а§За§Єа•Аа§≤а§ња§П ৵а•З вАШа§Єа§ња§Ха•На§Ха§ња§ЃвАЩ а§Ха•А а§Ъа§∞а•На§Ъа§Њ а§Ха§єа•Аа§В а§Ца•Б৶ а§Ха§∞১а•З ৮৺а•Аа§В а§Ѓа§ња§≤১а•З, а§Ьа§ђа§Ха§њ а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓ ৙а§∞ а§Й৮а•На§єа•Ла§В৮а•З а§Ха§Ња§Ђа•А ৵а§Ха•Н১ а§≤а§Ча§Ња§ѓа§Ња•§ а§Ца•Б৶ а§Жа§≤а•За§Ц а§≤а§ња§Ца§Њ, ৙а•Эа§Њ, а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓ а§Ха§Њ а§Єа§Ва§Ча•А১ ১а•Иа§ѓа§Ња§∞ а§Ха§ња§ѓа§Ња•§ ৮ড়а§∞а•Н৶а•З৴৮ ১а•Л ৕ৌ а§єа•Аа•§ а§Єа§В৶а•А৙ а§Х৺১а•З а§єа•Иа§В а§Ха§њ а§Й৮а•На§єа•За§В ৃৌ৶ а§єа•И а§ђа§Ња§ђа§Њ (а§∞а§Ња§ѓ) а§ѓа•В৮ড়а§Я а§Ха•Л а§Ра§Єа•А ৶а•Ба§∞а•На§Ча§Ѓ а§Ка§Ва§Ъа§Ња§За§ѓа•Ла§В ৙а§∞ а§≤а•З а§Ча§П а§Ьа§єа§Ња§В а§Ж৐ৌ৶а•А ১а•Л ৕а•А, ৙а§∞ ৮ а§ђа§ња§Ьа§≤а•А ৕а•А ৮ ৙৺а•Ба§Ва§Ъ৮а•З а§Ха•З а§Єа•Аа§Іа•З а§∞а§Ња§Єа•Н১а•З а§Фа§∞ а§ѓа§є ৙а§∞ড়৴а•На§∞а§Ѓ а§Й৮а•На§єа•Ла§В৮а•З а§Ъа•Ла§Ча•На§ѓа§Ња§≤ а§∞а§Ња§Ь а§Ха•З ১৕ৌа§Х৕ড়১ а§Єа•Б৴ৌ৪৮, ৵ড়а§Ха§Ња§Є, а§∞а§Ња§Ьа§Њ-а§∞ৌ৮а•А а§Ха•А а§≤а•Ла§Х৙а•На§∞ড়ৃ১ৌ а§Фа§∞ а§Ь৮а•Л৮а•На§Ѓа•Ба§Ц ৵а•Нৃ৵৺ৌа§∞ а§Ха•З а§Ы৶а•На§Ѓ а§Ъড়১а•На§∞а§£ а§Ха•З а§≤а§ња§П а§Ха§ња§ѓа§Ња•§
৶ৌа§∞а•На§Ьа•Аа§≤а§ња§Ва§Ч а§Ѓа•За§В а§Й৮а§Ха•З а§≠а§Ња§И ৮а•З вАШа§Єа§В৙ৌ৶а§Ха•Аа§ѓ а§Жа§Ь৊ৌ৶а•АвАЩ а§Ха§Њ а§Ьа•Л а§≠а§∞а•Ла§Єа§Њ ৶ড়ৃৌ ৕ৌ, ৵৺ а§Ча§Ва§Ча§Яа•Ла§Х а§Ѓа•За§В ৺৵ৌ а§єа•Л а§Ча§ѓа§Њ, а§єа§Ња§≤а§Ња§Ва§Ха§њ а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓ ৐৮ৌ৮а•З а§Ха•З ৶а•Л а§Єа§Ња§≤ ৐ৌ৶ а§єа•А а§Ъа•Ла§Ча•На§ѓа§Ња§≤ а§Ха•А а§Еа§≤а•Ла§Х৙а•На§∞ড়ৃ১ৌ а§Ь৮১ৌ а§Ха•З а§∞а•Ла§Ј а§Ѓа•За§В ৐৶а§≤ а§Ча§Иа•§ а§ѓа•Ла§В а§Єа§ња§Ха•На§Ха§ња§Ѓ ৕а•Ла•Ьа§Њ-а§ђа§єа•Б১ (а§∞а§Ха•На§Ја§Њ, а§Ха•Ва§Я৮а•А১ড় а§Фа§∞ а§Єа§Ва§Ъа§Ња§∞ а§Ѓа•За§В) а§≠а§Ња§∞১ а§Ха•З а§Еа§Іа§ња§∞а§Ња§Ь а§Ѓа•За§В ৕ৌ, ৙а§∞ а§∞а§Ь৵ৌа•Ьа•З а§Ха§Њ а§∞а§Ња§Ь৙ৌа§Я а§Єа•Н৵ৌৃ১а•Н১ а§•а§Ња•§ а§Ъа•Ла§Ча•На§ѓа§Ња§≤ а§Ха•З а§Ѓа§єа§≤ а§Ха•З ৪ৌু৮а•З 1973 а§Ѓа•За§В а§єа§ња§Ва§Єа§Х ৵ড়а§∞а•Ла§І а§єа•Ба§Жа•§ а§Єа§ња§Ха•На§Ха§ња§Ѓ а§Ха•З ৙а•На§∞৲ৌ৮ুа§В১а•На§∞а•А ৮а•З а§∞а§Ь৵ৌа•Ьа•З а§Ха•Л а§≠а§Ња§∞১ а§Ѓа•За§В ৴ৌুড়а§≤ а§Ха§∞৮а•З а§Ха•А а§Е৙а•Аа§≤ а§Ха•Аа•§ а§≠а§Ња§∞১а•Аа§ѓ а§Єа•З৮ৌ а§Ча§Ва§Ча§Яа•Ла§Х ৙৺а•Ба§Ва§Ъа•А а§Фа§∞ а§Ъа•Ла§Ча•На§ѓа§Ња§≤ а§ђа•З৶а§Ца§≤ а§єа•Л а§Ча§Па•§
а§Па§Х а§Ь৮ু১-а§Єа§Ва§Ча•На§∞а§є а§Ха§ња§ѓа§Њ а§Ча§ѓа§Њ, а§Ьа§ња§Єа§Ѓа•За§В а§≤а§Ча§≠а§Ч а§Єа§≠а•А а§≤а•Ла§Ч (97.5 ৙а•На§∞১ড়৴১) а§≠а§Ња§∞১ а§Ѓа•За§В ৵ড়а§≤а§ѓ а§Ха•З а§єа§Х а§Ѓа•За§В ৪ৌু৮а•З а§Жа§Па•§ а§≠а§Ња§∞১ а§Ха•З а§Єа§В৵ড়৲ৌ৮ а§Ѓа•За§В ৙а•Иа§В১а•А৪৵ৌа§В а§Єа§В৴а•Л৲৮ а§Ха§∞ а§Ѓа§И, 1975 а§Ѓа•За§В а§Єа§ња§Ха•На§Ха§ња§Ѓ а§Ха•Л вАШа§Єа§єа§Ња§ѓа§Х а§∞а§Ња§Ьа•На§ѓвАЩ а§Ха§Њ ৶а§∞а•На§Ьа§Њ ৶а•З ৶ড়ৃৌ а§Ча§ѓа§Ња•§ ৐ৌ৶ а§Ѓа•За§В а§Па§Х а§Фа§∞ а§Єа§В৴а•Л৲৮ а§Ха•З ৐ৌ৶ ৵৺ а§Єа§В৵ড়৲ৌ৮ а§Ха•А ৙৺а§≤а•А а§Єа•Ва§Ъа•А а§Ха§Њ а§∞а§Ња§Ьа•На§ѓ ৐৮ а§Ча§ѓа§Ња•§ а§Х৺১а•З а§єа•Иа§В, а§Ъа•Ла§Ча•На§ѓа§Ња§≤ ৮а•З ৪১а•На§ѓа§Ьড়১ а§∞а§Ња§ѓ а§Єа•З а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓ а§За§Єа§≤а§ња§П ৐৮৵ৌа§И ৕а•А, ১ৌа§Ха§њ а§≠а§Ња§∞১ а§ѓа§Њ а§Ъа•А৮ а§Ха•З ৪ৌু৮а•З а§Еа§В১а§∞а§∞а§Ња§Ја•На§Яа•На§∞а•Аа§ѓ ৶৐ৌ৵ ৐৮ а§Єа§Ха•За•§ а§∞а§Ња§ѓ а§Ха•А а§Ха•Аа§∞а•Н১ড় ১৐ ১а§Х а§Єа§Ња§∞а•З а§Єа§Ва§Єа§Ња§∞ а§Ѓа•За§В а§Ђа•Иа§≤ а§Ъа•Ба§Ха•А ৕а•Аа•§
৪১а•На§ѓа§Ьড়১ а§∞а§Ња§ѓ ৮а•З а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓ а§≠а§≤а•З а§єа•А а§Ъа•Ла§Ча•На§ѓа§Ња§≤ а§Ха•З а§≤а§ња§П ৐৮ৌа§И, ৙а§∞ а§Й৮а•На§єа•За§В а§ѓа§є а§Еа§єа§Єа§Ња§Є ৕ৌ а§Ха§њ а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓ а§Ха•Л ৮ড়ৣа•Н৙а§Ха•На§Ј ৮৺а•Аа§В а§∞а§Ц ৙ৌа§П а§єа•Иа§Ва•§ а§Й৮৪а•З а§єа•Ба§И ৐ৌ১а§Ъа•А১ а§Ха•З ৺৵ৌа§≤а•З а§Єа•З а§∞а•Й৐ড়৮৪৮ а§Х৺১а•З а§єа•Иа§В а§Ха§њ а§Ъа§Ња§≤а•Аа§Є ৙а•На§∞১ড়৴১ а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓ а§Єа§∞а§Ха§Ња§∞а•А а§Жа§Ва§Ха•Ьа•Ла§В-а§Ьৌ৮а§Ха§Ња§∞а§ња§ѓа•Ла§В ৙а§∞ ৐৮ৌ৮а•А ৙а•Ьа•Аа•§ ৶а•Ва§Єа§∞а•З, а§Йа§Єа§Ѓа•За§В ৮а•З৙ৌа§≤а•А а§Єа§Ѓа•Б৶ৌৃ а§Ха§Њ а§Єа§Ѓа•Ба§Ъড়১ ৙а•На§∞১ড়৮ড়৲ড়১а•Н৵ ৮৺а•Аа§В а§єа•Ба§Жа•§ а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓ ৶а•За§Ц১а•З а§єа•Ба§П а§ѓа§є а§Ѓа§єа§Єа•Ва§Є а§єа•Л১ৌ а§≠а•А а§єа•И а§Ха§њ ৵а•Г১а•Н১а§Ъড়১а•На§∞ а§Ѓа•За§В ৪১а•На§ѓа§Ьড়১ а§∞а§Ња§ѓ, ৮а•З৙ৌа§≤ а§Єа•З а§Жа§И а§Ж৐ৌ৶а•А а§Ха•Л а§Ьа•Нৃৌ৶ৌ ৐১ৌ১а•З а§єа•Иа§В, ৙а§∞ а§Й৮а§Ха§Њ а§Ьа•А৵৮, а§∞৺৮-৪৺৮ а§Фа§∞ а§∞а•А১ড়-а§∞ড়৵ৌа§Ьа§Љ а§Ж৶ড় а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓ а§Ѓа•За§В а§Єа§ња§∞а•З а§Єа•З а§Ча§Ља§Ња§ѓа§ђ а§єа•Иа§Ва•§ ৮а•З৙ৌа§≤а•А ৵৺ৌа§В а§Ха•А а§ђа•Ла§≤а§Ъа§Ња§≤ а§Ха•А а§≠а§Ња§Ја§Њ а§єа•И, ৵৺ а§≠а•А а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓ а§Ѓа•За§В а§Ха§єа•Аа§В а§Єа•Б৮ৌа§И ৮৺а•Аа§В ৙а•Ь১а•А, а§Ьа§ђа§Ха§њ а§Єа•Н৕ৌ৮а•Аа§ѓ а§ђа•М৶а•На§І а§Єа§Ѓа•Б৶ৌৃ а§Ха•З а§Ъа•За§єа§∞а•З, ৵а•З৴, ৴а•Га§Ва§Ча§Ња§∞, ু৆, а§Ѓа§В১а•На§∞а•Ла§Ъа•На§Ъа§Ња§∞, ৙а•На§∞а§Ња§∞а•Н৕৮ৌа§Па§В а§Фа§∞ ১а•На§ѓа•Ла§єа§Ња§∞ а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓ а§Ѓа•За§В а§Ыа§Ња§П а§∞৺১а•З а§єа•Иа§Ва•§
а§З১৮ৌ а§єа•А ৮৺а•Аа§В, а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓ а§Ха§Њ а§Еа§В১ড়ু а§єа§ња§Єа•На§Єа§Њ а§Єа§ња§Ха•На§Ха§ња§Ѓ а§Ха•З ৙ৌа§∞а§В৙а§∞а§ња§Х ৵а§∞а•На§Ја§Ња§В১ ৙а§∞ а§∞а§Ња§Ьа§Ѓа§єа§≤ ৙а§∞а§ња§Єа§∞ а§Ѓа•За§В а§єа§∞ а§Єа§Ња§≤ а§єа•Л৮а•З ৵ৌа§≤а•З а§Ха§Ња§∞а§Ча•За§Я а§Єа§Ѓа§Ња§∞а•Ла§є ৙а§∞ а§Ха•За§В৶а•На§∞ড়১ а§єа•Иа•§ ৪১а•На§∞а§є ুড়৮а§Я а§За§Є а§Й১а•Н৪৵ ৙а§∞ ৵а•Нৃ১а•А১ а§єа•Л১а•З а§єа•Иа§В, ৃৌ৮а•А а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓ а§Ха§Њ а§Па§Х ১ড়৺ৌа§И а§≠а§Ња§Ча•§ а§Єа§Ѓа§Ња§∞а•Ла§є а§Ѓа•За§В а§Жа§Ѓ а§Фа§∞ а§Ца§Ња§Є а§≤а•Ла§Ч а§≠а•А а§Ца•Ва§ђ а§єа•Иа§В, ৙а§∞ а§Ха•За§В৶а•На§∞ а§Ѓа•За§В а§Єа§Ьа§Њ-а§Іа§Ьа§Њ а§∞а§Ња§Ьа§Ѓа§єа§≤ а§Фа§∞ ৮ৌুа§Ча•На§ѓа§Ња§≤ ৙а§∞ড়৵ৌа§∞ а§єа•Иа•§ ৮а§Ьа§Ља§∞ৌ৮ৌ а§Єа•Н৵а•Аа§Ха§Ња§∞ а§Ха§∞১а•З а§Ъа•Ла§Ча•На§ѓа§Ња§≤, ৶а§Вৰ৵১ а§Ха§∞১а•А ৙а•На§∞а§Ьа§Њ, ৴ৌ৺а•А а§ђа•Иа§Ва§°, ৴ৌ৺а•А а§≠а•Ла§Ь, а§Іа§Ња§∞а•На§Ѓа§ња§Х а§∞а§Єа•На§Ѓ-а§У-а§∞ড়৵ৌа§Ьа§Ља•§
а§Ха•На§ѓа§Њ ৪১а•На§ѓа§Ьড়১ а§∞а§Ња§ѓ а§Ха•З ু৮ а§Ѓа•За§В ৐ৌ৶ а§Ѓа•За§В а§За§Є а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓ а§Ха•Л а§≤а•За§Ха§∞ а§Ха•Ба§Ы а§Ча•На§≤ৌ৮ড় а§Ха§Њ а§≠ৌ৵ а§∞а§єа§Њ? а§Ха•М৮ а§Ьৌ৮ а§Єа§Х১ৌ а§єа•И? а§єа•Л а§Єа§Х১ৌ а§єа•И, а§Єа§ња§∞а•На§Ђ а§Еа§Єа§В১а•Ла§Ј а§∞а§єа§Њ а§єа•Ла•§ а§Е৙৮а•З а§Ьа•А৵৮а•Аа§Ха§Ња§∞ а§Ха•З а§Єа§Ѓа§Ха•На§Ј ৵а•З а§З১৮ৌ а§єа•А вАШа§Єа§В১а•Ла§ЈвА٠৙а•На§∞а§Ха§Я а§Ха§∞১а•З а§єа•Иа§В а§Ха§њ а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓ а§Ха•З ৴а•Ба§∞а•В а§Ха•З вАШа§Хৌ৵а•Нৃৌ১а•На§Ѓа§Х ৪ৌ১ ুড়৮а§ЯвА٠৵а•З а§Е৙৮а•А а§Ѓа§∞а§Ьа•А а§Ха•З а§∞а§Ц а§Єа§Ха•З а§ѓа§Њ а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓ а§Ха§Њ вАШа§Ьа•А৵а§В১ а§Фа§∞ а§Ж৴ৌ৵ৌ৶а•АвАЩ а§Еа§В১, ৙а§∞ а§За§Єа•З а§∞а§Ња§ѓ а§Ха§Њ а§ђа•Ь৙а•Н৙৮ а§єа•А а§Єа§Ѓа§Эа§ња§П! ৵а§∞৮ৌ а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓ ৙а§∞ а§Й৮а§Ха•А а§Ыৌ৙ а§єа§∞ а§Ьа§Ча§є ৮а•Ба§Ѓа§Ња§ѓа§Ња§В а§єа•Иа•§
১৕а•На§ѓа•Ла§В а§Фа§∞ а§∞а§Ња§Ьৌ৴ৌ৺а•А а§Ха•Л а§Ыа•Ла•Ь ৶а•За§В, а§Ьа•Л ৵а§Ха•Н১ а§Ха•З ৕৙а•За•Ьа•Ла§В а§Ѓа•За§В а§Ца•Б৶ а§Е৙а•На§∞а§Ња§Єа§Ва§Ча§ња§Х а§єа•Л а§Ьৌ১а•З а§єа•Иа§В, ১а•Л вАШа§Єа§ња§Ха•На§Ха§ња§ЃвАЩ а§Єа§Ња§Іа§Ња§∞а§£ ৵а•Г১а•Н১а§Ъড়১а•На§∞ ৮৺а•Аа§Ва•§ ৵৺ ৙а•На§∞а§Ха•Г১ড় а§Ха§Њ а§Й১а•Н৪৵ а§єа•Иа•§ а§Єа•Ма§В৶а§∞а•На§ѓ а§Ха§Њ ৮ৌ৶ а§єа•Иа•§ а§Єа•Ба§Ц৶ а§∞а§Ва§Ча•Ла§В а§Ха•А а§ђа§∞৪ৌ১ а§єа•Иа•§ а§Фа§∞ а§Ха•Ла§Ѓа§≤ а§Іа•Н৵৮ড়ৃа•Ла§В а§Ха§Њ а§За§В৶а•На§∞৲৮а•Ба§Ја•§
৵ড়а§Ха§Ња§Є а§Ха•А а§Чৌ৕ৌ а§Ѓа•За§В а§≠а•А ৪১а•На§ѓа§Ьড়১ а§∞а§Ња§ѓ а§Е৙৮а•А ৐ৌ১ а§∞а§Ц৮а•З а§Ха§Њ а§Е৵а§Хৌ৴ ৥а•Ва§Ва•Э а§≤а•З১а•З а§єа•Иа§Ва•§ ৵а•З ৐১ৌ১а•З а§єа•Иа§В а§Ха§њ а§Єа§ња§Ха•На§Ха§ња§Ѓ ৴ৌ৪৮ а§Ха•А а§Уа§∞ а§Єа•З ৴ড়а§Ха•На§Ја§Њ а§Ѓа•Ба§Ђа•Н১ а§єа•И, ৙а•Ва§∞а•З а§ђа§Ьа§Я а§Ха§Њ а§Па§Х а§Ъа•М৕ৌа§И ৴ড়а§Ха•На§Ја§Њ ৙а§∞ а§Ца§∞а•На§Ъ а§єа•Л১ৌ а§єа•И, а§Ђа§ња§∞ а§За§Ха§≤а•М১а•З ৙৐а•На§≤а§ња§Х а§Єа•На§Ха•Ва§≤ а§Ха•З ৶а•Г৴а•На§ѓ а§Фа§∞ ৶а•А৵ৌа§∞ ৙а§∞ а§Ъа•Ла§Ча•На§ѓа§Ња§≤ ৶а§В৙১ড় а§Ха•А ১৪а•Н৵а•Аа§∞а•За§В ৶ড়а§Ца§Ња§Ха§∞ ৵а•З ৶а•Ва§Єа§∞а•А а§Єа§∞а§Ха§Ња§∞а•А а§Єа•На§Ха•Ва§≤а•Ла§В а§Ха§Њ а§єа§Ња§≤ ৶ড়а§Цৌ১а•З а§єа•Иа§Ва•§ а§ђа§Ча•Иа§∞ а§Ха§єа•З а§Ча§Ља§∞а•Аа§ђ а§Фа§∞ а§Еа§Ѓа•Аа§∞ а§Ха•А а§Ца§Ња§И а§Ха•А а§Уа§∞ а§З৴ৌа§∞а§Њ а§Ха§∞১а•З а§єа•Ба§Па•§
а§За§Єа•А ১а§∞а§є а§∞а§Ња§Ьа§Ѓа§єа§≤ ৙а§∞а§ња§Єа§∞ а§Ха•З а§Ѓа•За§≤а•З৮а•Ба§Ѓа§Њ а§Й১а•Н৪৵ а§Ѓа•За§В ৵а•З ৴ৌ৺а•А а§Ѓа•З৺ুৌ৮а•Ла§В а§Ха•А ৮а•Аа§∞а§Є ৴ড়а§∞а§Х১ а§Фа§∞ а§∞ৌ৮а•А а§Ха•А ৆а§Ва§°а•А а§Ѓа•За§Ь৐ৌ৮а•А а§Ха•З ৶а•Г৴а•На§ѓа•Ла§В а§Ха•З а§ђа•Аа§Ъ а§Ча§Ља§∞а•Аа§ђ а§≤а•Ла§Ча•Ла§В а§Ха•А а§Ъа§єа§≤-৙৺а§≤ а§≠а§∞а•А ৙а§Ва§Ч১, ৮ৌа§Ъ-а§Чৌ৮, а§Ца•За§≤-а§Ха•В৶ а§Ха•З ৶а•Г৴а•На§ѓ ৶ড়а§Ца§Ња§Ха§∞ а§Е৙৮ৌ а§Ѓа§В১৵а•На§ѓ а§Єа§Ња§Ђ а§Ха§∞ ৶а•З১а•З а§єа•Иа§Ва•§ а§Й১а•Н৪৵ а§Ѓа•За§В а§Х৶ু-а§Х৶ু ৙а§∞ ৮ৌа§Ъ১а•З-а§Ха•В৶১а•З а§Ѓа•Ба§Ца•Ма§Яа§Њ-а§Іа§Ња§∞а•А а§Ѓа§Єа§Ца§∞а•Ла§В а§Ха•А а§Й৙৪а•Н৕ড়১ড় а§ђа•Ьа•А ৙а•На§∞১а•Аа§Хৌ১а•На§Ѓа§Х а§єа•Иа•§ а§Ъа•Ла§Ча•На§ѓа§Ња§≤ а§Ха•З ৙а•На§∞৵а•З৴ ৙а§∞ ৵а•З а§Е৙৮а•А а§Е৶ৌ а§Ѓа•За§В а§Ьа§ња§Є ১а§∞а§є вАШ৶а§Вৰ৵১вАЩ а§Ха§∞১а•З а§єа•Иа§В, ৵৺ а§Й৙৺ৌ৪ а§Ха§Њ а§Єа§Њ ৶а•Г৴а•На§ѓ ৐৮ а§Ьৌ১ৌ а§єа•Иа•§ а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓ а§Ѓа•За§В а§∞а§Ња§ѓ а§Ха•А а§Єа§Іа•А а§єа•Ба§И а§Ха§Ѓа•За§Ва§Яа•На§∞а•А а§єа•И, а§≤а•За§Хড়৮ а§Ха§И а§Ьа§Ча§є а§Ъа•Б৙а•Н৙а•А а§єа•Иа•§ а§ѓа§Њ а§Єа§Ва§Ча•Аа§§а•§ а§Л১а•Н৵ড়а§Х а§Ша§Яа§Х а§Єа•З а§Йа§≤а§Я а§∞а§Ња§ѓ а§Ха•А а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓа•Ла§В а§Ѓа•За§В а§Жু১а•Ма§∞ ৙а§∞ ৴৐а•Н৶а•Ла§В а§Ха•А а§ђа§єа•Б১ৌৃ১ а§Ѓа§ња§≤১а•А а§єа•И, ৙а§∞ вАШа§Єа§ња§Ха•На§Ха§ња§ЃвА٠৵а•Г১а•Н১а§Ъড়১а•На§∞ а§єа•Л১а•З а§єа•Ба§П а§≠а•А а§Е৙৵ৌ৶ а§єа•Иа•§ а§Й৮а§Ха•З ৶а•Ва§Єа§∞а•З ৵а•Г১а•Н১а§Ъড়১а•На§∞а•Ла§В а§Ѓа•За§В а§Ьа•Л а§За§Ва§Яа§∞৵а•На§ѓа•В а§Фа§∞ ৮ৌа§Яа•На§ѓ-а§∞а•В৙а•А а§Еа§≠ড়৮а•А১ ৶а•Г৴а•На§ѓ а§Ѓа§ња§≤১а•З а§єа•Иа§В, ৵а•З а§≠а•А а§За§Єа§Ѓа•За§В ৮৺а•Аа§В а§єа•Иа§Ва•§ а§Єа§В৙ৌ৶৮ а§Ъа•Ба§Єа•Н১ а§єа•И, ৙а§∞ а§Єа§В৙ৌ৶а§Х а§Ха§Њ ৮ৌু а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓ а§Ѓа•За§В ৮৺а•Аа§В а§єа•Иа•§
вАШа§Єа§ња§Ха•На§Ха§ња§ЃвАЩ а§Ха§Ва§Ъ৮а§Ьа§Ва§Ша§Њ а§Ха•А а§Єа•Н৵а§∞а•На§£а§ња§Ѓ ৲৵а§≤ а§Ы৵ড় а§Єа•З ৴а•Ба§∞а•В а§єа•Л১а•А а§єа•И, а§Ха§Ва§Ъ৮а§Ьа§Ва§Ша§Њ ৙а§∞ а§єа•А а§Ц১а•На§Ѓа•§ вАШа§Ха§Ва§Ъ৮а§Ьа§Ва§Ша§ЊвАЩ а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓ а§Єа•З ৆а•Аа§Х а§єа§Яа§Ха§∞, а§Ьа§ња§Єа§Ѓа•За§В ৵а•З а§За§Є ৙а§∞а•Н৵১-৴а•Га§Ва§Ца§≤а§Њ а§Ха§Њ ৶а•Г৴а•На§ѓ а§Єа§ња§∞а•На§Ђ а§Еа§В১ а§Ѓа•За§В ৶ড়а§Цৌ১а•З а§єа•Иа§Ва•§ а§∞а§Ња§ѓ ৐১ৌ১а•З а§єа•Иа§В а§Ха§њ ৶а•Б৮ড়ৃৌ а§Ха•А ১а•Аа§Єа§∞а•А а§Єа§ђа§Єа•З а§Ка§Ва§Ъа•А а§Ъа•Ла§Яа•А а§Ха§Ва§Ъ৮а§Ьа§Ва§Ша§Њ а§Єа§ња§Ха•На§Ха§ња§Ѓ а§Ѓа•За§В ৙а•Ь১а•А а§єа•И а§Фа§∞ а§Єа§ња§Ха•На§Хড়ু৵ৌ৪а•А а§Йа§Єа•З ৶а•И৵а•Аа§ѓ а§∞а•В৙ а§Єа§Ѓа§Э১а•З а§єа•Иа§Ва•§ (৵а•Иа§Єа•З 1852 ১а§Х ১а•Л а§Ха§Ва§Ъ৮а§Ьа§Ва§Ша§Њ а§Ха•Л а§єа•А ৶а•Б৮ড়ৃৌ а§Ха•А а§Єа§ђа§Єа•З а§Ка§Ва§Ъа•А а§Ъа•Ла§Яа•А а§Єа§Ѓа§Эа§Њ а§Ьৌ১ৌ ৕ৌ, ৐ৌ৶ а§Ѓа•За§В а§Е৮а•За§Х ুৌ৙-৮ৌ৙ а§Фа§∞ а§Ча§£а§®а§Ња§Па§В а§єа•Ба§Иа§В, ১৐ а§Єа§Ча§∞ুৌ৕ৌ ৃৌ৮а•А а§П৵а§∞а•За§Єа•На§Я а§Ъа•Ла§Яа•А а§К৙а§∞ ৮ড়а§Ха§≤а•А, а§Ха§Ва§Ъ৮а§Ьа§Ва§Ша§Њ ১а•Аа§Єа§∞а•З ৮а§Ва§ђа§∞ ৙а§∞ ৆৺а§∞а•Аа•§)
а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓ а§Ьа•На§ѓа•Ла§В-а§Ьа•На§ѓа•Ла§В а§Жа§Ча•З а§ђа•Э১а•А а§єа•И, а§∞а§Ња§ѓ а§За§≤а§Ња§Ха•З а§Ха•А ৵৮৪а•Н৙১ড়ৃа•Ла§В а§Ха•З а§Ха§∞а•Аа§ђ а§Ьৌ১а•З а§єа•Иа§В, а§Ша§Ња§Є а§Фа§∞ а§ђа§Ња§Ва§Є ৶ড়а§Цৌ১а•З а§єа•Ба§П ১а•Аа§Єа•Н১ৌ ৮৶а•А а§Ха•З а§За§∞а•Н৶-а§Ча§ња§∞а•Н৶ а§Ха•А а§Ж৐ৌ৶а•А ৐১ৌ১а•З а§єа•Иа§В а§Фа§∞ а§К৙а§∞ а§Ха•А а§Уа§∞ а§Ьৌ১а•З а§єа•Иа§Ва•§ ৙а§Ча§°а§Ва§°а§ња§ѓа§Ња§Ва•§ а§Ьа§Ва§Ча§≤а•§ а§Ха•Ла§єа§∞а•З а§Ѓа•За§В а§Єа§єа§Ѓа•З ৙а•За•Ьа•§ ১а§∞а§є-১а§∞а§є а§Ха•З а§Ьа§Ва§Ча§≤а•А а§Ђа§≤а•§ а§Эа§Ња•Ьа§ња§ѓа§Ња§Ва•§ ৥а§≤৵ৌа§В а§Ца•За§§а•§ а§Ха§ња§Єа§Ња§®а•§ а§Ча§Ња§Ва§µа•§ а§≤а•Ла§Ча•§ а§ђа§Ъа•На§Ъа•З а§Фа§∞ а§Фа§∞১а•За§Ва•§ ৙৮а§Ъа§Ха•На§Ха•Аа•§ а§≤а§Ха•Ьа•А а§Ха•З а§Ша§∞а•§ а§Й৮а§Ха•З а§Ха§≤а§Ња§∞а•Ва§™а•§ а§Єа§ђ а§ђа•З৺৶ а§Ха§∞а•Аа§ђ а§Єа•За•§ ৙а•Аа§Ыа•З а§За§Х১ৌа§∞а•З а§Ьа•Иа§Єа§Њ а§Ха•Ла§И ৙৺ৌа•Ьа•А ৵ৌ৶а•На§ѓ а§ђа§Ь১ৌ а§Ъа§≤১ৌ а§єа•Иа•§
а§Ђа§ња§∞ ৮а•Аа§Ъа•З а§Й১а§∞ а§Ж১а•З а§єа•Иа§Ва•§ а§Ьৌ১а•Аа§ѓ а§Фа§∞ а§Єа§Ња§Ва§Єа•На§Ха•Г১ড়а§Х ৵ড়৵ড়৲১ৌ а§Ха§Њ а§ђа•На§ѓа•Ла§∞а§Ња•§ ৮ৌুа•На§Ъа•А а§Ха§Њ а§ђа§Ња§Ьа§Ља§Ња§∞а•§ а§∞৵ড়৵ৌа§∞ а§Ха•А а§Єа•Ба§ђа§є а§Ча§Ва§Ча§Яа•Ла§Х а§Ха§Њ а§≤а§Ња§≤ а§ђа§Ња§Ьа§Ља§Ња§∞а•§ ৴а•На§∞а§Ѓа§∞১ а§≤а•Ла§Ча•§ а§ђа•Б৮а§Ха§∞а•§ ৺ৌ৕а§Ха§∞а§Ша§Ња•§ а§≤а•Ба§єа§Ња§∞а•§ а§Ша•Ла•Ьа•З а§Ха•Л а§Ха§Ња§ђа•В а§Ха§∞১ৌ а§ѓа•Б৵а§Ха•§ а§Єа•Ьа§Х ৙а§∞ а§єа§Ња§Я а§Єа§Ьа§Ња§П а§Єа•Н১а•На§∞а§ња§ѓа§Ња§Ва•§ ৙ৌа§∞а§В৙а§∞а§ња§Х ৙а•Л৴ৌа§Ха•§ а§Ч৺৮а•За•§ а§З৮ а§Єа§ђа§Ха•З а§К৙а§∞ а§Й৮а§Ха•А а§Ъа§ња§∞-а§Ѓа•Ба§Єа§Ха§Ња§®а•§ а§Ха•Иа§Ѓа§∞а§Њ а§Ъа•За§єа§∞а§Њ-৶а§∞-а§Ъа•За§єа§∞а§Њ а§°а•Ла§≤১ৌ а§єа•Иа•§ ৕а•Ла•Ьа§Њ а§Ха§Ња§ђа•В, ৕а•Ла•Ьа§Њ а§Єа•Н৵а§Ъа•На§Ыа§Ва§¶а•§ а§Ха•Иа§Ѓа§∞а§Ња§Ѓа•И৮ а§Єа•Ла§Ѓа•За§В৶а•Б а§∞а•Йа§ѓ-а§Єа•Ба§ђа•На§∞১ а§∞а§Ња§ѓ а§Ха•З ৐ৌ৶ а§Ьа•Л а§∞а§Ња§ѓ а§Ха•З ৙а•На§∞а§ња§ѓ а§Ы৵ড়а§Ха§Ња§∞ а§∞а§єа•З, а§Ха•Л а§Ха§ња§Єа•А ৙а•А৆ ৙а§∞ а§ђа§Ъа•На§Ъа§Њ ৶ড়а§Ц а§Ьৌ১ৌ а§єа•Иа•§ а§Ха•Иа§Ѓа§∞а§Њ а§Єа§ђ а§Ыа•Ла•Ьа§Ха§∞ а§Йа§Єа§Ха•З ৙а•Аа§Ыа•З а§Ъа§≤১ৌ а§єа•И, а§Ѓа•Ба•Ь-а§Ѓа•Ба•Ь а§Ха§∞ а§Ха•Иа§Ѓа§∞а•З а§Ха•Л ৮ড়৺ৌа§∞১ৌ а§ђа§Ъа•На§Ъа§Њ ৕а§Х а§Ьৌ১ৌ а§єа•И, ৙а§∞ а§Ха•Иа§Ѓа§∞а§Њ ৮৺а•Аа§Ва•§
ৃৌ৮а•А а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓ, а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓ а§єа•Иа•§ а§∞а§Ња§Ьа§Њ-а§∞ৌ৮а•А а§Ха•А а§Х৺ৌ৮а•А а§єа•Ла§Ча•А а§Е৙৮а•А а§Ьа§Ча§єа•§ а§ђа•Ьа§Њ а§Ха§≤а§Ња§Ха§Ња§∞ а§Еа§Ха§Ња§≤ а§Фа§∞ а§Ѓа§єа§Ња§Ѓа§Ња§∞а•А а§Ѓа•За§В а§≠а•А а§Ьа•А৵৮ ৥а•Ва§Ва•Э а§≤а•За§Ча§Ња•§ ৪১а•На§ѓа§Ьড়১ а§∞а§Ња§ѓ а§Єа§ња§Ха•На§Ха§ња§Ѓ а§Ха•А а§Жа§ђа•Л৺৵ৌ, а§∞а§Ва§Ча•Ла§В а§Фа§∞ а§Іа•Н৵৮ড়ৃа•Ла§В а§Ха•З ৪ৌ৕ а§Ь৮-а§Ьа•А৵৮ а§Ха•Л а§Ьа§ња§Є ১а§∞а§є а§єа§Ѓа§Ња§∞а•З а§Ха§∞а•Аа§ђ а§≤ৌ১а•З а§єа•Иа§В, а§ѓа§Ха•А৮ ুৌ৮ড়а§П! а§Ха§ња§Єа•А а§≠а•А а§Ха§ња§Єа•На§Ѓ а§Ха§Њ а§ђа•М৶а•На§Іа§ња§Х а§∞а§Ва§Ь ৶а•За§∞ ১а§Х а§Яа§ња§Ха§Њ ৮৺а•Аа§В а§∞а§є а§Єа§Ха§§а§Ња•§ ৮ а§ђа§Ња§ђа§Њ а§∞а§Ња§ѓ а§Ха§Њ а§Е৙৮ৌ, ৮ ৶а§∞а•Н৴а§Х а§Ѓа§Ња§И-৐ৌ৙ а§Ха§Ња•§
৙а§∞ а§Єа§∞а§Ха§Ња§∞ а§Ха§Њ а§∞а§Ва§Ь ৴ৌৃ৶ а§Ха§≠а•А а§Ц১а•На§Ѓ ৮ а§єа•Л১ৌ, а§Еа§Ча§∞ а§ѓа§є ৵а•Г১а•Н১а§Ъড়১а•На§∞ ৪১а•На§ѓа§Ьড়১ а§∞а§Ња§ѓ а§Ьа•Иа§Єа•А а§єа§Єа•Н১а•А а§Ха§Њ ৐৮ৌৃৌ а§єа•Ба§Ж ৮ а§єа•Ла§§а§Ња•§ ৵ড়৶а•З৴ а§Ѓа§В১а•На§∞а§Ња§≤а§ѓ а§Ха•З а§ђа§Ња§ђа•В вАШ৙৕а•За§∞ ৙ৌа§Ва§Ъа§Ња§≤а•АвАЩ а§Ха•Л ৵ড়৶а•З৴ а§Ьৌ৮а•З а§Єа•З а§∞а•Ла§Х а§∞а§єа•З ৕а•З, ১а•Л ৮а•За§єа§∞а•В ৮а•З а§Ыа•Ба•Ьа§Ња§ѓа§Ња•§ а§Єа§ња§Ха•На§Ха§ња§Ѓ а§Ха•З ৵ড়а§≤а§ѓ а§Ха•З ৐ৌ৶ ৶а•З৴ а§Ѓа•За§В а§За§Ѓа§∞а§Ьа•За§Ва§Єа•А а§≤а§Ња§Ча•В а§єа•Л а§Ча§И ৕а•Аа•§ ৴ৌৃ৶ а§Йа§Єа•А ৶а•Ма§∞ а§Ѓа•За§В вАШа§Єа§ња§Ха•На§Ха§ња§ЃвАЩ а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓ ৙а§∞ ৙а•На§∞১ড়৐а§Ва§І а§≤а§Ња§Ча•В а§єа•Ба§Жа•§
а§Ьа•Иа§Єа§Њ а§Ха§њ а§∞а§Ња§ѓ ৮а•З а§Ха§єа§Њ, ৙а•На§∞১ড়৐а§Ва§І а§Ха§Њ а§Ха•Ла§И а§Фа§Ъড়১а•На§ѓ ৮ ৕ৌ, а§Ха•На§ѓа•Ла§Ва§Ха§њ а§Йа§Є ৶а•Ма§∞ а§Ѓа•За§В ৵৺а•А ৵ৌ৪а•Н১৵ড়а§Х১ৌ ৕а•Аа•§ ৴ৌৃ৶ а§Єа§∞а§Ха§Ња§∞ а§Ѓа•За§В а§Ха§ња§Єа•А а§ђа•Ьа•З а§ђа§Ња§ђа•В ৮а•З а§Хৌ৮ а§≠а§∞а•З а§єа•Ла§Ва§Ча•З а§Ха§њ а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓ а§Ѓа•За§В а§Єа•Н৵১а§В১а•На§∞ а§∞а§Ња§Ьৌ৴ৌ৺а•А а§єа•И, ১ড়৐а•Н৐১а•А ৴а•На§∞৶а•На§Іа§Ња§≤а•Б а§єа•Иа§В, а§Ха§∞ুৌ৙ৌ, а§Й৮а§Ха§Њ ু৆, а§Ѓа§Ва§°а§∞ৌ১а•З а§≠а§Ња§∞১а•Аа§ѓ а§Єа•И৮ড়а§Х а§Фа§∞ а§Еа§Іа§ња§Ха§Ња§∞а•А а§єа•Иа§В а§Фа§∞ а§≤а•Ла§Ч а§ђа§єа•Б১ а§Ца§Ља•Б৴ ৮а§Ьа§Ља§∞ а§Ж১а•З а§єа•Иа§В, а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓ ৶а•За§Ц а§≤а•А ১а•Л а§Ъа•А৮ а§Єа§ња§Ха•На§Ха§ња§Ѓ а§Ха•Л а§Ха§≠а•А ুৌ৮а•Нৃ১ৌ ৮৺а•Аа§В ৶а•За§Ча§Ња•§
а§Ъа•А৮ ৮а•З а§Єа§ња§Ха•На§Ха§ња§Ѓ а§Ха•А ুৌ৮а•Нৃ১ৌ ৵а•Иа§Єа•З а§≠а•А а§Яа§Ња§≤а•З а§∞а§Ца•Аа•§ а§Ха•Ла§И ১а•Аа§Є а§Єа§Ња§≤а•§ 2003 а§Ѓа•За§В а§Эа•Ба§Ха§Њ, ১৐, а§Ьа§ђ а§≠а§Ња§∞১ ৮а•З а§Ъа•А৮ а§Ха•З а§Ха§ђа•На§Ьа•З ৵ৌа§≤а•З ১ড়৐а•Н৐১ ৙а•На§∞৶а•З৴ а§Ха•Л а§Ъа•А৮ а§Ха§Њ а§єа§ња§Єа•На§Єа§Њ ুৌ৮ а§≤а§ња§ѓа§Њ а§Фа§∞ а§За§Є а§Эа•Ба§Ха§Њ-а§Эа•Ба§Ха•А а§Ха•З ৪ৌ১ а§Єа§Ња§≤ ৐ৌ৶ ৵а•Г১а•Н১а§Ъড়১а•На§∞ вАШа§Єа§ња§Ха•На§Ха§ња§ЃвАЩ а§Ха•Л ৵ড়৶а•З৴ а§Ѓа§В১а•На§∞а§Ња§≤а§ѓ ৮а•З а§≠а§Ња§∞১ а§Ха•А а§Ь৮১ৌ а§Ха•З а§≤а§ња§П а§Жа§Ь৊ৌ৶ а§Ха§ња§ѓа§Ња•§ а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓ ৐৮৮а•З а§Ха•З ৙а•Ва§∞а•З а§Ъа§Ња§≤а•Аа§Є а§Єа§Ња§≤ ৐ৌ৶, ৴ৌৃ৶ а§ѓа§є а§Єа•Ла§Ъа§Ха§∞ а§Ха§њ ৙а•Б৮а§∞а•Б৶а•На§Іа§Ња§∞ а§Ха•З ৐ৌ৶ а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓ а§Еа§Ча§∞ ৵ড়৶а•З৴ а§Ѓа•За§В а§ђа§ња§Х৮а•З а§≤а§Ча•А ১а•Л а§Жа§Ь а§Ха•З ৶а•Ма§∞ а§Ѓа•За§В а§Йа§Єа•З а§ѓа§єа§Ња§В ৙৺а•Ба§Ва§Ъ৮а•З а§Ѓа•За§В а§Хড়১৮а•А ৶а•За§∞ а§≤а§Ча•За§Ча•А? ৙а§∞ а§ђа§Ња§ђа•В а§≤а•Ла§Ч а§Ра§Єа•З а§єа•А а§Єа•Ла§Ъ১а•З а§єа•Иа§Ва•§ а§Й৮а§Ха•З ৙ৌ৪ а§Е৙৮а•А а§Еа§Ха•На§≤ а§єа•И а§Фа§∞ а§Еа§Ха•На§≤ а§≤а§Ња§≤ а§ђа§Ња§Ьа§Ља§Ња§∞ а§Ѓа•За§В ১а•Л ৮৺а•Аа§В а§ђа§ња§Х১а•А? а§Ь৮৪১а•Н১ৌ а§Єа•З а§Єа§Ња§≠а§Ња§∞а•§

 а§Ѓа§Іа•На§ѓ ৙а•На§∞৶а•З৴
а§Ѓа§Іа•На§ѓ ৙а•На§∞৶а•З৴ 





















