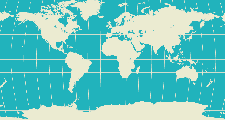लेकिन 'बतरस' का मजा ही कुछ और है…!
Saturday 15 February 2014 05:37:24 PM

हृदयनारायण दीक्षित
सभी रस प्राय: आनंददाता होते हैं, लेकिन 'बतरस' का मजा ही कुछ और है। सो 'संवाद' से मन नहीं भरता। हम सब जीवन का अधिकांश भाग संवाद में लगाते हैं। भाषण और लेखन भी संवाद हैं। भाषण में श्रोता सामने होते हैं। इसलिए संबोधन में हावभाव का भी आदान प्रदान होता है। श्रोता की संलिप्तता या उदासीनता साफ समझी जाती है। लेखन में पाठक सामने नहीं होते। इसलिए हावभाव का काम भी लिखे शब्दों ही लेना पड़ता है। लेखक अपने वाक्यों को संशोधित भी कर सकते हैं। भाषण में संशोधन की गुंजाइश नहीं होती। कहावत है-कि बोली और गोली वापस नहीं होती, इसलिए सोच समझकर बोलना चाहिए, लेकिन बतरस का अपना मजा है और अपनी उपयोगिता भी। भाषा संवाद का मुख्य उपकरण है। दुनिया में अनेक भाषाएं हैं। मनुष्य भाषा से संवाद का मजा लेते हैं। जान पड़ता है कि पशु पक्षी भी अपनी भाषा में बतियाते हैं। तुलसीदास ने 'खग जाने खग की ही भाखा लिखा है। 'भाखा' यहां भाषा है। मनुष्य भी मनुष्येतर प्राणियों से बतियाते हैं। कुत्ता ज्यादा संवेदनशील है, वह भाव भाषा पकड़ने का विशेषज्ञ है। तोता वैसा संवेदनशील नहीं है, लेकिन शब्द याद करने में वैसी दूसरी प्रजाति नहीं। वह रट्टू है, लेकिन कुत्ता समझदार। बातें तो पौधे भी करते होंगे। सतत् अभिव्यक्ति ही प्रकृति का मुख्य गुण है। स्वयं को लगातार व्यक्त करना इसका स्वभाव है। अंतस् को व्यक्त करने का ही एक कृत्य है संवाद।
वैदिक ऋषि संवाद प्रवीण थे। उन्होंने मनुष्यों के साथ ही कीट, पतिंग और वनस्पतियों से भी बातें की। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में अथर्वा ने पृथ्वी से संवाद बनाया है। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और नदियों के बीच संवाद है। सरस और भाव प्रवणता का ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। इस संवाद में नदियों ने भी विश्वामित्र से बातें की है। ऋग्वेद में व्यापारियों और एक कुतिया सरमा के बीच भी रोचक संवाद है। वैदिक परंपरा में अनेक देवता हैं। देवता प्रकृति की शक्तियां हैं। कुछ प्रत्यक्ष हैं, कुछ प्रत्यक्ष नहीं, लेकिन अनुभूति से देखी गई है। सूर्य प्रत्यक्ष है, अग्नि, जल, वनस्पति भी प्रत्यक्ष है। इंद्र इतिहास नहीं जान पड़ते, वे अनुभूतिपरक होंगे। प्रत्यक्ष से संवाद बनाने का उपकरण भाषा है। भाषा के साथ भाव प्रकट करते हुए शरीर को हिला डुलाकर हम कुत्तों, पक्षियों आदि से बातें करते हैं, लेकिन ऋषियों के सामने मूलभूत प्रश्न रहा होगा कि अदृश्य से संवाद की भाषा क्या हो? ज्ञात से संवाद के उपकरण घटाए या बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन अज्ञात से संवाद की भाषा क्या हो? शैली क्या हो? हावभाव का संयोजन क्या हो? वैदिक ऋषियों ने इसके लिए भी संस्कृत-छंदस् का ही सुंदर उपयोग किया है। ऋषि अनेक देवों की स्तुतियां करते हैं। वे इसी भाषा का प्रयोग करते हैं।
कह सकते हैं कि अपनी भाषा को ही माध्यम बनाने के अलावा और कोई उपाय भी नहीं होता, लेकिन इसके विपरीत दूसरा तर्क भारी प्रतीत होता है। हम अंग्रेजी विद्वान से संवाद के लिए अंग्रेजी को सुविधाजनक पाते हैं। अंग्रेज यहां सत्ताधीश थे। अंग्रेजी सत्ता की भाषा थी। कोर्ट कचहरी में अंग्रेजी थी आज भी है। हम स्वयं से श्रेष्ठ से वार्ता में प्राय उसी की भाषा में बात करना ठीक मानते हैं। वैदिक ऋषियों के मन में भी यह बात अवश्य रही होगी। आखिर दिव्य शक्तियां या देवों को कौन भाषा प्रिय रही होगी? क्या वे भी भाषा के बंधन में रहे होंगे? या दुनिया की सभी भाषाओं के जानकार रहे होंगे? आस्थावश ऐसा मान भी सकते हैं। आस्थालु देवों को भाषा में नहीं बांधते, लेकिन प्रश्न बड़ा है। भारत में संस्कृत ही प्रार्थना की भाषा है। विवाह और अन्य संस्कारों की भी। इसी तरह मुस्लिम मित्रों के यहां संस्कार आदि की भाषा अरबी है। रोमन कैथोलिक में लैटिन है। यहूदियों में हिबू्र है। आर्थोडाक्स ईसाई ग्रीक का प्रयोग करते हैं। भिन्न भिन्न सभ्यताओं में प्रार्थना और संस्कार की भाषाएं भिन्न भिन्न हैं।
हरेक भाषा के संस्कार भी होते हैं। ऋग्वेद दुनिया का प्राचीनतम शब्द प्रमाण है। वैदिक भाषा भी प्राचीनतम है। वैदिक भाषा के भी अपने संस्कार हैं। वैदिक समाज ने इसी भाषा को संवाद का माध्यम बनाया था। उन्होंने इसी भाषा माध्यम को समाज गठन का उपकरण भी बनाया। इसी भाषा से दैनिक जीवन के कामकाज भी किए और इसी भाषा के माध्यम से सूर्य, चंद्र, नदी, पर्वत और वनस्पति आदि से भी संवाद बनाया। यज्ञ कर्मकांड में भी इसी भाषा का प्रयोग हुआ। कर्मकांड के एक मजेदार मंत्र में कहते हैं यह स्वाहा अंतरिक्ष तक पहुंचे, यह समुद्र को और यह स्वाहा वनस्पतियों औषधियों तक पहुंचे।'' ऋषियों ने इसी भाषा में देव स्तुतियां भी कीं। यहां कई भौतिकवादी प्रश्न उठते हैं-क्या देवता होते हैं? क्या वे हमारी स्तुतियां सुनते हैं? सुनते भी हैं तो क्या भाषा विशेष को ही महत्व देते हैं? वैदिक ऋषियों ने प्रकृति की शक्तियों को देवता कहा है। प्रकृति प्रत्यक्ष है, इसकी शक्तियां भी प्रत्यक्ष हैं। स्तुतियां हमारा मनोभाव हैं। प्रार्थना और स्तुति में भाव की महत्ता है। प्रार्थना चित्त को प्रसन्न करती है। निराशी होने से बचाती है। स्तुतियां आनंदवर्द्धन होती ही हैं। आस्तिक समाज प्रार्थना को महत्व देते हैं। इसलिए प्रार्थना के साथ इसकी भाषा भी महत्वपूर्ण है।
भाव अंत: स्थल है। भावजगत् में पदार्थ नहीं होते, इसलिए रूप आकार भी नहीं होते। भाव को भाषा में प्रकट करना आसान नहीं होता। रूप या आकार के नाम होते हैं। नाम सुनते या पढ़ते ही रूप या आकार प्रकट हो जाता है। रूप नाम सार्वजनीन बोध है, लेकिन भाव परिपूर्ण सार्वजनीन बोध नहीं होते। प्रीति भाव है। प्रीति शब्द सुनते या पढ़ते हुए हरेक के चित्त में एक जैसी समझ नहीं बनती। ग्लानि, ईर्ष्या, लज्जा, भय आदि भी ऐसे ही शब्द हैं। इन शब्दों के अर्थ परिपूर्ण सार्वजनीन नहीं हैं। इन शब्दों के अर्थ हरेक व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न हैं। यहां भाषा की सीमा है। उद्धव गोपियों के पास गए थे-श्रीकृष्ण का संदेश लेकर। गोपियां प्रेम विह्वल थीं। इस पर जगन्नाथ दास रत्नाकर की कविता है-नेकु कही बैननि सों/अनेकु कही नैननि सों/ रही सही सोऊ कहि दीनी हिचकीन सों।'' यहां भाषा से पूरा प्रेम प्रकट नहीं हो पाया-थोड़ा कुछ बातों से, ज्यादा कुछ आंखों से और शेष हिचकियों से प्रकट हुआ। परिपूर्ण भाव अभिव्यक्ति के मामले में भाषा की सीमा है, लेकिन संस्कृत में इस सीमा के अतिक्रण के प्रयास आश्चर्यचकित करने वाले हैं। संस्कृत विद्वानों ने विराट और असीम से भी संवाद करने का काम किया है।
विचार का रूप आकार नहीं होता। भारतीय दर्शन में रूप का अनेकश: अतिक्रमण हुआ है। ऋषि स्वयं रूप गढ़ते हैं। देवों का रूप विधान गाते हैं फिर उन्हें व्यापक करते हुए विराट तक ले जाते हैं रूप की सत्ता मिट जाती है। विराट जैसा शब्द संस्कृत में हो सकता है। विराट का आयतन नहीं हो सकता। विराट असीम है। वस्तु का रूप होता है और रूप का आयतन। आयतन होगा तभी रूप होगा। ऋग्वेद का 'पुरूष' संपूर्ण जगत् आच्छादित करता है फिर भी वह शेष बचता है। अभिव्यक्ति की ऐसी शक्ति संस्कृत में ही दिखाई पड़ती है। दुनिया की अन्य भाषाएं प्रत्यक्ष जगत् को ही बोली और शब्द दे सकती हैं। वे दार्शनिक अनुभूति और गहन प्रतीति को व्यक्त नहीं कर सकतीं। संस्कृत अप्रत्यक्ष और अव्यक्त जगत् को भी प्रत्यक्ष करने की क्षमता से लैस है। विश्वविख्यात् मनोवैज्ञानिक युंग ने ठीक कहा था कि पूरब (भारत) ने विचारों को वैसे ही देखा है, जैसे पश्चिम ने वस्तुओं और पदार्थो को। संस्कृत इसीलिए लोकभाषा के साथ देवभाषा भी कही गई।

 मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश