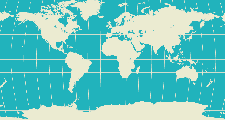
а§∞ৌু৙а•Н৙ৌ а§Фа§∞ а§єа§Ьа§Ља§Ња§∞ а§Єа•Н১а§Ва§≠а•Ла§В ৵ৌа§≤а§Њ ৶а•З৵ৌа§≤а§ѓ
а§∞а§Ѓа•З৴а§Ъа§В৶а•На§∞ ৴ৌ৺
Tuesday 05 February 2013 07:06:04 AM

ু৮а•Ба§Ја•На§ѓ а§Па§Х а§Єа§Ња§Ѓа§Ња§Ьа§ња§Х ৙а•На§∞а§Ња§£а•А а§єа•И, ু৮а•Ба§Ја•На§ѓ а§Па§Х а§Жа§∞а•Н৕ড়а§Х а§Фа§∞ а§∞а§Ња§Ь৮а•А১ড়а§Х ৙а•На§∞а§Ња§£а•А а§≠а•А а§єа•И, а§≤а•За§Хড়৮ а§За§Єа§Ха•З ৪ৌ৕ а§єа•А ৪ৌ৕ а§За§Єа§Єа•З а§ђа§єа•Б১ ৙৺а§≤а•З а§Єа•З ৵৺ а§Па§Х ৶а•З৵৙а•Ва§Ьа§Х ৙а•На§∞а§Ња§£а•А а§≠а•А а§єа•Иа•§ а§єа§Ѓа§Ња§∞а•А ু৮а•Ба§Ја•Нৃ১ৌ а§Ха§Њ а§єа•А а§Е৮ড়৵ৌа§∞а•На§ѓ а§Еа§Ва§Ч а§єа•И-а§єа§Ѓа§Ња§∞а•А а§Іа§∞а•На§Ѓ а§≠ৌ৵৮ৌ а§ѓа§Њ а§Іа§Ња§∞а•На§Ѓа§ња§Х а§Єа§В৵а•З৶৮ৌ а§Фа§∞ а§Йа§Єа•А ু৮а•Ба§Ја•Нৃ১ৌ а§Ха§Њ а§Й১৮ৌ а§єа•А а§Еа§≠ড়৮а•Н৮ а§Фа§∞ а§Е৮ড়а§∞а•Н৵ৌৃ а§Еа§Ва§Ч а§Ха§Њ а§Жа§ѓа§Ња§Ѓ а§єа•И-а§єа§Ѓа§Ња§∞а•А а§Єа•Ма§В৶а§∞а•На§ѓ а§Ъа•З১৮ৌ а§ѓа§Њ а§Ха§≤ৌ১а•На§Ѓа§Х а§Єа§В৵а•За§¶а§®а§Ња•§ ৶а•Л৮а•Ла§В а§Ха§Њ а§Ѓа•За§≤ а§Фа§∞ а§Ч৆৐а§В৲৮ ৙а•На§∞а§Ча§Я а§єа•Л১ৌ а§єа•И, а§єа§Ѓа§Ња§∞а•З а§З৮ ৶а•З৵а•А-৶а•З৵১ৌа§Уа§В а§Ѓа•За§В, а§Ьа•Л а§єа§Ѓа§Ња§∞а•А ুৌ৮৵а•А ৙а•На§∞а§Ха•Г১ড় а§Ѓа§Ња§Ва§Ч а§Ха•А а§єа•А ৙а•Ва§∞а•Н১ড় а§Ха§∞৮а•З а§Ха•Л а§Е৵১а§∞ড়১ а§єа•Л১а•З вАМа§єа•Иа§В а§єа§Ѓа§Ња§∞а•А а§Ъа•З১৮ৌ а§Ѓа•За§В а§Фа§∞ а§Ђа§ња§∞ а§Ѓа•Ва§∞а•Н১ а§∞а•В৙ а§≤а•З১а•З а§єа•Иа§В, а§єа§Ѓа§Ња§∞а•А а§єа•А а§Ьа•На§Юৌ৮а•За§В৶а•На§∞а§ња§ѓа•Ла§В-а§Ха§∞а•На§Ѓа•За§В৶а•На§∞а§ња§ѓа•Ла§В ৃৌ৮а•А, а§єа§Ѓа§Ња§∞а•А а§єа•А а§Жа§Ва§Ца•Ла§В а§Фа§∞ ৺ৌ৕а•Ла§В-а§Ха•З а§Ьа§∞а§ња§П а§За§Єа•А а§Ѓа§ња§Яа•На§Яа•А, а§™а§Ња§Ја§Ња§£ а§Фа§∞ ৲ৌ১а•Б а§Ха•А а§Ц৮ড়а§Ь а§Єа§В৙৶ৌ а§Ѓа•За§В а§Ьа•Л а§єа§Ѓа§Ња§∞а•А а§єа•А ১а§∞а§є а§Фа§∞ а§єа§Ѓа§Єа•З а§≠а•А ৙৺а§≤а•З ৙а•На§∞а§Ха•Г১ড় а§Ха•З а§Ча§∞а•На§≠ а§Єа•З а§Й৙а§Ьа•За•§ а§ѓа§є а§Е৮а•В৆ৌ а§Єа•НвАН৕ৌ৙১а•На§ѓ, а§ѓа•З а§Єа•Н১а§Ва§≠ а§Фа§∞ а§Й৮ ৙а§∞ а§Йа§Ха•За§∞а•А а§Ча§Иа§В а§ѓа•З а§Еа§Єа§Ва§Ца•На§ѓ а§Ѓа•Ва§∞а•Н১ড়-৴ড়а§≤а•Н৙а§Ха•Г১ড়ৃৌа§В а§Ъа•З১৮ৌ а§Ха§Њ а§Ъа•З১৮ৌ а§Єа•З ৮ড়а§∞а§В১а§∞ а§Єа§В৵ৌ৶ ৮৺а•Аа§В ১а•Л а§Фа§∞ а§Ха•На§ѓа§Њ а§єа•И? а§Па§Х ৙а•На§∞а§Ча§Я а§Фа§∞ а§Ьа§Ња§Ча•А а§єа•Ба§И а§Ъа•З১৮ৌ а§Ха§Њ а§Па§Х а§Е৙а•На§∞а§Ха§Я а§Фа§∞ а§Єа•Ла§И а§Ъа•З১৮ৌ а§Ха•Л а§єа•А а§Ьа§Чৌ৮а•З а§Ха§Њ а§Й৙а§Ха•На§∞а§Ѓа•§
а§ѓа§є ৐ৌ১ а§За§Є ১а§∞а§є, а§З১৮а•З а§Єа§Ња§Ђ ১а•Ма§∞ ৙а§∞ а§ѓа§єа•Аа§В а§За§Єа•А а§Ьа§Ча§є а§Ха•На§ѓа•Ла§В а§Ѓа•За§∞а•З а§Єа§ња§∞ ৙а§∞ а§Ъ৥৊а§Ха•З а§ђа•Ла§≤ а§∞а§єа•А а§єа•И, а§За§Єа•А а§∞ৌু৙а•Н৙ৌ а§Ѓа§В৶ড়а§∞ а§Ха•З ৪ৌু৮а•З, а§Ьа§ња§Єа§Ха§Њ ৮ৌু ১а§Х ৮৺а•Аа§В а§Єа•Б৮ৌ ৕ৌ а§Ѓа•И৮а•З, а§ѓа§єа§Ња§В а§Ж৮а•З а§Єа•З ৙৺а§≤а•За•§ а§Єа§Ва§Ьа•Ла§Ч-а§Па§Х ৮ড়а§∞а§Њ а§Єа§Ва§Ьа•Ла§Ч-а§єа•А ৮ а§Ха§єа•За§Ва§Ча•З а§За§Єа•З, а§Ха§њ а§Ѓа•За§∞а•З ৙৕ ৶а§∞а•Н৴а§Х а§Фа§∞ ৪৺ৃৌ১а•На§∞а•А ৴а•На§∞а•А৙১ড় а§Ха•Л а§Еа§Ъৌ৮а§Х а§Єа•Ва§Эа§Њ а§Ха§њ а§Ха•На§ѓа•Ла§В ৮ а§З৮а•На§єа•За§В а§≤а§Ча•З ৺ৌ৕ ৵৺ а§Ѓа§В৶ড়а§∞ а§≠а•А ৶ড়а§Ца§≤а§Њ ৶а•За§В-৵а§∞а§Ва§Ча§≤ а§Ха•З а§Е৙а•За§Ха•На§Ја§Ња§Ха•Г১ а§Єа•Б৵ড়а§Ца•Нৃৌ১ а§Єа§єа§Єа•НвАН১а•На§∞ а§Єа•Н১а§Ва§≠ ৶а•З৵ৌа§≤а§ѓ а§Ха•З ৪ৌ৕-৪ৌ৕, а§Ьа•Л а§єа•И ১а•Л а§Ха§Ња§Ђа•А ৶а•Ва§∞ а§Фа§∞ а§Еа§≤а§Ч-৕а§≤а§Ч, а§≤а•За§Хড়৮ а§За§Є ুৌ৮а•З а§Ѓа•За§В а§За§Ха§≤а•М১ৌ а§Фа§∞ ৵ড়а§≤а§Ха•На§Ја§£ а§Ха§њ а§За§Єа§Ха§Њ ৮ৌু а§За§Єа•З ৐৮ৌ৮а•З ৵ৌа§≤а•З ৙а•На§∞а§Ѓа•Ба§Ц ৴ড়а§≤а•Н৙а•А а§Ха•З ৮ৌু ৙а§∞ ৙ৰ৊ৌ а§єа•И ৮ а§Ха§њ ৶а•З৵ৌа§≤а§ѓ а§Ѓа•За§В ৙а•На§∞১ড়ৣа•Н৆ড়১ ৶а•З৵ৌ৲ড়৶а•З৵ ৴ড়৵ ৙а§∞а•§ ৴а•На§∞а•А৙১ড় ৆а•Аа§Х ৪৵ৌ а§Ыа§є а§ђа§Ьа•З а§Єа•Ба§ђа§є а§Яа•Иа§Ха•На§Єа•А а§≤а•За§Ха§∞ а§єа§Ѓа§Ња§∞а•З ৵ড়а§Ьа§ња§Яа§ња§Ва§Ч а§Єа•На§Ха§Ња§≤а§∞а•На§Є а§≤а•За§Х-৵а•На§ѓа•В а§Ча•За§Єа•На§Я а§єа§Ња§Йа§Є ৙৺а•Ба§Ва§Ъ а§Ча§ѓа§Њ а§•а§Ња•§ ৪ৌ৥৊а•З ৪ৌ১ а§ђа§Ьа•З а§Єа§ња§Ха§В৶а§∞ৌ৐ৌ৶ а§Єа•З а§Ча•Ба§Ва§Яа•Ва§∞-а§Єа§ња§Ха§В৶а§∞ৌ৐ৌ৶ а§За§Ва§Яа§∞а§Єа§ња§Яа•А а§Па§Ха•Н৪৙а•На§∞а•За§Є ৙а§Ха§°а§Ља§Ха§∞ ১а•А৮ а§Ша§Ва§Яа•З ৐ৌ৶ а§Ха§Ња§Ьа•А৙а•За§Я ৙৺а•Ба§Ва§Ъа•За•§ а§Ѓа•И а§Єа§Ѓа§Эа§Њ ৕ৌ а§Ха§њ ৵а§∞а§Ва§Ча§≤ ৙৺а§≤а•З а§Ьа§Ња§Па§Ва§Ча•З, ১৐ ৵৺ৌа§В а§Єа•З а§∞ৌু৙а•Н৙ৌ а§Ѓа§В৶ড়а§∞а•§ а§Єа§∞৙а•На§∞а§Ња§За§Ь а§°а§ња§Єа•На§Х৵а§∞а•А ৕а•А, а§єа§Ѓа§Ња§∞а•З а§≤а§ња§П а§ѓа§є ৪১а•Н১а§∞ а§Ха§ња§≤а•Ла§Ѓа•Аа§Яа§∞ а§Ха•А а§Єа§∞৙а•На§∞а§Ња§За§Ь ৃৌ১а•На§∞а§Њ, а§За§Єа§≤а§ња§П а§Ха§њ ৴а•На§∞а•А৙১ড় ৮а•З а§Єа•Б৶а•Ва§∞ а§ђа§Ъ৙৮ а§Ѓа•За§В а§Ха§≠а•А ৶а•За§Ца•З а§За§Є а§Ѓа§В৶ড়а§∞ а§Ха•З а§∞а•Ла§Ѓа§Ња§Ва§Ъ а§Ха•Л а§єа§Ѓа§Ња§∞а•З а§≤а§ња§П а§єа•А ৮৺а•Аа§В, а§Єа•Н৵ৃа§В а§Е৙৮а•З а§≤а§ња§П а§≠а•А а§Ча•Л৙৮а•Аа§ѓ а§Фа§∞ а§Єа•Ба§∞а§Ха•Нৣড়১ ৐৮ৌа§Ха§∞ а§Єа§єа•За§Ь а§∞а§Ца§Њ а§•а§Ња•§ а§∞а§Ња§Єа•Н১ৌ ু৮а•Ла§∞а§Ѓ а§Фа§∞ а§Єа§Ѓа•Ва§Ъа§Њ а§≤а•Иа§Ва§°а§Єа•На§Ха•З৙ а§єа•А а§За§Є а§Х৶а§∞ ৙а§≤-৙а§≤ ৙а§∞ড়৵а§∞а•Н১ড়১ ৙а•На§∞а§Ха•Г১ড় ৵а•З৴ а§Єа•З а§Єа§В৙а§В৮ ৕ৌ а§Ха§њ ৪১а•Н১а§∞ а§Ха§ња§≤а•Ла§Ѓа•Аа§Яа§∞ а§Ха§Њ а§≠а§∞а•А-৶а•Л৙৺а§∞а•А а§Ха§Њ а§Єа§Ђа§∞ а§≠а•А а§єа§Ѓа§Ѓа•За§В а§Ха•На§≤а§Ња§В১ড় ৮৺а•Аа§В а§Й৙а§Ьа§Њ а§™а§Ња§ѓа§Ња•§
а§За§Є ১৕а•На§ѓ а§Ха•З ৐ৌ৵а§Ьа•В৶ а§Ха§њ а§Цৌ৮а•З-৙а•А৮а•З а§Ха•Л а§Ха§єа•Аа§В а§Ха•Ба§Ы а§Й৙а§≤а§ђа•НвАНа§І ৮৺а•Аа§В а§єа•Ба§Ж а§Фа§∞ ৙ৌ৕а•За§ѓ а§Ьа•Иа§Єа§Њ а§≠а•А а§єа§Ѓ а§Ха•Ба§Ы ৪ৌ৕ ৮৺а•Аа§В а§∞а§Ца•З ৕а•З, а§ѓа§є ুৌ৮а§Ха§∞ а§Ъа§≤৮а•З а§Ха•З а§Ха§Ња§∞а§£ а§Ха§њ а§∞ৌু৙а•Н৙ৌ а§Ѓа§В৶ড়а§∞ а§Ха•А а§ђа§Ња§∞а•А ১а•Л ৐ৌ৶ а§Ѓа•За§В а§Жа§Па§Ча•А, ৙৺а§≤а•З ১а•Л ৵а§∞а§Ва§Ча§≤ а§Ха•Л а§єа•А ৮ড়৐а§Яৌ৮ৌ а§єа•И а§Фа§∞ ৵а§∞а§Ва§Ча§≤ а§Ѓа•За§В а§≠а§≤а§Њ а§Ха§ња§Є а§Ъа•Аа§Ь а§Ха•А а§Ха§Ѓа•А а§єа•И, а§Ца§Њ-৙а•Аа§Ха§∞ а§єа•А а§Еа§Ча§≤а§Њ а§Еа§≠ড়ৃৌ৮ а§Жа§∞а§Ва§≠ а§Ха§∞а•За§Ва§Ча•За•§ а§Ха§Ѓа§Ња§≤ а§Ха•А ৐ৌ১ а§ѓа§є а§єа•И а§Ха§њ а§≠а•Ва§Ц а§Фа§∞ ৙а•На§ѓа§Ња§Є ৶а•Л৮а•Ла§В а§єа•А а§Е৙৮а•А ৮а•Иа§Єа§∞а•На§Ча§ња§Х а§Й১а•На§Ха•Га§Ја•На§Я১ৌ а§Ха•З ৪ৌ৕ а§Е৙৮а•А-а§Е৙৮а•А ৆а•Ма§∞ а§Єа•НвАН৕а§Чড়১ а§∞а§єа•За•§ а§ѓа•Ла§В а§Ха•На§ѓа§Њ-а§Ха•На§ѓа§Њ ৮৺а•Аа§В ৶а•За§Ца§Њ а§єа•И, а§З৮ а§Жа§Ва§Ца•Л ৮а•З, ৶а•За§Є-৐ড়৶а•За§Є, а§Єа§∞а•Н৵১а•На§∞-а§Па§≤а•Ла§∞а§Њ, а§Па§≤а•Аа§Ђа•За§Ва§Яа§Њ а§Ца§Ьа•Ба§∞а§Ња§єа•Л, а§Ха•Ла§£а§Ња§∞а•На§Х, ৐৶ৌুа•А а§Ха•З৵а•На§Ь, а§Єа§Ња§Ва§Ъа•А-৵ড়৶ড়৴ৌ, а§≠а•Ла§Ь৙а•Ба§∞-а§≠а•Аа§Ѓа§ђа•За§Яа§Ха§Њ, а§Ѓа§єа§Ња§ђа§≤а•А৙а•Ба§∞а§Ѓ а§Фа§∞ ৙а§∞৶а•За§Є а§Ѓа•За§В а§≠а•А, а§Па§Х а§Єа•З а§Па§Х а§Ха§Ња§Єа§≤ а§Фа§∞ а§Єа•На§Ѓа§Ња§∞а§Х, ১৐ а§Ђа§ња§∞ а§За§Є а§Єа•Б৶а•Ва§∞ а§Ха•Л৮а•З а§Ѓа•За§В а§Еа§≤а§Ха•Нৣড়১ а§Ъа•Б৙а§Ъৌ৙ ৙ৰ৊а•З а§За§Є а§Е৮ৌু-а§Еа§Ха§ња§Ва§Ъ৮ а§Єа•З а§Ѓа§В৶ড়а§∞ ৮а•З а§єа§Ѓа•За§В а§Ха•На§ѓа•Ла§В а§ђа•Ба§≤а§Ња§ѓа§Њ? а§Ха•Иа§Єа•З а§Фа§∞ а§Ха•На§ѓа•Ла§В а§єа§Ѓ а§Па§Х-৶а•Ва§Єа§∞а•З а§Ца§Ва§≠а•З а§Фа§∞ а§Йа§Є ৙а§∞ а§Йа§Ха•За§∞а•А а§єа•Ба§И а§Па§Х-а§Па§Х а§Ѓа•Ва§∞а•Н১ড়, а§Па§Х-а§Па§Х ৴ড়а§≤а•Н৙ а§Ха•Л ৮ড়৺ৌа§∞৮а•З а§Ѓа•За§В а§За§Є а§Х৶а§∞ ১а§≤а•На§≤а•А৮ а§єа•Иа§В а§Ха§њ а§≠а•Ва§Ц-৙а•На§ѓа§Ња§Є а§≠а•А а§≠а•Ба§≤а§Њ а§ђа•И৆а•З а§єа•Иа§В? а§Єа•Ма§В৶а§∞а•На§ѓ-а§Ха•Га§Ја•НвАНа§£а§Ѓа•Ва§∞а•Н১ড় а§Ха§Њ а§Х৺৮ৌ а§єа•И-а§Єа•Ма§В৶а§∞а•На§ѓ ৵৺ а§єа•И, а§Ьа•Л а§єа§Ѓа•За§В а§Ха•Ба§Ы а§Ха•На§Ја§£а•Ла§В а§Ха•З а§≤а§ња§П а§єа•А а§Єа§єа•А, а§Па§Х৶ু а§Ж১а•Нু৵ড়৪а•На§Ѓа•Г১ ৃৌ৮а•А ১৮а•На§Ѓа§ѓ а§Ха§∞ ৶а•З১ৌ а§єа•Иа•§ а§Єа•Ма§В৶а§∞а•На§ѓ а§Ха•А ৵৺ ৙а§∞а§ња§≠а§Ња§Ја§Њ а§≠а•А а§≠а§≤а§Њ а§Ха•На§ѓа•Ла§В а§Еа§≠а•А а§За§Єа•А а§Ша§°а§Ља•А ৃৌ৶ а§Ж а§∞а§єа•А а§єа•И?
а§За§Є а§Ѓа§В৶ড়а§∞ а§Ха•З а§Єа•Н১а§Ва§≠а•Ла§В ৙а§∞ ১а•Ла§∞а§£-৶а•Н৵ৌа§∞ ৙а§∞ а§Ьа•Л ৶а•Г৴а•На§ѓ а§Йа§Ха•За§∞а•З а§Ча§П а§єа•Иа§В, ৵а•З а§Ха•Ба§Ы ১а•Л а§Єа•Н৙ৣа•На§Я а§єа•А а§∞а§Ња§Ѓа§Ња§ѓа§£ а§Ха•З а§єа•Иа§В, а§Ьа•Л а§ђа§єа•Б১ ৙৺а§≤а•З ৙৥৊а•З а§єа•Ба§П ৴ড়৵ ৙а•Ба§∞а§Ња§£ а§Фа§∞ а§Е৮а•На§ѓ ৙а•Ба§∞а§Ња§£а•Ла§В а§Ха•З ৙а•На§∞а§Єа§Ва§Ча•Ла§В а§Єа•З а§Ьа•Ба§°а§Ља•З а§Ьৌ৮ ৙ৰ৊১а•З а§єа•Иа§В а§Фа§∞, а§Ха•На§ѓа§Њ ৐ৌ১ а§Ха§њ а§ѓа§єа§Ња§В ু৶৮ড়а§Ха§Ња§Уа§В а§Фа§∞ ৮ৌа§Чড়৮ড়ৃа•Ла§В а§Ха•А а§ђа§°а§Ља•А а§Ѓа§єа§ња§Ѓа§Њ а§єа•И? а§Ьড়১৮а•А а§Ха•А а§Хড়৮а•На§єа•Аа§В а§Фа§∞ а§Ьа§Ча§єа•Ла§В а§Ѓа•За§В ৮৺а•Аа§В ৶ড়а§Ца§Ња§И ৶а•Аа•§ а§Ча§∞а•На§≠а§Ча•Га§є а§Ха•З ৶а•Н৵ৌа§∞ ৙а§∞ а§єа•А ৶а•За§Ц а§≤а•За§В-а§Хড়১৮а•А а§Єа§Ња§∞а•А ু৶৮ড়а§Ха§Ња§Па§В а§Фа§∞ ৮ৌа§Чড়৮ড়ৃৌа§В а§Й১а•На§Ха•Аа§∞а•На§£ а§єа•Иа§В-а§Па§Х а§Єа•З а§Па§Х а§Ѓа•Ла§єа§Х а§Ѓа•Б৶а•На§∞а§Ња§Уа§В а§Ѓа•За§Ва•§ а§ѓа•З а§Ха§Ња§Х১а•Аа§ѓ а§∞а§Ња§Ьа§Њ ১а•Л ৴а•И৵৲а§∞а•Нুৌ৮а•Ба§ѓа§Ња§ѓа•А а§єа•А ৕а•З а§®а•§ а§Ѓа§В৶ড়а§∞ а§≠а•А а§ѓа§є ৴ড়৵ а§Ѓа§В৶ড়а§∞ а§єа•А ৮ а§єа•И? а§ђа§Ња§єа§∞ ৵৺ а§Ха•На§ѓа§Њ а§Ѓа§ња§≤а§Њ ৕ৌ? ৮а§В৶а•А-а§Ѓа§Вৰ৙ а§єа•А ৮? а§Па§Х а§Ца§Ва§≠а•З а§Ха•Л ৴а•На§∞а•А৙১ড় а§Е৙৮а•А а§Йа§≤а•На§Яа•А а§Йа§Ва§Ча§≤а•А а§Єа•З а§ђа§Ьа§Њ а§∞а§єа§Њ а§єа•Иа•§ а§≤а•Л! а§За§Єа§Ѓа•За§В ১а•Л ৪ৌ১а•Ла§В а§Єа•Ба§∞ а§Ѓа•Ма§Ьа•В৶ а§єа•Иа§Ва•§ а§ѓа§є а§Ха•Иа§Єа§Њ а§Ьৌ৶а•В а§єа•И? а§Ьৌ৶а•В ৮৺а•Аа§В а§≠а•Иа§ѓа§Њ, а§Ча§£а§ња§§ а§єа•И а§ѓа§є, ৴а•Б৶а•На§І а§Ча§£а§ња§§а•§ а§Єа§Ња§Йа§Ва§° а§Еа§∞а•Н৕ৌ১ ৮ৌ৶ а§≠а•А ১а•Л а§Ка§Ја•На§Ѓа§Њ а§Фа§∞ ৙а•На§∞а§Хৌ৴ а§Ха•А ১а§∞а§є ৵а•Иа§Ьа•На§Юৌ৮ড়а§Х а§Е৮а•Ба§Єа§В৲ৌ৮ а§Ха§Њ а§єа•А ৵ড়ৣৃ ৮ а§єа•И? ৙৥৊ৌ ১а•Л а§Єа§ђ а§Єа•На§Ха•Ва§≤-а§Ха•Йа§≤а•За§Ь а§Ха•З ৶ড়৮а•Ла§В а§Ѓа•За§Ва•§ ৪ড়৶а•На§Іа§Ња§В১ а§≠а•А а§Фа§∞ ৙а•На§∞а§ѓа•Ла§Ч а§Ха§∞а§Ха•З а§≠а•А ৶а•За§Ца§Њ ৕ৌ а§Ха§њ ৮৺а•Аа§В? а§Яа•На§ѓа•В৮ড়а§Ва§Ч а§Ђа•Йа§Х ৵а§Ча•Иа§∞а§є-৵а§Ча•Иа§∞а§єа•§ а§Ка§∞а•На§Ьа§Њ а§Ха§Њ а§єа•А ১а•Л а§Ца•За§≤ а§єа•И а§ѓа§є а§Єа§ђ, а§Ъа§Ња§єа•З а§Іа•Н৵৮ড় а§єа•Л, а§Ъа§Ња§єа•З а§≤а§ѓ, а§Ъа§Ња§єа•З ৙а•На§∞а§Хৌ৴ а§Фа§∞ а§ѓа§є а§Ъа§∞а§Ња§Ъа§∞ а§Ьа•А৵৮-а§≤а•Аа§≤а§Њ а§≠а•А а§Ха•На§ѓа•Ла§В ৮৺а•Аа§В? а§Єа•НвАН৕а•Ва§≤ а§Єа•З а§≤а•За§Ха§∞ а§Єа•Ва§Ха•На§Ја•Нুৌ১ড়৪а•Ва§Ха•На§Ја•На§Ѓ ১а§Х, а§Єа§ђ а§Ха•Ба§Ы а§Ка§∞а•На§Ьа§Њ-১а§∞а§Ва§Ча•Л а§ѓа§Њ а§Ха§£а•Ла§В а§Ха•З а§єа•А а§Еа§Єа§Ва§Ца•На§ѓ ৙а•На§∞а§Ха§Ња§∞ а§Ха•З а§Єа•Н৙а§В৶৮а•Ла§В а§Ха§Њ а§єа•А ১а•Л а§Ца•За§≤ ৮৺а•Аа§В а§єа•И а§Ха•На§ѓа§Њ?
а§ѓа§є а§≤а•Аа§Ьа§ња§П а§За§Є а§Єа•Н১а§Ва§≠ ৙а§∞ а§ѓа§є а§Ха•На§ѓа§Њ а§Ца•Б৶ৌ а§єа•Ба§Ж а§єа•И? ৙а•На§∞а§Ња§Ъа•А৮ ১а•За§≤а•Ба§Ча•В а§≤ড়৙а•А а§єа•И а§ѓа§єа•§ ৮а§В৶а•А а§Ѓа§Вৰ৙ а§Ха•З ৶а•Л৮а•Ла§В а§Уа§∞ а§ѓа•З а§Ьа•Л а§Ѓа§В৶ড়а§∞ а§єа•Иа§В-а§Ха§Ња§Ѓа•З৴а•Н৵а§∞ а§Ѓа§В৶ড়а§∞ а§Фа§∞ а§Ха§Ња§Яа•З৴а•Н৵а§∞ а§Ѓа§В৶ড়а§∞, а§З৮а•На§єа•Аа§В а§Ха•З а§™а§Ња§Єа•§ а§З১ড়৺ৌ৪ а§єа§Ѓ а§≠а§Ња§∞১а•Аа§ѓа•Ла§В а§Ха•З а§≤а§ња§П а§Ьа•Нৃৌ৶ৌ а§Е৺ুড়ৃ১ ৮৺а•А а§∞а§Ца§§а§Ња•§ а§Е৙৮а•А а§За§Є а§Ха§Ѓа•А а§Ха§Њ а§ђа§єа•Б১ а§Ѓа§єа§Ва§Ча§Њ а§Ѓа•Ла§≤ а§≠а•А а§Ъа•Ба§Ха§Ња§ѓа§Њ а§єа•А а§єа•Ла§Ча§Њ ৺ু৮а•За•§ а§Ьа§ња§Єа§Ха§Њ а§З১ড়৺ৌ৪ ১а§Ча§°а§Ља§Њ ৮৺а•Аа§В, а§Йа§Єа§Ха•А а§∞а§Ња§Ь৮а•А১ড় а§≠а•А а§Ха•Иа§Єа•З ১а§Ча§°а§Ља•А а§єа•Ла§Ча•А а§≠а§≤а§Ња•§ а§≠а§≤а§Њ а§єа•Л а§З৮ а§Еа§≠а§ња§≤а•За§Ца•Ла§В а§Ха§Њ а§Фа§∞ а§≠а§≤а§Њ а§єа•Л а§Й৮ а§Ча§°а§Ља•З а§Ѓа•Ба§∞а•Н৶а•З а§Йа§Цৌৰ৊৮а•З а§Ха•А а§Ха§≤а§∞ а§Ѓа•За§В ৮ড়ৣа•НвАНа§£а§Ња§§ а§≤а•Ла§Ча•Ла§В а§Ха§Њ, а§Ьড়৮а•На§єа•Ла§В৮а•З а§Ца•Б৶ а§єа§Ѓа§Ња§∞а§Њ а§З১ড়৺ৌ৪ а§єа§Ѓа§Ха•Л ৮ড়а§Ха§Ња§≤ а§Ха•З ৕ুৌৃৌ а§Фа§∞ а§Єа§ња§Ца§Ња§ѓа§Ња•§ а§ђа§єа§∞а§єа§Ња§≤, а§За§Є а§Еа§≠а§ња§≤а•За§Ц а§Ха•З а§Е৮а•Ба§Єа§Ња§∞ а§ѓа§є а§Ѓа§В৶ড়а§∞ 1213 а§Ѓа•За§В ৮ড়а§∞а•Нুড়১ а§єа•Ба§Ж ৕ৌ ৃৌ৮а•А а§Жа§Ь а§Єа•З а§Ха•Ла§И а§Ж৆ а§Єа•М ৵а§∞а•На§Ј ৙а•Ва§∞а•На§µа•§ а§З১৮ৌ ১а•Л а§єа§Ѓа§Ња§∞а•З а§Ьа•Иа§Єа•З а§Еа§≤а•Н৙а§Ьа•На§Ю а§≠а•А а§Ѓа§єа§Єа•Ва§Є а§Ха§∞ а§Єа§Ха•З а§ХвАМа§њ а§ђа§°а§Ља•З а§Ха§≤ৌ৙а•На§∞а•За§Ѓа•А ৕а•З а§ѓа•З а§Ха§Ња§Х১а•Аа§ѓ а§∞а§Ња§Ь৵а§В৴ а§Ха•З а§≤а•Ла§Ча•§ а§З৮а§Ха•З ৴ড়а§≤а•Н৙ а§Ха•А а§Ха•Ба§Ы а§Ца§Ња§Є а§Е৙৮а•А ৙৺а§Ъৌ৮ а§єа•Иа•§ а§Чৌৃ৮ а§Фа§∞ ৮а•Г১а•На§ѓ а§Ха•А ু৮а•Ла§єа§Ња§∞а•А а§≠а§Ва§Ча§ња§Ѓа§Ња§Уа§В а§Ха§Њ ৙а•На§∞а§Ња§Ъа•Ба§∞а•На§ѓ а§ѓа§є а§≠а•А а§Єа§Ња§Ђ а§Ь১ৌ১ৌ а§єа•И а§Ха§њ а§Єа§Ва§Ча•А১ а§Фа§∞ ৮а•Г১а•На§ѓ а§Ѓа•За§В а§≠а•А ৮ড়ৣа•НвАНа§£а§Ња§§ а§∞а§єа•З а§єа•Ла§Ва§Ча•З а§ѓа•З а§≤а•Ла§Ча•§ а§Ха§Ња§Х১а•Аа§ѓ ৮а§∞а•З৴ а§Ча§£а§™а§§а§њ а§Ха•З а§Єа•З৮ৌ৙১ড় а§∞а•З৴а§∞а§≤а§Њ а§∞а•Б৶а•На§∞ а§Ха§Њ а§єа•А ৵а§В৴а§Ь ৕ৌ ৵৺, а§Ьа§ња§Єа§Ха•З а§Ха§Ња§∞а§£ а§Ха§Яа•З৴а•Н৵а§∞ ৮ৌু ৙ৰ৊ৌ а§За§Є ৙ৌа§∞а•Н৴а•Н৵৙а§∞а•Н১а•А а§Ѓа§В৶ড়а§∞ а§Ха§Ња•§ ৴а•На§∞а•А৙১ড় а§Ђа•Ла§Яа•Л а§Ца•Аа§Ва§Ъ৮а•З а§Ѓа•За§В ু৴а§Ча•Ва§≤ а§єа•Иа•§ а§Ѓа§єа§Ња§∞১ а§єа§Ња§Єа§ња§≤ а§єа•И а§Йа§Єа•З а§Ђа•Ла§Яа•Ла§Ча•На§∞а§Ња§Ђа•А а§Ѓа•За§Ва•§ а§Ха•На§ѓа•Ла§В ৮ а§єа•Л? ৙а•В৮ৌ а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓ а§За§Ва§Єа•На§Яа•Аа§Яа•На§ѓа•Ва§Я а§Ха§Њ а§Єа•Н৮ৌ১а§Х а§єа•И ৵৺ а§Фа§∞ а§ѓа§єа•Аа§В а§єа•И৶а§∞ৌ৐ৌ৶ а§Ха•А ১а•За§≤а•Ба§Ча•Б а§ѓа•В৮ড়৵а§∞а•На§Єа§ња§Яа•А а§Ѓа•За§В а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓ-৵ড়৶а•На§ѓа§Њ а§Ха§Њ ৵а•На§ѓа§Ња§Ца•Нৃৌ১ৌ а§≠а•Аа•§ а§Ђа§ња§∞, а§За§Є а§Ѓа§В৶ড়а§∞ а§Єа•З ১а•Л а§Йа§Єа§Ха§Њ а§≤а§Чৌ৵ а§Ха•Ба§Ы ৵ড়৴а•За§Ј а§єа•А а§єа•Иа•§ а§ђа§Ъ৙৮ а§Ха•А ৙а•На§∞а•А১ а§ђа§єа•Б১ а§Чৌ৥৊а•А а§єа•Л১а•А а§єа•Иа•§ а§Йа§Єа•А а§Ха•З а§Ха§Ња§∞а§£ ১а•Л а§єа§Ѓ а§Єа§Ња§Ха•Нৣৌ১а•Н ৶а§∞а•Н৴৮ а§Ха§∞ а§∞а§єа•З а§єа•Иа§В, а§За§Є а§Єа•Ма§В৶а§∞а•На§ѓ а§Ха§Ња•§
а§∞а§Ња§Єа•Н১а•З а§Ха•З ৶а•Л৮а•Ла§В ১а§∞а§Ђ ৪৙а•Н১৙а§∞а•На§£а•А а§Ха•З ৵а•Га§Ха•На§Ја•Ла§В а§Ха•А а§ђа§єа§Ња§∞ а§єа•Иа•§ а§Ка§Ва§Ъа§Њ ৮৺а•Аа§В а§єа•И а§Ѓа§В৶ড়а§∞, ৙а§∞ а§Ьа•На§ѓа•Ла§В-а§Ьа•На§ѓа•Ла§В ৮ড়а§Ха§Я а§Ж১а•З а§Ьৌ১а•З а§єа•Иа§В, а§Йа§Єа§Ха•А а§≠৵а•Нৃ১ৌ а§≠а•А ৮ড়а§Ца§∞১а•А а§Ьৌ১а•А а§єа•Иа•§ ৶а§Ха•На§Ја§ња§£ а§Ха•З а§Ѓа§В৶ড়а§∞а•Ла§В а§Ѓа•За§В а§Єа§≠а•А а§Ьа§Ча§є а§Ча•Л৙а•Ба§∞ ৶а•Аа§Ц১а•З а§єа•Иа§В, ৙а§∞ а§Ха§Ња§Х১а•Аа§ѓа•Ла§В а§Ха•А ৮ড়а§∞а•Нুড়১ড়ৃа•Ла§В а§Ѓа•За§В а§Ка§Ва§Ъа•З ৴ড়а§Ца§∞ ৮৺а•Аа§В ৶ড়а§Ц১а•За•§ а§Іа•Нৃৌ৮ а§Єа•З ৶а•За§Ц৮а•З ৙а§∞ а§Ыа•Ла§Яа§Њ-а§Єа§Њ а§Ча•Л৙а•Ба§∞ а§≠а•А ৶ড়а§Ца•За§Ча§Њ, а§Ѓа§Ча§∞ а§єа§≤а•На§Ха•А а§Иа§Ва§Яа•Ла§В а§Єа•З ৮ড়а§∞а•Нুড়১, ১ৌа§ХвАМа§њ а§Ы১ ৙а§∞ а§Ьа•Нৃৌ৶ৌ а§≠а§Ња§∞ ৮ ৙ৰ৊а•За•§ а§Єа§Ња§∞а•А а§Ха§≤а§Њ а§Ча§∞а•На§≠ а§Ча•Га§є а§Фа§∞ а§Єа§≠а§Њ а§Ѓа§Вৰ৙ а§Ха•З а§Єа•Н১а§Ва§≠а•Ла§В ৙а§∞ ৮ড়а§Ыৌ৵а§∞ а§єа•Иа•§ а§ђа§°а§Ља•З-а§ђа§°а§Ља•З ৴ড়৵а§≤а§ња§Ва§Ч а§Фа§∞ а§Ча§∞а•На§≠а§Ча•Га§є а§Ха•З а§К৙а§∞ а§Ы১ ৙а§∞ ৐৮ৌ а§Ъа§Ха•На§∞, а§ѓа§є а§Ха§Ња§Х১а•Аа§ѓ ৴ড়а§≤а•Н৙ а§Ха•А ৙৺а§Ъৌ৮ а§єа•И, ৵ড়৴а•Зৣ১ৌ а§єа•Иа•§ а§Ча§∞а•На§≠а§Ча•Га§є а§Ха•З ৶а•Н৵ৌа§∞а§Њ а§Єа•З а§Єа§Яа•З ৴ড়а§≤а•Н৙ ৵ড়৴а•За§Ј а§Ха§≤ৌ৙а•Ва§∞а•На§£ а§≤а§Ч১а•З а§єа•Иа§Ва•§ а§Па§Х ৙৺а§Ъৌ৮ а§Фа§∞ а§≠а•А, а§ѓа§є а§Ха§њ а§Ха§Ња§Х১а•Аа§ѓ ৶а•Н৵ৌа§∞а•Ла§В а§Ха•З а§К৙а§∞ а§Ча§Ьа§≤а§Ха•На§Ја•На§Ѓа•А а§ѓа§Њ а§Ча§£а§™а§§а§њ а§Ха•А а§Ѓа•Ва§∞а•Н১ড় а§≤а§Ч১а•А а§єа•И а§Фа§∞ ৶а•Н৵ৌа§∞а•Ла§В а§Ха•З а§К৙а§∞ а§Ѓа§Ха§∞-১а•Ла§∞а§£а•§ а§Ѓа§Ха§∞ а§Ха•З а§Ѓа•Ба§Ц а§Єа•З ৮ড়а§Ха§≤১а•А а§≤১ৌа§Па§В а§Ѓа•Ба§Ца•На§ѓ ৶а•З৵ুа•Ва§∞а•Н১ড় а§Єа•З а§Ьа§Њ а§Ѓа§ња§≤১а•А а§єа•Иа§Ва•§ а§Ѓа§Ха§∞১а•Ла§∞а§£ ৮ৌু а§За§Єа•Аа§≤а§ња§Па•§
а§Ѓа§В৶ড়а§∞ а§Ха§Њ ৙а•На§∞৶а§Ха•На§Ја§ња§£а§Њ-৙৕ а§≠а•А а§ђа§єа•Б১ ু৮а•Ла§∞а§Ѓ а§єа•Иа•§ ৺ৌ৕а•А, а§Єа§ња§Ва§є а§Фа§∞ а§єа§Ва§Є ৵а§Ча•Иа§∞а§є а§Й১а•На§Ха•Аа§∞а•На§£ а§єа•Иа§В, а§ѓа§єа§Ња§В а§Фа§∞ ৙৶а•На§Ѓ ৵а§Ча•Иа§∞а§є а§≠а•Аа•§ а§Х৺১а•З а§єа•Иа§В, а§Ха§Ња§Х১а•Аа§ѓ ৴ড়а§≤а•Н৙ а§Ѓа•За§В а§ђа•М৶а•На§І-৙৶а•Н৲১ড় а§Фа§∞ а§єа•Ла§ѓа§Єа§≤ ৙৶а•Н৲১ড়-а§Па§Х ৮ড়а§∞а§≤а§Ва§Ха•Г১ а§Фа§∞ ৶а•Ва§Єа§∞а•А а§Еа§≤а§Ва§Ха•Га§§а•§ ৶а•Л৮а•Ла§В а§Ха•З а§ђа•Аа§Ъ а§Ха§Њ а§Ѓа§Ња§∞а•На§Ч ৮ড়а§Ха§Ња§≤а§Њ а§Ча§ѓа§Њ а§єа•Иа•§ а§Еа§≤а§Ва§Ха§Ња§∞ а§Еа§Іа§ња§Х ৮৺а•Аа§В, а§Ха§ња§В১а•Б ৮ড়৴а•На§Ъа§≤ а§Іа•Нৃৌ৮-а§Ѓа•Б৶а•На§∞а§Њ а§Ха•А а§Ьа§Ча§є а§Ьа•А৵ৌа§В১ ৺ৌ৵-а§≠ৌ৵а•Ла§В ৙а§∞ а§Ьа•Ла§∞ ৶а•З৮а•З ৵ৌа§≤а•А а§Па§Хুৌ১а•На§∞ ৙а•Ба§Єа•Н১ড়а§Ха§Њ, а§Ьа•Л а§єа§ња§В৶а•А а§Ѓа•За§В ৶ড়а§Ца§Ња§И ৙ৰ৊а•А, а§Йа§Єа§Ѓа•За§В а§Ха§Њ а§Па§Х а§Еа§В৴ а§Й৶а•Н৲১ а§Ха§∞৮а•З а§≤а§Ња§ѓа§Х а§≤а§Ч а§∞а§єа§Њ а§єа•Иа•§ а§Еа§Я৙а§Яа•А а§≠а§Ња§Ја§Њ а§Ха•З ৐ৌ৵а§Ьа•В৶ а§Ха§єа•Аа§В а§Ча§єа§∞а•З а§Ѓа•За§В ু৮ а§Ха•Л ৙а§Ха§°а§Љ а§≤а•З৮а•З ৵ৌа§≤а•А ৐ৌ১ а§Ха§њ а§Ха§Ња§Х১а•Аа§ѓ ৴ড়а§≤а•Н৙ а§Ѓа•За§В а§Ъа•И১৮а•На§ѓ ৶ড়а§Цৌ৮а•З а§Ха•А ৙а•На§∞৕ৌ а§єа•Иа•§ а§Ъа§Ња§єа•З ৶а•З৵ুа•Ва§∞а•Н১ড়ৃৌа§В а§єа•Ла§В, а§Ъа§Ња§єа•З ৮а•На§ѓа§Ња§ѓ ৮ৌа§∞а•Аа§Ѓа•Ва§∞а•Н১ড়ৃৌа§В, а§Єа§≠а•А а§Ѓа•За§В а§ѓа§єа•А а§Ъа•И১৮а•На§ѓ ৶ড়а§Ца§Ња§И ৙ৰ৊১ৌ а§єа•И, а§За§Єа§≤а§ња§П а§Ѓа•Ва§∞а•Н১ড়ৃа•Ла§В а§Ѓа•За§В а§Ьа•А৵-а§Ъа•И১৮а•На§ѓ ৙а•На§∞а§Ха§Я а§єа•Л১ৌ а§єа•И, а§ѓа•З ৵ৌа§Ха•На§ѓ а§Ѓа•Ба§Эа•З а§Ъа•Ма§Ва§Ха§Њ ৶а•З১а•З а§єа•Иа§В, а§За§Єа§≤а§ња§П ৙ৌ৆а§Х а§Ха•Л а§≠а•А а§Ъа•Ма§Ха§Ња§Па§Ва§Ча•З а§єа•А, а§Ра§Єа•А а§Ѓа•Ба§Эа•З а§Йа§Ѓа•На§Ѓа•А৶ а§єа•Иа•§ а§Ъа•Ма§Ва§Хৌ৮а•З а§Ха§Њ ু১а§≤а§ђ а§ѓа§єа§Ња§В а§Єа§ња§∞а•На§Ђ а§Ъа•Ма§Ва§Хৌ৮ৌ а§≠а§∞ ৮৺а•Аа§В, а§Ха•Ба§Ы а§Єа•Ла§Ъ৮а•З а§Ха•Л а§≠а•А ৙а•На§∞а•За§∞ড়১ а§Ха§∞৮а•З ৵ৌа§≤а§Њ а§єа•И, а§Ра§Єа§Њ а§Ѓа•Ба§Эа•З а§Ха•На§ѓа•Л а§≤а§Ч а§∞а§єа§Њ а§єа•И?
৶а•Л а§Ша§Ва§Яа•З а§Ха§ђ а§ђа•А১ а§Ча§П, а§Ха•Ба§Ы ৙১ৌ ৮৺а•Аа§В а§Ъа§≤а§Ња•§ а§Па§Ха§Ња§Па§Х а§Ша§°а§Ља•А ৙а§∞ ৮ড়а§Ча§Ња§є а§Ча§Иа§В, а§Ьа•На§ѓа•Л১а•НвАНа§Єа•Н৮ৌ а§Ха•А, ১а•Л а§єа§°а§Ља§ђа§°а§Ља§Ња§Ха§∞ а§Й৪৮а•З а§єа§Ѓ ৶а•Л৮а•Ла§В а§Ха•Л а§Єа§Ъа•З১ а§Ха§ња§ѓа§Њ, а§Ъа§≤а•Л а§≠а§И, а§Хড়১৮а•А ৶а•За§∞ а§єа•Л а§Ча§И, ৵а§∞а§Ва§Ча§≤ ৶а•За§Ц৮ৌ а§єа•И а§Ха§њ ৮৺а•Аа§В? ৪ৌ১ а§ђа§Ьа•З а§Ха•А а§Ча§Ња§°а§Ља•А ৙а§Хৰ৊৮а•А а§єа•И а§Ха§њ ৮৺а•Аа§В? а§Ђа§Яа§Ња§Ђа§Я а§єа§Ѓ а§≤а•Ла§Ч а§∞ৌু৙а•Н৙ৌ а§Ѓа§В৶ড়а§∞ а§Ха•Л а§Еа§≤৵ড়৶ৌ а§Ха§єа§Ха•З а§Яа•Иа§Ха•На§Єа•А ৙а§∞ ৪৵ৌа§∞ а§єа•Ба§П а§Фа§∞ а§∞ৌু৙а•Н৙ৌ а§Єа§∞а•Л৵а§∞ а§Ха•А ৴а•Ла§≠а§Њ ৮ড়৺ৌа§∞১а•З а§єа•Ба§П а§Ша§Ва§Яа•З а§≠а§∞ а§Ѓа•За§В а§єа•А ৵а§∞а§Ва§Ча§≤ ৙৺а•Ба§Ва§Ъ а§Ча§Па•§ а§Йа§°а•Б৙а•А а§єа•Ла§Яа§≤ а§Ха§Њ а§ђа§Ъа§Њ-а§Ца•Ба§Ъа§Њ а§ђа•За§Єа•Н৵ৌ৶ а§Фа§∞ ৆а§Ва§°а§Њ а§≠а•Ла§Ь৮ ৮ড়а§Ча§≤а§Ха§∞ а§Єа•Аа§Іа•З а§Е৙৮а•З а§Еа§Єа§≤а•А а§Ч১а§В৵а•На§ѓ а§Єа§єа§Єа•НвАН১а•На§∞а§Єа•Н১а§Ва§≠ ৶а•З৵ৌа§≤а§ѓ ৵а•За§ѓа•На§ѓа•Аа§Єа•Н১а§Ва§≠а§Ња§Ча•Ба§°а§Ља•А а§Ьа§Њ ৙৺а•Ба§Ва§Ъа•За•§ ৺৮а•На§Ѓа§Ха•Ла§Ва§°а§Њ а§Ха§єа§≤ৌ১ৌ ৕ৌ а§ѓа§є ৮а§Ча§∞ а§З১ড়৺ৌ৪ а§Ѓа•За§Ва•§ а§Єа§єа§Єа•НвАН১а•На§∞а§Єа•Н১а§Ва§≠а§Њ а§Ха§Њ а§Еа§∞а•Н৕ ৶а•За§Ц১а•З а§єа•А а§Єа§Ѓа§Э а§Ѓа•За§В а§Ж а§Ча§ѓа§Ња•§ а§ѓа§єа§Ња§В а§Ха§єа•Аа§В ৶ড়৵ৌа§∞а•За§В ৮৺а•Аа§В, а§Єа•Н১а§Ва§≠ а§єа•А ৶а•А৵ৌа§∞а•Ла§В а§Ха§Њ а§Ха§Ња§Ѓ а§Ха§∞১а•З а§єа•Иа§Ва•§ а§Ъа§Ња§∞ а§Єа•Н১а§Ва§≠а•Ла§В ৙а§∞ а§Па§Х ৴ড়а§≤а§Ња§Ђа§≤а§Х а§Фа§∞ а§За§Єа•А ১а§∞а§є ৵ড়৪а•Н১ৌа§∞ а§єа•Л১ৌ а§єа•И а§Ѓа§В৶ড়а§∞ а§Ха§Ња•§ ৙а•На§∞а§Хৌ৴ а§Фа§∞ ৵ৌৃа•Б а§Ха§Њ ৮ড়а§∞а•На§ђа§Ња§І ৙а•На§∞৵а•З৴ а§Єа•Б৮ড়৴а•На§Ъড়১ а§Ха§ња§ѓа§Њ а§Ча§ѓа§Њ а§За§Є ১а§∞а§єа•§ а§Єа•Н১а§Ва§≠а•Ла§В а§Ха•З а§Ѓа§Іа•На§ѓ а§ђа§єа•Б১ вАМа§єа•А а§ђа§Ња§∞а•Аа§Х ৴а•В৮а•На§ѓ, а§З১৮ৌ а§ђа§Ња§∞а•Аа§Х а§Ха§њ а§Па§Х а§Па§Ха§Ња§Па§Х ৶ড়а§Ца•З а§≠а•А ৮৺а•Аа§В а§Ха§ња§Єа•А а§Ха•Ла•§ а§Ца§Ња§Є ৐ৌ১ а§ѓа§є а§Ха§њ а§Єа§Ња§∞а•З а§Єа•Н১а§Ва§≠а•Ла§В ৙а§∞ ৮а•Г১а•На§ѓ-а§Ѓа•Б৶а•На§∞а§Ња§Уа§В а§Ха§Њ ৵ড়৪а•На§Ѓа§ѓа§Ха§Ња§∞а•А ৵а•И৵ড়৲а•На§ѓа•§ ৮а•Г১а•На§ѓ ৵ড়৴а•За§Ја§Ьа•На§Юа•Ла§В ৮а•Г১а•На§ѓ-а§∞а§Єа§ња§Ха•Ла§В а§Ха•З а§≤а§ња§П а§Ра§Єа§Њ ৙а•На§∞১а•На§ѓа§Ха•Нৣ৙ৌ৆ ৮а•Г১а•На§ѓ а§Ха§Њ а§Ха•На§ѓа§Њ а§Фа§∞ а§≠а•А а§Ха§єа•Аа§В а§Єа•Ба§≤а§≠ а§єа•Ла§Ча§Њ? а§Ра§Єа§Њ а§≤а§Ч১ৌ ৮৺а•Аа§Ва•§ ৶а•З৵ৌа§≤а§ѓ а§Ха•З а§ђа•Аа§Ъа•Ла§В-а§ђа•Аа§Ъ а§∞а§Ва§Ч а§Ѓа§Ва§°а§™а•§ а§Єа§Ња§∞а•З а§Єа•Н১а§Ва§≠ а§Ха•Ба§Ы а§За§Є ১а§∞а§є ৵ড়৮ড়а§∞а•Нুড়১ а§Фа§∞ ৵ড়৮а•На§ѓа§Єа•Н১ а§Ха§њ а§∞а§Ва§Ча§Ѓа§Вৰ৙ а§Ха•За§В৶а•На§∞ а§Ѓа•За§В ৙а•На§∞১ড়ৣа•Н৆ড়১ а§єа•Ла§В, а§Ча§∞а•На§≠а§Ча•Га§є а§Ха§Њ ৮ড়а§∞а•На§Ѓа§Ња§£-а§Ха•М৴а§≤ а§Е৵а§∞а•На§£а§®а•Аа§ѓа•§ а§Єа§Ѓа§Э а§Ѓа•За§В а§Жа§ѓа§Њ а§Ха§њ а§За§Є а§Ѓа§В৶ড়а§∞ а§Ха•А ৙а•На§∞৪ড়৶ড়৲а•НвАН а§ѓа•Ла§В а§єа•А ৮৺а•Аа§Ва•§ а§Жа§Ь а§≠а•А а§Ьа§ђ а§З১৮ৌ а§Ьа•А৵а§В১ а§єа•И ১а•Л а§Йа§Є а§Єа§Ѓа§ѓ а§Ха•На§ѓа§Њ ৮৺а•Аа§В а§∞а§єа§Њ а§єа•Ла§Ча§Њ?
а§З১ড়৺ৌ৪ а§єа§Ѓ а§≠а§Ња§∞১а•Аа§ѓа•Ла§В а§Ха•З а§≤а§ња§П а§Ьа•Нৃৌ৶ৌ а§Е৺ুড়ৃ১ ৮৺а•Аа§В а§∞а§Ца§§а§Ња•§ а§Е৙৮а•А а§За§Є а§Ха§Ѓа•А а§Ха§Њ а§ђа§єа•Б১ а§Ѓа§єа§Ва§Ча§Њ а§Ѓа•Ла§≤ а§≠а•А а§Ъа•Ба§Ха§Ња§ѓа§Њ а§єа•А а§єа•Ла§Ча§Њ ৺ু৮а•За•§ а§Ьа§ња§Єа§Ха§Њ а§З১ড়৺ৌ৪ ১а§Ча§°а§Ља§Њ ৮৺а•Аа§В, а§Йа§Єа§Ха•А а§∞а§Ња§Ь৮а•А১ড় а§≠а•А а§Ха•Иа§Єа•З ১а§Ча§°а§Ља•А а§єа•Ла§Ча•А а§≠а§≤а§Њ, а§≠а§≤а§Њ а§єа•Л а§З৮ а§Еа§≠а§ња§≤а•За§Ца•Ла§В а§Ха§Њ а§Фа§∞ а§≠а§≤а§Њ а§єа•Л а§Й৮ а§Ча§°а§Ља•З а§Ѓа•Ба§∞а•Н৶а•З а§Йа§Цৌৰ৊৮а•З а§Ха•А а§Ха§≤а§Њ а§Ѓа•За§В ৮ড়ৣа•НвАНа§£а§Ња§§ а§≤а•Ла§Ча•Ла§В а§Ха§Њ, а§Ьড়৮а•На§єа•Ла§В৮а•З а§Ца•Б৶ а§єа§Ѓа§Ња§∞а§Њ а§З১ড়৺ৌ৪ а§єа§Ѓа§Ха•Л ৮ড়а§Ха§Ња§≤ а§Ха•З ৕ুৌৃৌ а§Фа§∞ а§Єа§ња§Ца§Ња§ѓа§Ња•§ а§Ха§Ња§Х১а•Аа§ѓ ৵а§В৴-৵а•Га§Ха•На§Ј ৙а•На§∞৕ু ৙а•На§∞а§Ња§≤а§∞а§Ња§Ьа•Б 1025-1085 а§Єа•З ৙а•На§∞а§Ња§∞а§Ва§≠ а§єа•Л১ৌ а§єа•И, а§Фа§∞ ৙а•На§∞১ৌ৙ а§∞а•Б৶а•На§∞ 1290-1326 ১а§Х а§Ђа§≤১ৌ а§Ђа•Ва§≤১ৌ а§єа•Иа•§ а§Ха§Ња§Х১а•Аа§ѓ ৵а§В৴ а§Єа•З ৙а•Ва§∞а•Н৵ а§Ъа§Ња§≤а•Ба§Ха•На§ѓа•Ла§В а§Ха§Њ а§∞а§Ња§Ьа§Њ а§•а§Ња•§ а§Ха§Ња§Х১а•Аа§ѓа•Ла§В а§Ѓа•За§В а§Єа§ђа§Єа•З ৙а•На§∞১ৌ৙а•А а§Ча§£а§™а§§а§ња§¶а•З৵ а§єа•Ба§П а§Фа§∞ а§Й৮а§Ха•З ৐ৌ৶ а§∞а•Б৶а•На§∞ু৶а•З৵а•А а§ѓа§Њ а§∞а•Б৶а•На§∞а§Ња§Ва§ђа§Њ ৮ৌু а§Ха•А а§Й৮а§Ха•А ৙а•Б১а•На§∞а•А, а§Ьড়৮а§Ха§Њ а§Йа§≤а•На§≤а•За§Ц-а§Єа•Б৮ৌ, а§Ѓа§Ња§∞а•На§Ха•Л৙а•Ла§≤а•Л ৮а•З а§≠а•А а§Ха§ња§ѓа§Њ а§єа•Иа•§ ৵а§∞а§Ва§Ча§≤ а§Ха§Њ ৙а•Ба§∞ৌ৮ৌ а§Р১ড়৺ৌ৪ড়а§Х ৮ৌু а§Уа§∞а•Ба§Ча§≤а•На§≤а•Б а§•а§Ња•§ а§Уа§Ва§Яа§ња§Ѓа§ња§Яа•На§Яа§Њ а§Фа§∞ а§Па§Х৴ড়а§≤а§Њ а§≠а•Аа•§ а§Ха•На§ѓа§Њ а§ѓа•Б৶а•На§І а§Ха•М৴а§≤, а§Ха•На§ѓа§Њ а§µа§Ња§£а§ња§Ьа•На§ѓ ৵а•Нৃৌ৙ৌа§∞ а§Фа§∞ а§Ха•На§ѓа§Њ а§Ха§≤а§Њ-а§Ха•М৴а§≤, а§Єа§≠а•А а§Ха•На§Ја•З১а•На§∞а•Ла§В а§Ѓа•За§В а§З৮ а§Ха§Ња§Х১а•Аа§ѓа•Ла§В а§Ха•З а§Е৶а•Ба§≠১ ৙а•Ба§∞а•Ба§Ја§Ња§∞а•Н৕ а§Ха•З а§Єа•На§Ѓа§Ња§∞а§Х а§Жа§Ь а§≠а•А ৶а•За§Ца•З а§Ьа§Њ а§Єа§Х১а•З а§єа•Иа§Ва•§ ু৮ а§Ѓа•За§В а§Ха•Ма§Ва§Іа§Њ а§Еа§Ъৌ৮а§Х а§єа•А-а§Ха§єа•Аа§В а§єа§Ѓ а§≠а•А а§Е৙৮а•З ৙а•Ба§∞а•Ба§Ца•Ла§В а§Ха•З ৙а•Ба§∞а•Ба§Ја§Ња§∞а•Н৕ а§Іа•Н৵а§В৪ৌ৵а•За§Ј а§єа•А ১а•Л ৮৺а•Аа§В?
а§Ѓа§В৶ড়а§∞ ১а•Л а§Е৶а•Ба§≠а•Б১ а§єа•И, а§∞ৌু৙а•Н৙ৌ а§Ѓа§В৶ড়а§∞ а§Єа•З а§≠а•А а§≠৵а•Нৃ১а§∞ а§Фа§∞ а§Е১а•Ба§≤৮а•Аа§ѓ а§Єа•НвАН৕ৌ৙১а•На§ѓ а§Ха§≤а§Њ а§Ха§Њ ৮ুа•В৮ৌ, а§≤а•За§Хড়৮ а§∞а§Ц-а§∞а§Цৌ৵ а§За§Єа§Ха•А ৙а•На§∞১ড়ৣа•Н৆ৌ а§Ха•З а§Е৮а•Ба§∞а•Б৙ а§Х১а§И ৮৺а•Аа§Ва•§ ু৮ ৵ড়ৣৌ৶ а§Єа•З а§≠а§∞ а§Ча§ѓа§Њ а§За§Є ৶а•Ба§∞а•Н৶৴ৌ а§Ха•З а§Єа§Ња§Ха•Нৣৌ১ а§Єа•За•§ ৪ৌু৮а•З а§єа•А а§Ьа•Л а§Ѓа§Вৰ৙ ৕ৌ-а§Е১а•Ба§≤৮а•Аа§ѓ а§Ха§≤ৌ১а•На§Ѓа§Х а§Єа•Ма§В৶а§∞а•На§ѓ а§Ха§Њ а§Еа§Іа§ња§Ја•Н৆ৌ৮, ৵৺ а§Ьৌ৮а•З а§Ха§ђ а§Єа•З а§Яа•Ва§Яа§Њ ৙ৰ৊ৌ а§єа•Иа•§ а§Ха§Ња§≤-৙а•На§∞а§≠ৌ৵ а§Єа•З ৮৺а•Аа§В, а§ђа§≤а•На§Ха§њ а§За§Єа§Ха•А а§Яа•Ва§Я-а§Ђа•Ва§Я а§Ха•А а§Ѓа§∞а§Ѓа•Нু১ а§Ха§∞৵ৌ৮ৌ а§Ъৌ৺৮а•З ৵ৌа§≤а•Ла§В а§Ха•А ৮ৌ৶ৌ৮а•А а§Ха•З а§Ђа§≤а§Єа•Н৵а§∞а•Ва§™а•§ а§≤а§Ч১ৌ ৮৺а•Аа§В, а§Ха§≠а•А ৵৺ а§Е৙৮а•А ৙а•Ва§∞а•Н৵ а§Е৵৪а•НвАН৕ৌ а§Ха•Л ৙а•На§∞ৌ৙а•Н১ а§Ха§∞ ৙ৌа§Па§Ча§Ња•§ а§Е৙а•Ва§∞а§£а•Аа§ѓ а§Ха•Нৣ১ড় а§єа•И а§ѓа§є-а§Еа§Ха•На§Ја§∞৴а§Га•§ а§ѓа§є а§Ѓа§В৶ড়а§∞ а§Ха§Ња§Х১а•Аа§ѓ ৮а§∞а•З৴ а§∞а•В৶а•На§∞৶а•З৵ ৙а•На§∞৕ু ৮а•З ৐৮৵ৌৃৌ а§•а§Ња•§ ৵а§∞а•На§Ј 1163а§Ѓа•За§Ва•§ а§Ьа§ња§Є ৵а•З৶ড়а§Ха§Њ ৙а§∞ а§Ѓа§В৶ড়а§∞ а§Ца§°а§Ља§Њ а§єа•И, ৵৺ а§Па§Х а§Ѓа•Аа§Яа§∞ а§Ка§Ва§Ъа•А а§єа•Ла§Ча•Аа•§ ৙а§∞а§ња§Іа§њ 31 а§Ча•Ба§£а§Њ 25 а§Ѓа•Аа§Яа§∞а•§ а§Ха•За§В৶а•На§∞а§ња§ѓ а§Єа§≠а§Ња§Ха§Ха•На§Ј а§Ха•З а§Ъа§Ња§∞а•Ла§В а§Уа§∞ а§Ѓа§В৶ড়а§∞ ৐৮а•З а§єа•Иа§Ва•§ ১а•А৮ а§Ѓа§В৶ড়а§∞ ৵ড়ৣа•НвАНа§£а•Б, ৴ড়৵ а§Фа§∞ а§Єа•Ва§∞а•На§ѓ а§Ха•За•§ ৵а•За§ѓа•На§ѓа•А а§Єа•Н১а§Ва§≠а§Ња§Ча•Ба§°а•А, а§Ха•А а§Ы৵ড় ু৮ а§Ѓа•За§В а§Єа§Ва§Ьа•Ла§Ха§∞ а§єа§Ѓ а§≠৶а•На§∞а§Ха§Ња§≤а•А а§Ѓа§В৶ড়а§∞ а§Ча§Па•§ а§За§Єа§Ха§Њ ৮ড়а§∞а•На§Ѓа§Ња§£ а§∞а•В৶а•На§∞а§Ња§Ва§ђа§Њ ৮а•З а§Ха§∞৵ৌৃৌ а§•а§Ња•§ а§Ѓа§В৶ড়а§∞ а§Ха•З а§Єа§Ѓа•Ва§Ъа•З ৙а§∞а§ња§Єа§∞ а§Ха•А а§Єа•Б৵а•Нৃ৵৪а•НвАН৕ৌ ৶а•За§Ца§Ха§∞ а§Ъড়১а•Н১ ৙а•На§∞৪৮а•Н৮ а§єа•Л а§Ча§ѓа§Ња•§ ৙а•Га§Ја•Н৆а§≠а•Ва§Ѓа§њ а§Ѓа•За§В а§≠а•Аа§Ја§£ а§Єа•Ба§В৶а§∞ а§≠а•Аа§Ѓа§Ња§Ха§Ња§∞ ৴ড়а§≤а§Њ а§єа•Иа•§ ৴ড়а§≤а§Њ а§Ха•На§ѓа§Њ, ৙а§∞а•Н৵১ а§єа•А а§Єа§Ѓа§Эа•Ла•§ а§Еа§Ча•На§∞а§≠а•Ва§Ѓа§њ а§Ѓа•За§В а§Ѓа•А৆а•З ৙ৌ৮а•А а§Ха§Њ ৵ড়৴ৌа§≤ а§Єа§∞а•Л৵а§∞, а§Ьа•Л а§Єа§Ѓа•Ва§Ъа•З ৮а§Ча§∞ а§Ха•А ৙а•На§ѓа§Ња§Є а§ђа•Ба§Эৌ১ৌ а§єа•Иа•§ а§∞а•В৶ৌа§Ва§ђа§Њ ৃ৕ৌ ৮ৌু ১৕ৌ а§Ча•Ба§£ а§Ха•А а§Па§Х ৵ড়а§≤а§Ха•На§Ја§£ а§∞ৌ৮а•А ৕а•Аа•§ ৙а•Ба§∞а•Ла§Ја•Ла§Ъড়১ ৵а•Аа§∞১ৌ ৵ ৙а•На§∞৴ৌ৪а§Ха•Аа§ѓ а§Ха•Нৣু১ৌ а§Єа•З а§Єа§В৙а§В৮, а§Ьа§ња§Єа§Ха•А а§Ѓа§єа§ња§Ѓа§Њ ৙а•На§∞১а•На§ѓа§Ха•На§Ј а§Е৮а•Ба§≠৵ а§Ха•А а§Ьа§Њ а§Єа§Х১а•А а§єа•И а§ѓа§єа§Ња§Ва•§ ৵৺ а§Ча§£а§™а§§а§ња§¶а•З৵ а§Ха•З ৶а•З৺ৌ৵৪ৌ৮ а§Ха•З а§Й৙а§∞а§Ња§В১ 1290 а§Єа§ња§В৺ৌ৪৮ৌа§∞а•Б৥৊ а§єа•Ба§И ৕а•Аа•§
৵৺ৌа§В а§Єа•З а§єа§Ѓ ৵а§∞а§Ва§Ча§≤ а§Ха§Њ ৵ড়а§Ца•Нৃৌ১ ৶а•Ба§∞а•На§Ч ৶а•За§Ц৮а•З а§Ча§Па•§ а§Єа§Ѓа§ѓ а§Ха§Ѓ а§ђа§Ъа§Њ а§•а§Ња•§ а§Ха§ња§≤а§Њ ১а•Л ৮ৌু৴а•За§Ј а§єа•А а§єа•Иа•§ ুৌ১а•На§∞ а§Па§Х ৵ড়৴ৌа§≤ а§Єа§≠а§Ња§Ча•Га§є а§≠а§∞ а§ђа§Ъа§Њ а§єа•И, а§Ха§ња§В১а•Б а§Іа•Н৵а§В৪ৌ৵৴а•За§Ј а§Па§Х а§У৙৮ а§Па§Еа§∞ а§Ѓа•На§ѓа•Ва§Ьа§ња§ѓа§Ѓ а§Ѓа•За§В а§Єа•Ба§∞а§Ха•Нৣড়১ а§єа•Иа•§ а§Йа§Є ৵ড়а§Ч১ ৵а•Иа§≠৵ а§Ха•З ৙а•На§∞১а•На§ѓа§Ха•На§Ј ৵ৌ৪а•Н১а•Б৙ৌ৆ а§Ха•А ১а§∞а§єа•§ а§ђа§Є а§Ха§ња§Єа•А ১а§∞а§є а§≠а§Ња§Ч-৶а•Ма§°а§Ља§Ха§∞ ৙а§∞а§ња§Ха•На§∞а§Ѓа§Њ а§Ха•А а§Йа§Єа§Ха•Аа•§ ৵а§∞а§Ва§Ча§≤ а§Фа§∞ ৺৮а•На§Ѓа§Ха•Ла§Ва§°а§Њ а§Ха•Л а§Ѓа§ња§≤а§Ња§Ха§∞ а§≤а§Ча§≠а§Ч 19 ৵а§∞а•На§Ч а§Ха§ња§≤а•Ла§Ѓа•Аа§Яа§∞ а§Ѓа•За§В ৵ড়৪а•Н১а•Г১ ৕ৌ а§ѓа§є ৶а•Ба§∞а•На§Ч а§Е৙৮а•А ৮а•М ৶а•Ба§∞а•На§≠а•За§Ш ৙а•На§∞а§Ња§Ъа•Аа§∞а•Ла§В а§Єа§Ѓа•За§§а•§ а§Ха§Ња§Х১а•Аа§ѓа§Ња§Ва§Іа•На§∞ а§Єа§Ња§Ѓа•На§∞а§Ња§Ьа•На§ѓ а§Ха•А а§∞а§Ња§Ь৲ৌ৮а•А а§Ха§Њ а§ѓа§є а§Е৙а•Ва§∞а•Н৵ а§Єа•На§Ѓа§Ња§∞а§Х ৶а•За§Ца•З ৐ড়৮ৌ а§ѓа§є ৃৌ১а•На§∞а§Њ а§Еа§Іа•Ва§∞а•А а§∞৺১а•А а§Єа§Ъа§Ѓа•Ба§Ъа•§ а§Ца•Иа§∞ а§Ча•Ба§Ьа§∞а•А а§єа§Ѓа§Ња§∞а•А а§Яа•На§∞а•З৮ а§Па§Х а§Ша§Ва§Яа§Њ а§≤а•За§Я ৕а•А, а§Ђа§ња§∞ а§≠а•А а§∞ী১ৌа§∞ а§Ра§Єа•А ৙а§Ха§°а§Ља•А а§Ха§њ ৶৪ а§ђа§Ьа•З а§Єа§ња§Ха§В৶а§∞ৌ৐ৌ৶ а§Ж а§≤а§Ча•За•§ ৙а•Иа§В১а•Аа§Є а§Ха§ња§≤а•Ла§Ѓа•Аа§Яа§∞ а§Ха§Њ а§≠а•Аа§Ја§£ а§Ь৮ৌа§Ха•Аа§∞а•На§£ ৙৕ ৙ৌа§∞ а§Ха§∞а§Ха•З а§Ча•На§ѓа§Ња§∞а§є а§ђа§Ьа•З а§≤а•За§Х-৵а•На§ѓа•В а§Ча•За§Єа•На§Я а§єа§Ња§Йа§Є а§Ж ৙৺а•Ба§Ва§Ъа•За•§ а§Ча§∞а§Ѓ ৙ৌ৮а•А а§Ха•З а§Єа•Н৮ৌ৮ ৮а•З а§Єа§Ња§∞а•А а§Ха•На§≤а§Ња§В১ড় а§єа§∞ а§≤а•А а§Фа§∞ а§Ча§єа§∞а•А ৮а•Аа§В৶ а§Єа•Ба§≤а§Њ а§¶а§ња§ѓа§Ња•§ а§Ра§Єа•А а§Ча§єа§∞а•А а§Фа§∞ а§Єа§∞а•Н৵৕ৌ ৮ড়৪а•Н৵৙ ৮а•Аа§В৶, а§Ьа•Иа§Єа•А а§єа§Ѓ а§Єа§∞а•Аа§Ца•З ১৕ৌа§Х৕ড়১ а§ђа•Б৶а•На§Іа§ња§Ьа•А৵ড়ৃа•Ла§В а§Ха•Л а§Ѓа•Б৴а•На§Ха§ња§≤ а§Єа•З а§єа•А а§Ха§≠а•А а§Ха§≠а§Ња§∞ ৮৪а•Аа§ђ а§єа•Л ৙ৌ১а•А а§єа•И а§Фа§∞, а§єа§Ѓа§Ња§∞а§Њ ৮ৌৃа§Х а§єа§ѓ а§єа§ѓ ৮ৌৃа§Х, а§Ха§єа§Ха•З а§Ьа§ња§Єа§Ха§Њ а§Єа•Н৵ৌа§Ч১ а§Ха§∞৮а•З а§Ха•А а§Ж৶১ ৙ৰ৊ а§Ьৌ৮а•З ৵ৌа§≤а•А а§єа•И а§Ѓа•Ба§Эа•З а§Йа§Єа•А а§Ха•З ৶а•Н৵ৌа§∞а§Њ а§Єа•Ба§≤а§≠ а§Ха§∞а§Ња§И а§Ча§И а§Па§Х ১а•За§≤а•Ба§Ча•В а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓ а§Ѓа§Ња§ѓа§Њ а§ђа§Ња§Ьа§Ња§∞ ৶а•За§Ц৮а•З а§Ха•З а§ђа§Ња§¶а•§
৴а•На§∞а•А৙১ড়? а§Йа§Єа•З ৶а•За§Ца§Ха§∞ а§Ха•М৮ а§Ха§єа•За§Ча§Њ а§Ха•На§≤а§Ња§В১ড় а§ѓа§Њ ৕а§Хৌ৮ а§Ьа•Иа§Єа•А а§Ъа•Аа§Ьа•Ла§В а§Єа•З а§≠а•А а§За§Є а§ѓа•Б৵а§Х а§Ха§Њ а§Ха•Ла§И а§≤а•З৮ৌ-৶а•З৮ৌ а§єа•Л а§Єа§Х১ৌ а§єа•Иа•§ а§Ьа§ѓ а§єа•Л ৴а•На§∞а•А৙১ড়, а§Ьа§ѓ а§єа•Л а§єа§Ѓа§Ња§∞а•А ৮а§И ৙а•А৊৥৊а•А а§Ха•А а§Й১а•На§Єа§Ња§є-а§Йа§Ѓа§Ва§Ч а§Фа§∞ а§Єа•Ва§Э-а§ђа•Ва§Э а§≠а§∞а•А а§ѓа•Б৵ৌ а§Ка§∞а•На§Ьа§Њ а§Ха•Аа•§ а§Еа§ђ а§ђа§Ња§∞а•А а§єа•И ৴а•На§∞а•А ৴а•Иа§≤а§Ѓа•Н а§Ха•Аа•§ ৮৺а•Аа§В ৮ৌа§Ча§Ња§∞а•На§Ьа•Б৮ а§Ха•Ла§Ва§°а§Њ, ৮৺а•Аа§В а§Ла§Ја§њ-а§Ша§Ња§Яа•А а§Ха•А а§Фа§∞, а§єа§В৙а•А а§Ха•А а§≠а•А а§Ха•На§ѓа•Ла§В ৮৺а•Аа§В? а§≤а•За§Хড়৮ а§Ха•На§ѓа§Њ ১а•Ба§Ѓа•На§єа§Ња§∞а§Њ ৪ৌ৕ ৶а•З৮а•З а§Ха•Л а§Єа§∞а•Н৵১а•На§∞ а§Ра§Єа§Њ ৪৺ৃৌ১а•На§∞а•А а§Єа•Ба§≤а§≠ а§єа•Ла§Ча§Њ? а§Ь৮৪১а•Н১ৌ а§Єа•З а§Єа§Ња§≠а§Ња§∞вАМа•§

 а§Ѓа§Іа•На§ѓ ৙а•На§∞৶а•З৴
а§Ѓа§Іа•На§ѓ ৙а•На§∞৶а•З৴ 





















